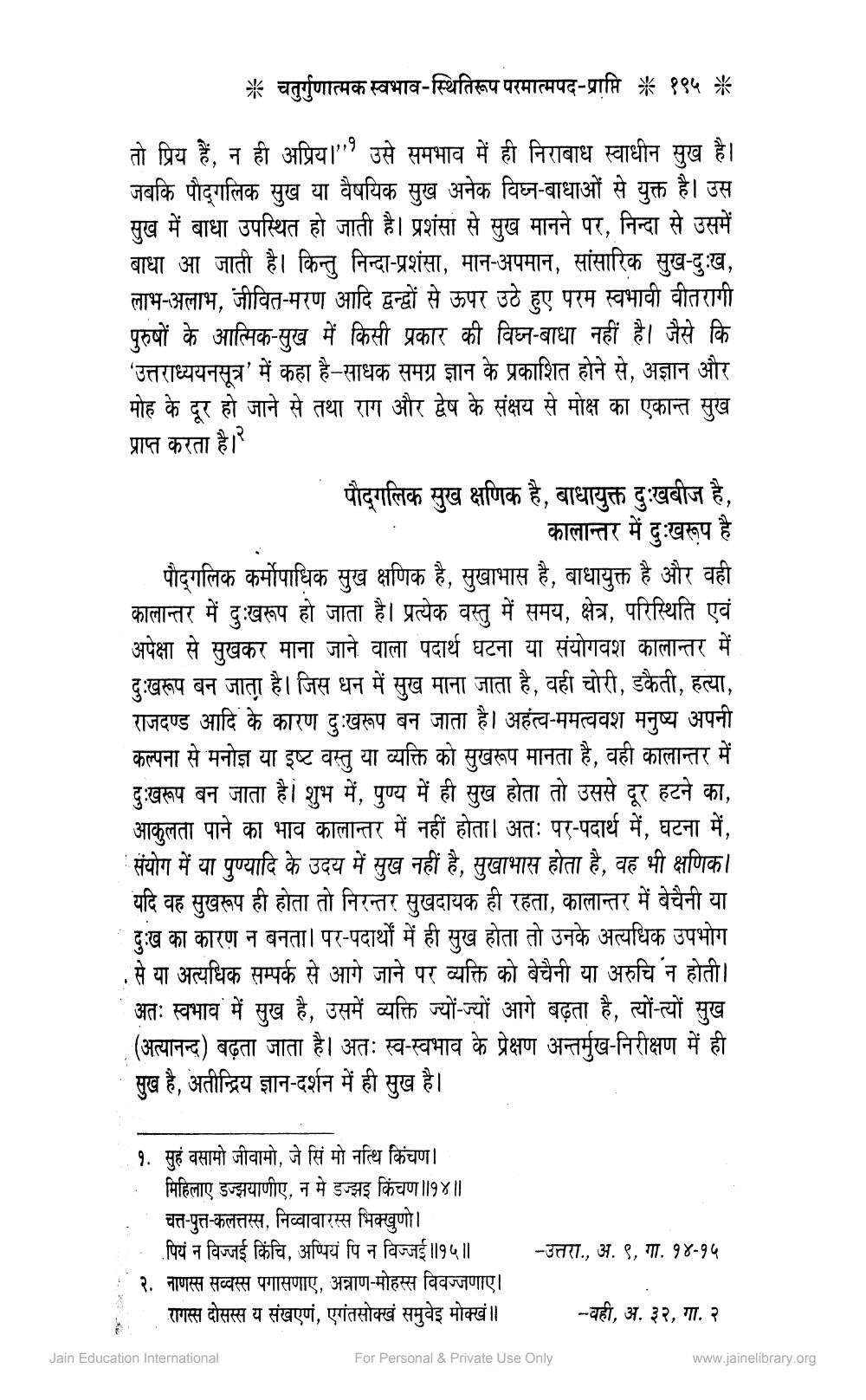________________
* चतुर्गुणात्मक स्वभाव-स्थितिरूप परमात्मपद-प्राप्ति * १९५ *
तो प्रिय हैं. न ही अप्रिय।"१ उसे समभाव में ही निराबाध स्वाधीन सुख है। जबकि पौद्गलिक सुख या वैषयिक सुख अनेक विघ्न-बाधाओं से युक्त है। उस सुख में बाधा उपस्थित हो जाती है। प्रशंसा से सुख मानने पर, निन्दा से उसमें बाधा आ जाती है। किन्तु निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान, सांसारिक सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, जीवित-मरण आदि द्वन्द्वों से ऊपर उठे हुए परम स्वभावी वीतरागी पुरुषों के आत्मिक-सुख में किसी प्रकार की विघ्न-बाधा नहीं है। जैसे कि 'उत्तराध्ययनसूत्र' में कहा है-साधक समग्र ज्ञान के प्रकाशित होने से, अज्ञान और मोह के दूर हो जाने से तथा राग और द्वेष के संक्षय से मोक्ष का एकान्त सुख प्राप्त करता है। पौद्गलिक सुख क्षणिक है, बाधायुक्त दुःखबीज है,
कालान्तर में दुःखरूप है पौद्गलिक कर्मोपाधिक सुख क्षणिक है, सुखाभास है, बाधायुक्त है और वही कालान्तर में दुःखरूप हो जाता है। प्रत्येक वस्तु में समय, क्षेत्र, परिस्थिति एवं अपेक्षा से सुखकर माना जाने वाला पदार्थ घटना या संयोगवश कालान्तर में दुःखरूप बन जाता है। जिस धन में सुख माना जाता है, वही चोरी, डकैती, हत्या,
राजदण्ड आदि के कारण दुःखरूप बन जाता है। अहंत्व-ममत्ववश मनुष्य अपनी कल्पना से मनोज्ञ या इष्ट वस्तु या व्यक्ति को सुखरूप मानता है, वही कालान्तर में दुःखरूप बन जाता है। शुभ में, पुण्य में ही सुख होता तो उससे दूर हटने का, आकुलता पाने का भाव कालान्तर में नहीं होता। अतः पर-पदार्थ में, घटना में, संयोग में या पुण्यादि के उदय में सुख नहीं है, सुखाभास होता है, वह भी क्षणिक। यदि वह सुखरूप ही होता तो निरन्तर सुखदायक ही रहता, कालान्तर में बेचैनी या दुःख का कारण न बनता। पर-पदार्थों में ही सुख होता तो उनके अत्यधिक उपभोग से या अत्यधिक सम्पर्क से आगे जाने पर व्यक्ति को बेचैनी या अरुचि न होती। अतः स्वभाव में सुख है, उसमें व्यक्ति ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों सुख (अत्यानन्द) बढ़ता जाता है। अतः स्व-स्वभाव के प्रेक्षण अन्तर्मुख-निरीक्षण में ही सुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान-दर्शन में ही सुख है।
१. सुहं वसामो जीवामो, जे सिं मो नत्थि किंचण।
मिहिलाए डज्झयाणीए, न मे डज्झइ किंचण॥१४॥ चत्त-पुत्त-कलत्तस्स, निव्वावारस्स भिक्खुणो। पियं न विज्जई किंचि, अप्पियं पि न विज्जई ॥१५॥ २. नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण-मोहस्स विवज्जणाए।
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्खं समुवेइ मोक्खं॥
-उत्तरा., अ. ९, गा. १४-१५
-वही, अ. ३२, गा. २
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org