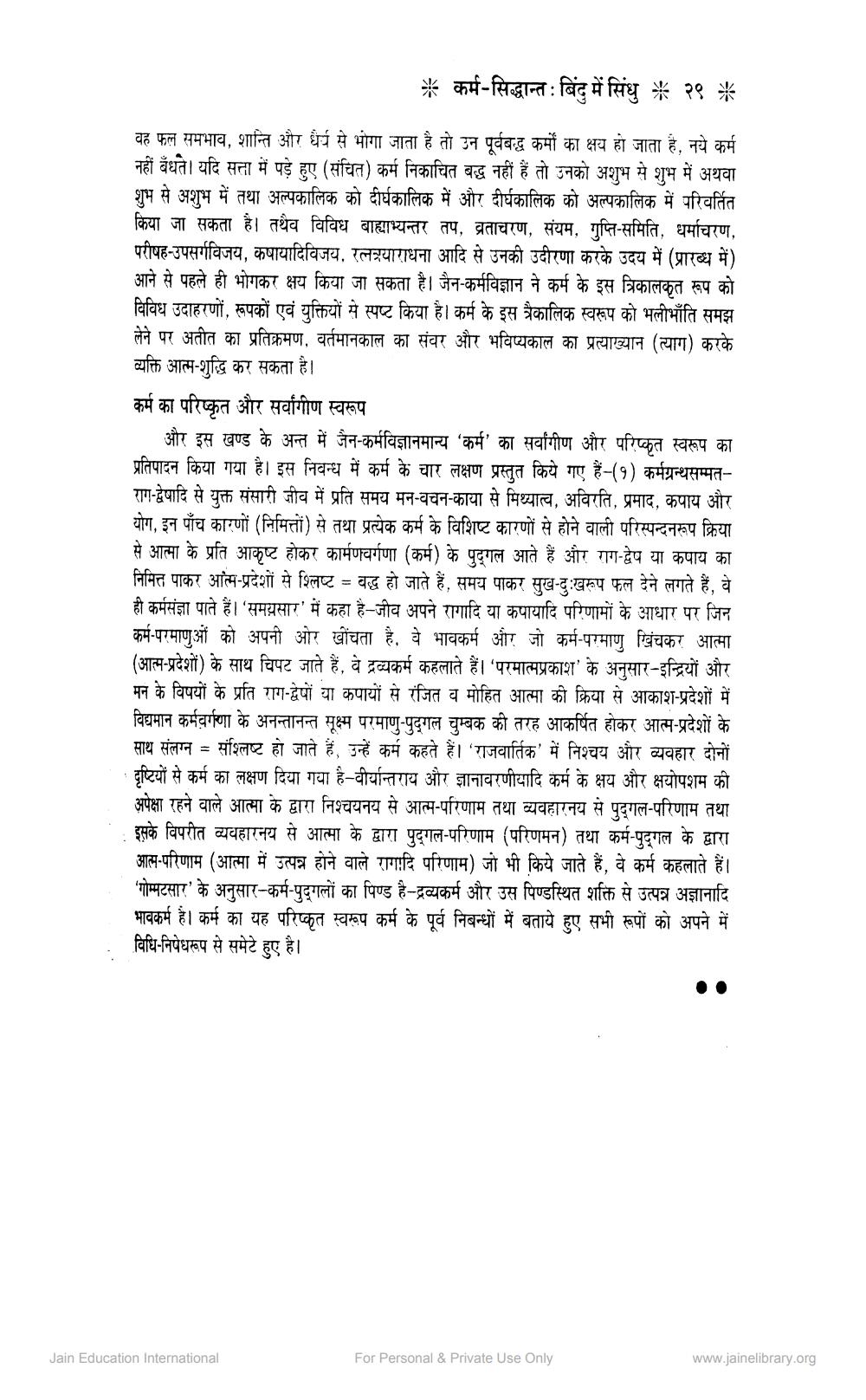________________
* कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु * २९ *
वह फल समभाव, शान्ति और धैर्य से भोगा जाता है तो उन पूर्वबद्ध कर्मों का क्षय हो जाता है, नये कर्म नहीं बँधते। यदि सत्ता में पड़े हुए (संचित) कर्म निकाचित बद्ध नहीं हैं तो उनको अशुभ से शुभ में अथवा शुभ से अशुभ में तथा अल्पकालिक को दीर्घकालिक में और दीर्घकालिक को अल्पकालिक में परिवर्तित किया जा सकता है। तथैव विविध बाह्याभ्यन्तर तप, व्रताचरण, संयम, गुप्ति-समिति, धर्माचरण, परीषह-उपसर्गविजय, कषायादिविजय. रत्नत्रयाराधना आदि से उनकी उदीरणा करके उदय में (प्रारब्ध में) आने से पहले ही भोगकर क्षय किया जा सकता है। जैन-कर्मविज्ञान ने कर्म के इस त्रिकालकृत रूप को विविध उदाहरणों, रूपकों एवं युक्तियों से स्पष्ट किया है। कर्म के इस त्रैकालिक स्वरूप को भलीभाँति समझ लेने पर अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमानकाल का संवर और भविष्यकाल का प्रत्याख्यान (त्याग) करके व्यक्ति आत्म-शुद्धि कर सकता है। कर्म का परिष्कृत और सर्वांगीण स्वरूप ___और इस खण्ड के अन्त में जैन-कर्मविज्ञानमान्य 'कर्म' का सर्वांगीण और परिष्कृत स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस निबन्ध में कर्म के चार लक्षण प्रस्तुत किये गए हैं-(१) कर्मग्रन्थसम्मतराग-द्वेषादि से युक्त संसारी जीव में प्रति समय मन-वचन-काया से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद. कपाय और योग, इन पाँच कारणों (निमित्तों) से तथा प्रत्येक कर्म के विशिष्ट कारणों से होने वाली परिस्पन्दनरूप क्रिया से आत्मा के प्रति आकृष्ट होकर कार्मणवर्गणा (कर्म) के पुद्गल आते हैं और गग-द्वेष या कपाय का निमित्त पाकर आत्म-प्रदेशों से श्लिष्ट = बद्ध हो जाते हैं, समय पाकर सुख-दुःखरूप फल देने लगते हैं, वे ही कर्मसंज्ञा पाते हैं। 'समयसार' में कहा है-जीव अपने रागादि या कपायादि परिणामों के आधार पर जिन कर्म-परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है, वे भावकर्म और जो कर्म-परमाणु खिंचकर आत्मा (आत्म-प्रदेशों) के साथ चिपट जाते हैं, वे द्रव्यकर्म कहलाते हैं। ‘परमात्मप्रकाश' के अनुसार-इन्द्रियों और मन के विषयों के प्रति राग-द्वेषों या कपायों से रंजित व मोहित आत्मा की क्रिया से आकाश-प्रदेशों में विद्यमान कर्मवर्गणा के अनन्तानन्त सूक्ष्म परमाणु-पुद्गल चुम्बक की तरह आकर्षित होकर आत्म-प्रदेशों के साथ संलग्न = संश्लिष्ट हो जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। 'राजवार्तिक' में निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से कर्म का लक्षण दिया गया है-वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणीयादि कर्म के क्षय और क्षयोपशम की अपेक्षा रहने वाले आत्मा के द्वारा निश्चयनय से आत्म-परिणाम तथा व्यवहारनय से पुद्गल-परिणाम तथा इसके विपरीत व्यवहारनय से आत्मा के द्वारा पुद्गल-परिणाम (परिणमन) तथा कर्म-पुद्गल के द्वारा आत्म-परिणाम (आत्मा में उत्पन्न होने वाले रागादि परिणाम) जो भी किये जाते हैं, वे कर्म कहलाते हैं। 'गोम्मटसार' के अनुसार-कर्म-पुद्गलों का पिण्ड है-द्रव्यकर्म और उस पिण्डस्थित शक्ति से उत्पन्न अज्ञानादि भावकर्म है। कर्म का यह परिष्कृत स्वरूप कर्म के पूर्व निबन्धों में बताये हुए सभी रूपों को अपने में विधि-निषेधरूप से समेटे हुए है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org