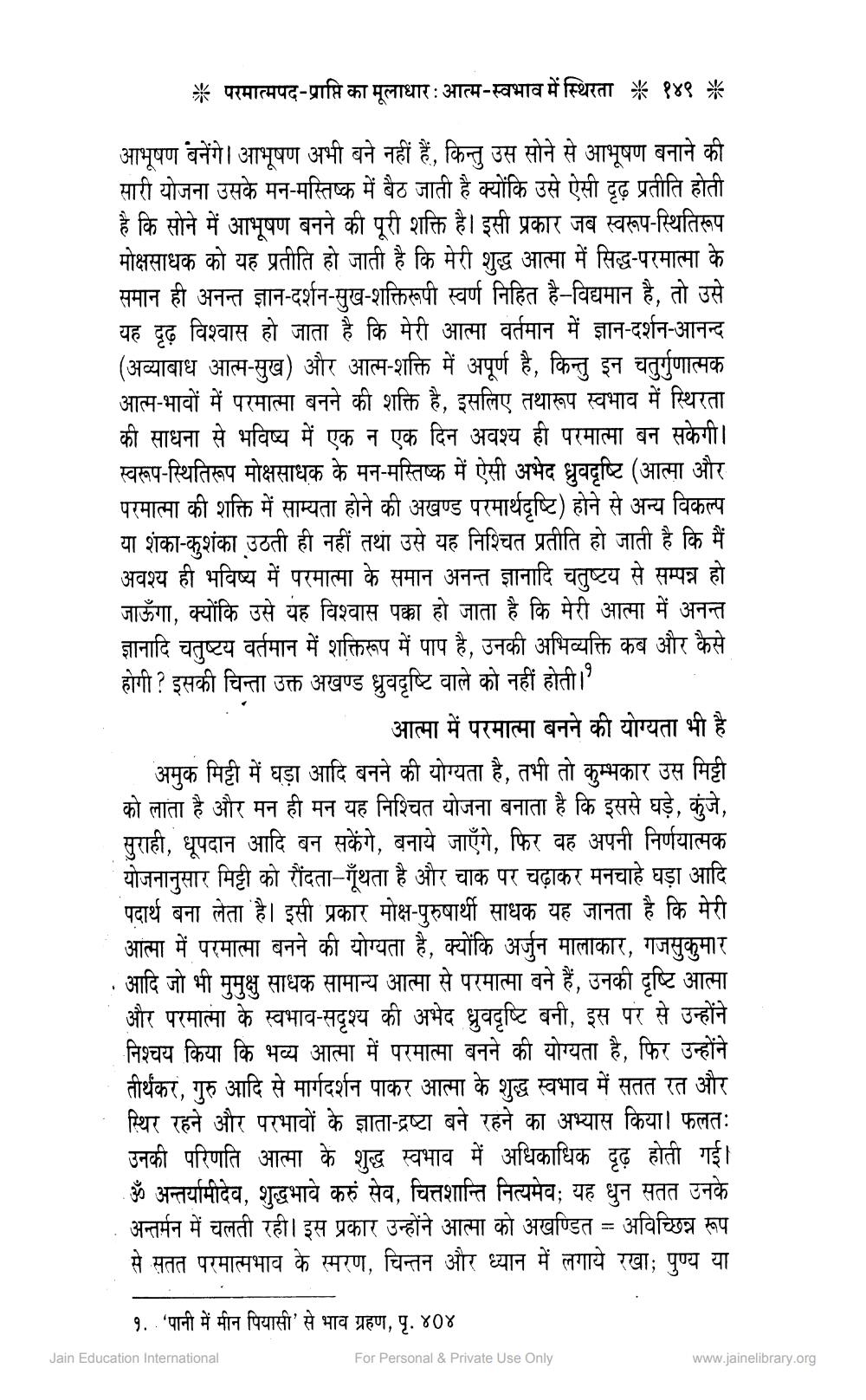________________
* परमात्मपद-प्राप्ति का मूलाधार : आत्म-स्वभाव में स्थिरता * १४९ *
आभूषण बनेंगे। आभूषण अभी बने नहीं हैं, किन्तु उस सोने से आभषण बनाने की सारी योजना उसके मन-मस्तिष्क में बैठ जाती है क्योंकि उसे ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है कि सोने में आभूषण बनने की पूरी शक्ति है। इसी प्रकार जब स्वरूप-स्थितिरूप मोक्षसाधक को यह प्रतीति हो जाती है कि मेरी शुद्ध आत्मा में सिद्ध-परमात्मा के समान ही अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख-शक्तिरूपी स्वर्ण निहित है-विद्यमान है, तो उसे यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि मेरी आत्मा वर्तमान में ज्ञान-दर्शन-आनन्द (अव्याबाध आत्म-सुख) और आत्म-शक्ति में अपूर्ण है, किन्तु इन चतुर्गुणात्मक आत्म-भावों में परमात्मा बनने की शक्ति है, इसलिए तथारूप स्वभाव में स्थिरता की साधना से भविष्य में एक न एक दिन अवश्य ही परमात्मा बन सकेगी। स्वरूप-स्थितिरूप मोक्षसाधक के मन-मस्तिष्क में ऐसी अभेद ध्रवदृष्टि (आत्मा और परमात्मा की शक्ति में साम्यता होने की अखण्ड परमार्थदृष्टि) होने से अन्य विकल्प या शंका-कुशंका उठती ही नहीं तथा उसे यह निश्चित प्रतीति हो जाती है कि मैं अवश्य ही भविष्य में परमात्मा के समान अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय से सम्पन्न हो जाऊँगा, क्योंकि उसे यह विश्वास पक्का हो जाता है कि मेरी आत्मा में अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय वर्तमान में शक्तिरूप में पाप है, उनकी अभिव्यक्ति कब और कैसे होगी? इसकी चिन्ता उक्त अखण्ड ध्रुवदृष्टि वाले को नहीं होती।
आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता भी है अमुक मिट्टी में घड़ा आदि बनने की योग्यता है, तभी तो कुम्भकार उस मिट्टी को लाता है और मन ही मन यह निश्चित योजना बनाता है कि इससे घड़े, कुंजे, सुराही, धूपदान आदि बन सकेंगे, बनाये जाएंगे, फिर वह अपनी निर्णयात्मक योजनानुसार मिट्टी को रौंदता-गूंथता है और चाक पर चढ़ाकर मनचाहे घड़ा आदि पदार्थ बना लेता है। इसी प्रकार मोक्ष-पुरुषार्थी साधक यह जानता है कि मेरी आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, क्योंकि अर्जुन मालाकार, गजसुकुमार आदि जो भी मुमुक्षु साधक सामान्य आत्मा से परमात्मा बने हैं, उनकी दृष्टि आत्मा और परमात्मा के स्वभाव-सदृश्य की अभेद ध्रुवदृष्टि बनी, इस पर से उन्होंने निश्चय किया कि भव्य आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, फिर उन्होंने तीर्थंकर, गुरु आदि से मार्गदर्शन पाकर आत्मा के शुद्ध स्वभाव में सतत रत और स्थिर रहने और परभावों के ज्ञाता-द्रष्टा बने रहने का अभ्यास किया। फलतः उनकी परिणति आत्मा के शुद्ध स्वभाव में अधिकाधिक दृढ़ होती गई। ॐ अन्तर्यामीदेव, शुद्धभावे करुं सेव, चित्तशान्ति नित्यमेव; यह धुन सतत उनके अन्तर्मन में चलती रही। इस प्रकार उन्होंने आत्मा को अखण्डित = अविच्छिन्न रूप से सतत परमात्मभाव के स्मरण, चिन्तन और ध्यान में लगाये रखा; पुण्य या
१. 'पानी में मीन पियासी' से भाव ग्रहण, पृ. ४०४ Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org