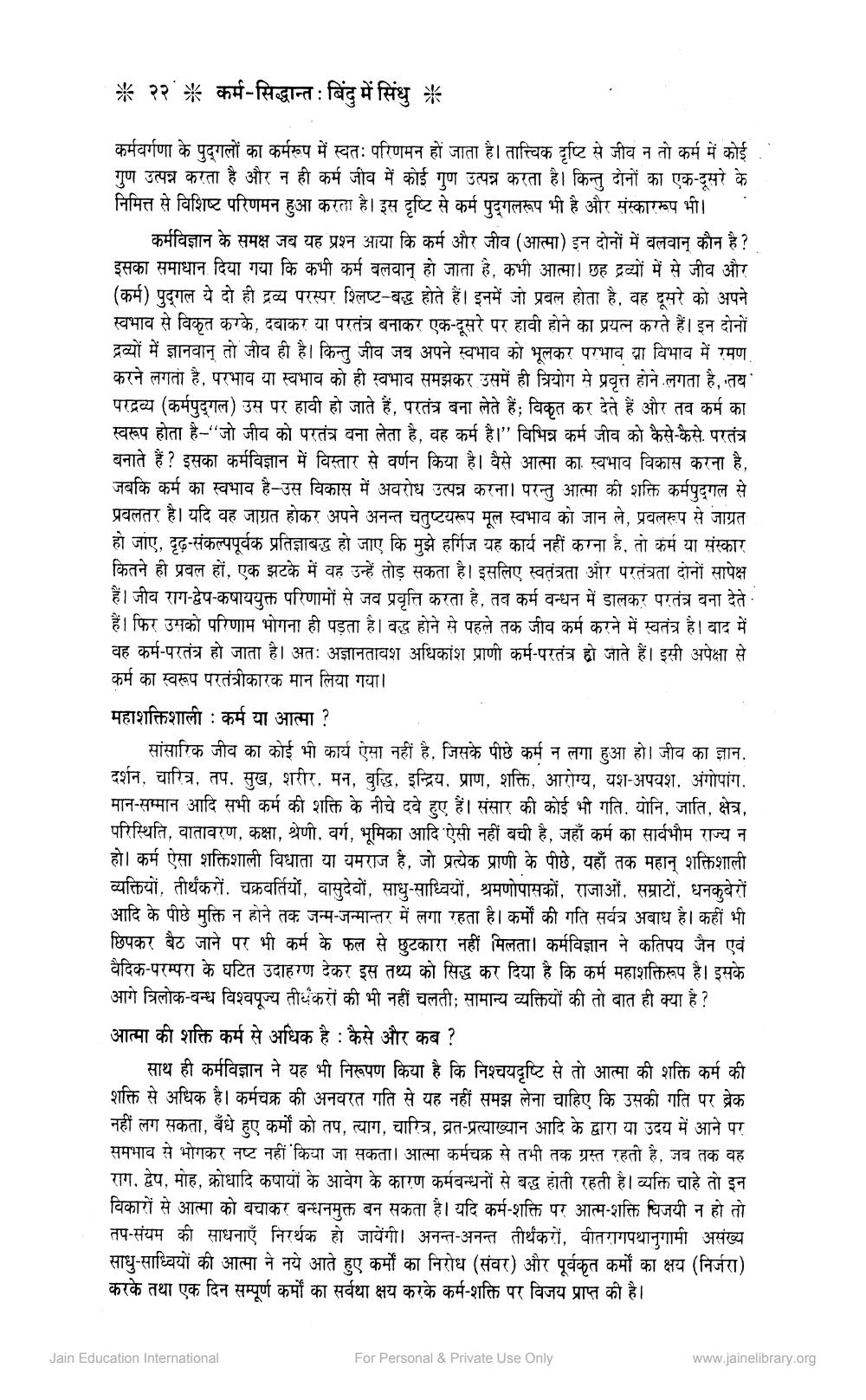________________
* २२ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
कर्मवर्गणा के पुद्गलों का कर्मरूप में स्वतः परिणमन हो जाता है। तात्त्विक दृष्टि से जीव न तो कर्म में कोई .. गुण उत्पन्न करता है और न ही कर्म जीव में कोई गुण उत्पन्न करता है। किन्तु दोनों का एक-दूसरे के निमित्त से विशिष्ट परिणमन हुआ करता है। इस दृष्टि से कर्म पुद्गलरूप भी है और संस्काररूप भी।
कर्मविज्ञान के समक्ष जब यह प्रश्न आया कि कर्म और जीव (आत्मा) इन दोनों में बलवान् कौन है ? इसका समाधान दिया गया कि कभी कर्म बलवान हो जाता है, कभी आत्मा। छह द्रव्यों में से जीव और (कर्म) पुद्गल ये दो ही द्रव्य परस्पर श्लिष्ट-बद्ध होते हैं। इनमें जो प्रबल होता है, वह दूसरे को अपने स्वभाव से विकृत करके, दबाकर या परतंत्र बनाकर एक-दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न करते हैं। इन दोनों द्रव्यों में ज्ञानवान तो जीव ही है। किन्तु जीव जब अपने स्वभाव को भूलकर परभाव या विभाव में रमण करने लगता है, परभाव या स्वभाव को ही स्वभाव समझकर उसमें ही त्रियोग से प्रवृत्त होने लगता है, तब परद्रव्य (कर्मपुद्गल) उस पर हावी हो जाते हैं, परतंत्र बना लेते हैं; विकृत कर देते हैं और तव कर्म का स्वरूप होता है-"जो जीव को परतंत्र बना लेता है, वह कर्म है।" विभिन्न कर्म जीव को कैसे-कैसे. परतंत्र बनाते हैं ? इसका कर्मविज्ञान में विस्तार से वर्णन किया है। वैसे आत्मा का. स्वभाव विकास करना है, जबकि कर्म का स्वभाव है-उस विकास में अवरोध उत्पन्न करना। परन्तु आत्मा की शक्ति कर्मपुद्गल से प्रबलतर है। यदि वह जाग्रत होकर अपने अनन्त चतुष्टयरूप मूल स्वभाव को जान ले, प्रवलरूप से जाग्रत हो जाए, दृढ़-संकल्पपूर्वक प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए कि मुझे हर्गिज यह कार्य नहीं करना है. तो कर्म या संस्कार कितने ही प्रवल हों, एक झटके में वह उन्हें तोड़ सकता है। इसलिए स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों सापेक्ष हैं। जीव राग-द्वेष-कषाययुक्त परिणामों से जव प्रवृत्ति करता है, तब कर्म वन्धन में डालकर परतंत्र बना देते . हैं। फिर उसको परिणाम भोगना ही पड़ता है। बद्ध होने से पहले तक जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। बाद में वह कर्म-परतंत्र हो जाता है। अतः अज्ञानतावश अधिकांश प्राणी कर्म-परतंत्र हो जाते हैं। इसी अपेक्षा से कर्म का स्वरूप परतंत्रीकारक मान लिया गया। महाशक्तिशाली : कर्म या आत्मा ?
सांसारिक जीव का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जिसके पीछे कर्म न लगा हुआ हो। जीव का ज्ञान. दर्शन, चारित्र, तप, सुख, शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण, शक्ति, आरोग्य, यश-अपयश, अंगोपांग. मान-सम्मान आदि सभी कर्म की शक्ति के नीचे दबे हुए हैं। संसार की कोई भी गति, योनि, जाति, क्षेत्र, परिस्थिति, वातावरण, कक्षा, श्रेणी, वर्ग, भूमिका आदि ऐसी नहीं बची है, जहाँ कर्म का सार्वभौम राज्य न हो। कर्म ऐसा शक्तिशाली विधाता या यमराज है, जो प्रत्येक प्राणी के पीछे, यहाँ तक महान् शक्तिशाली व्यक्तियों, तीर्थंकरों. चक्रवर्तियों, वासुदेवों, साधु-साध्वियों, श्रमणोपासकों, राजाओं, सम्राटों, धनकुबेरों
आदि के पीछे मुक्ति न होने तक जन्म-जन्मान्तर में लगा रहता है। कर्मों की गति सर्वत्र अबाध है। कहीं भी छिपकर बैठ जाने पर भी कर्म के फल से छुटकारा नहीं मिलता। कर्मविज्ञान ने कतिपय जैन एवं वैदिक-परम्परा के घटित उदाहरण देकर इस तथ्य को सिद्ध कर दिया है कि कर्म महाशक्तिरूप है। इसके आगे त्रिलोक-बन्ध विश्वपूज्य तीर्थंकरों की भी नहीं चलती; सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही क्या है ? आत्मा की शक्ति कर्म से अधिक है : कैसे और कब ?
साथ ही कर्मविज्ञान ने यह भी निरूपण किया है कि निश्चयदृष्टि से तो आत्मा की शक्ति कर्म की शक्ति से अधिक है। कर्मचक्र की अनवरत गति से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि उसकी गति पर ब्रेक नहीं लग सकता, बँधे हुए कर्मों को तप, त्याग, चारित्र, व्रत-प्रत्याख्यान आदि के द्वारा या उदय में आने पर समभाव से भोगकर नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा कर्मचक्र से तभी तक ग्रस्त रहती है, जब तक वह राग, द्वेष, मोह, क्रोधादि कषायों के आवेग के कारण कर्मबन्धनों से बद्ध होती रहती है। व्यक्ति चाहे तो इन विकारों से आत्मा को बचाकर बन्धनमुक्त बन सकता है। यदि कर्म-शक्ति पर आत्म-शक्ति विजयी न हो तो तप-संयम की साधनाएँ निरर्थक हो जायेंगी। अनन्त-अनन्त तीर्थंकरों, वीतरागपथानुगामी असंख्य साधु-साध्वियों की आत्मा ने नये आते हुए कर्मों का निरोध (संवर) और पूर्वकृत कर्मों का क्षय (निर्जरा) करके तथा एक दिन सम्पूर्ण कर्मों का सर्वथा क्षय करके कर्म-शक्ति पर विजय प्राप्त की है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org