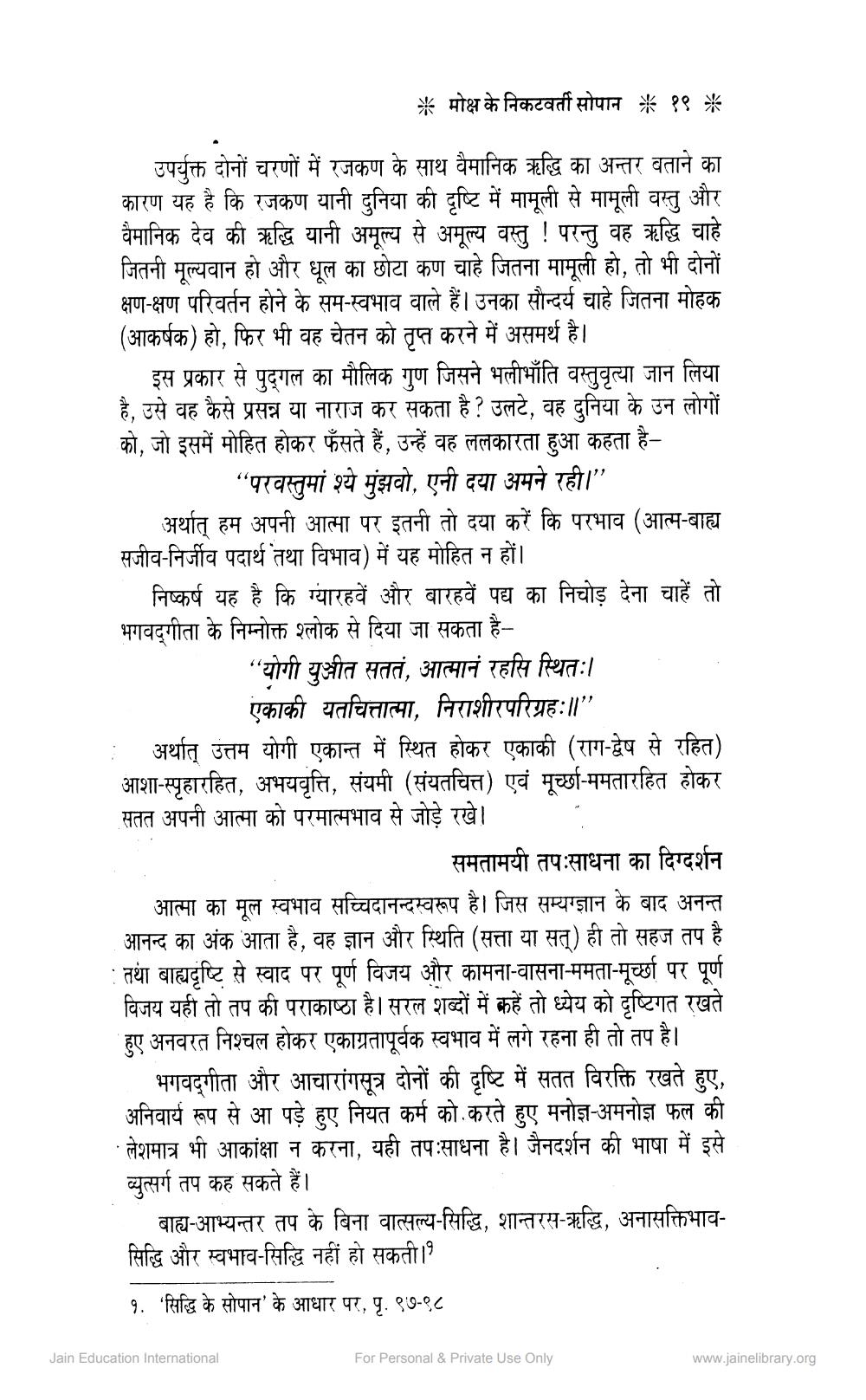________________
* मोक्ष के निकटवर्ती सोपान * १९ *
उपर्युक्त दोनों चरणों में रजकण के साथ वैमानिक ऋद्धि का अन्तर बताने का कारण यह है कि रजकण यानी दुनिया की दृष्टि में मामूली से मामूली वस्तु और वैमानिक देव की ऋद्धि यानी अमूल्य से अमूल्य वस्तु ! परन्तु वह ऋद्धि चाहे जितनी मूल्यवान हो और धूल का छोटा कण चाहे जितना मामूली हो, तो भी दोनों क्षण-क्षण परिवर्तन होने के सम-स्वभाव वाले हैं। उनका सौन्दर्य चाहे जितना मोहक (आकर्षक) हो, फिर भी वह चेतन को तृप्त करने में असमर्थ है।
इस प्रकार से पुद्गल का मौलिक गुण जिसने भलीभाँति वस्तुवृत्या जान लिया है, उसे वह कैसे प्रसन्न या नाराज कर सकता है ? उलटे, वह दुनिया के उन लोगों को, जो इसमें मोहित होकर फँसते हैं, उन्हें वह ललकारता हुआ कहता है
___“परवस्तुमां श्ये मुंझवो, एनी दया अमने रही।" अर्थात् हम अपनी आत्मा पर इतनी तो दया करें कि परभाव (आत्म-बाह्य सजीव-निर्जीव पदार्थ तथा विभाव) में यह मोहित न हों। __निष्कर्ष यह है कि ग्यारहवें और बारहवें पद्य का निचोड़ देना चाहें तो भगवद्गीता के निम्नोक्त श्लोक से दिया जा सकता है
“योगी युञ्जीत सततं, आत्मानं रहसि स्थितः।
एकाकी यतचित्तात्मा, निराशीरपरिग्रहः॥" : अर्थात् उत्तम योगी एकान्त में स्थित होकर एकाकी (राग-द्वेष से रहित) आशा-स्पृहारहित, अभयवृत्ति, संयमी (संयतचित्त) एवं मूर्छा-ममतारहित होकर सतत अपनी आत्मा को परमात्मभाव से जोड़े रखे।
समतामयी तपःसाधना का दिग्दर्शन आत्मा का मूल स्वभाव सच्चिदानन्दस्वरूप है। जिस सम्यग्ज्ञान के बाद अनन्त आनन्द का अंक आता है, वह ज्ञान और स्थिति (सत्ता या सत्) ही तो सहज तप है तथा बाह्यदृष्टि से स्वाद पर पूर्ण विजय और कामना-वासना-ममता-मूर्छा पर पूर्ण विजय यही तो तप की पराकाष्ठा है। सरल शब्दों में कहें तो ध्येय को दृष्टिगत रखते हुए अनवरत निश्चल होकर एकाग्रतापूर्वक स्वभाव में लगे रहना ही तो तप है। ___ भगवद्गीता और आचारांगसूत्र दोनों की दृष्टि में सतत विरक्ति रखते हुए,
अनिवार्य रूप से आ पड़े हुए नियत कर्म को करते हुए मनोज्ञ-अमनो फल की • लेशमात्र भी आकांक्षा न करना, यही तपःसाधना है। जैनदर्शन की भाषा में इसे व्युत्सर्ग तप कह सकते हैं।
बाह्य-आभ्यन्तर तप के बिना वात्सल्य-सिद्धि, शान्तरस-ऋद्धि, अनासक्तिभावसिद्धि और स्वभाव-सिद्धि नहीं हो सकती।' १. 'सिद्धि के सोपान' के आधार पर, पृ. ९७-९८
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org