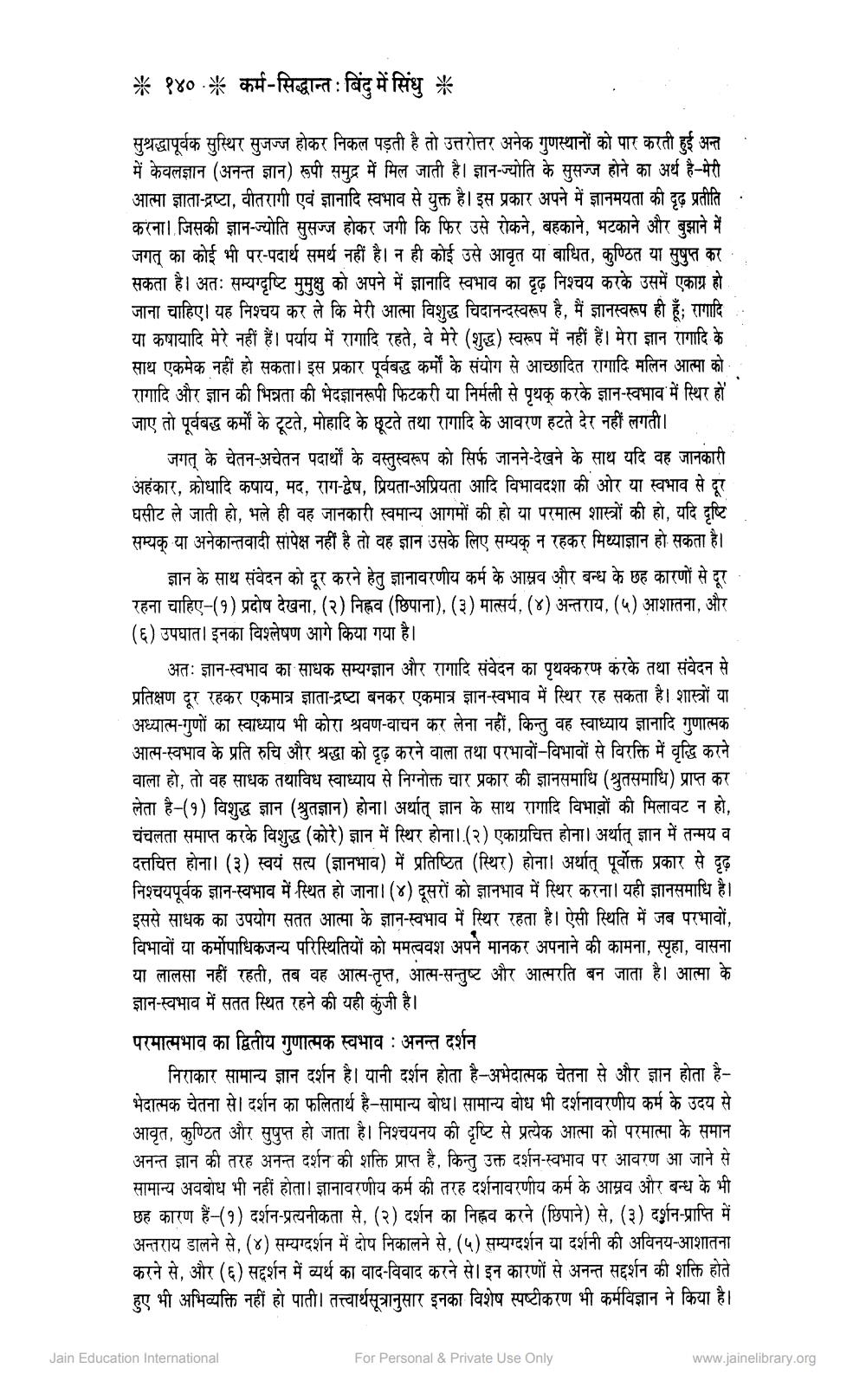________________
* १४० * कर्म - सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
सुश्रद्धापूर्वक सुस्थिर सुजज्ज होकर निकल पड़ती है तो उत्तरोत्तर अनेक गुणस्थानों को पार करती हुई अन्त में केवलज्ञान (अनन्त ज्ञान) रूपी समुद्र में मिल जाती है। ज्ञान ज्योति के सुसज्ज होने का अर्थ है - मेरी आत्मा ज्ञाता द्रष्टा, वीतरागी एवं ज्ञानादि स्वभाव से युक्त है। इस प्रकार अपने में ज्ञानमयता की दृढ़ प्रतीति करना। जिसकी ज्ञान - ज्योति सुसज्ज होकर जगी कि फिर उसे रोकने, बहकाने, भटकाने और बुझाने में जगत् का कोई भी पर-पदार्थ समर्थ नहीं है। न ही कोई उसे आवृत या बाधित, कुण्ठित या सुषुप्त कर सकता है। अतः सम्यग्दृष्टि मुमुक्षु को अपने में ज्ञानादि स्वभाव का दृढ़ निश्चय करके उसमें एकाग्र हो जाना चाहिए। यह निश्चय कर ले कि मेरी आत्मा विशुद्ध चिदानन्दस्वरूप है, मैं ज्ञानस्वरूप ही हूँ; रागादि या कषायादि मेरे नहीं हैं। पर्याय में रागादि रहते, वे मेरे (शुद्ध) स्वरूप में नहीं हैं। मेरा ज्ञान रागादि के साथ एकमेक नहीं हो सकता। इस प्रकार पूर्वबद्ध कर्मों के संयोग से आच्छादित रागादि मलिन आत्मा को रागादि और ज्ञान की भिन्नता की भेदज्ञानरूपी फिटकरी या निर्मली से पृथक् करके ज्ञान स्वभाव में स्थिर हों जाए तो पूर्वबद्ध कर्मों के टूटते, मोहादि के छूटते तथा रागादि के आवरण हटते देर नहीं लगती ।
जगत्
के चेतन-अचेतन पदार्थों के वस्तुस्वरूप को सिर्फ जानने-देखने के साथ यदि वह जानकारी अहंकार, क्रोधादि कषाय, मद, राग-द्वेष, प्रियता-अप्रियता आदि विभावदशा की ओर या स्वभाव से दूर घसीट ले जाती हो, भले ही वह जानकारी स्वमान्य आगमों की हो या परमात्म शास्त्रों की हो, यदि दृष्टि सम्यक् या अनेकान्तवादी सांपेक्ष नहीं है तो वह ज्ञान उसके लिए सम्यक् न रहकर मिथ्याज्ञान हो सकता है।
ज्ञान के साथ संवेदन को दूर करने हेतु ज्ञानावरणीय कर्म के आम्रव और बन्ध के छह कारणों से दूर रहना चाहिए - (१) प्रदोष देखना, (२) निह्नव (छिपाना), (३) मात्सर्य, (४) अन्तराय, (५) आशातना, और (६) उपघात । इनका विश्लेषण आगे किया गया है।
अतः ज्ञान-स्वभाव का साधक सम्यग्ज्ञान और रागादि संवेदन का पृथक्करण करके तथा संवेदन से प्रतिक्षण दूर रहकर एकमात्र ज्ञाता- द्रष्टा बनकर एकमात्र ज्ञान - स्वभाव में स्थिर रह सकता है। शास्त्रों या अध्यात्म - गुणों का स्वाध्याय भी कोरा श्रवण- वाचन कर लेना नहीं, किन्तु वह स्वाध्याय ज्ञानादि गुणात्मक आत्म-स्वभाव के प्रति रुचि और श्रद्धा को दृढ़ करने वाला तथा परभावों-विभावों से विरक्ति में वृद्धि करने वाला हो, तो वह साधक तथाविध स्वाध्याय से निग्नोक्त चार प्रकार की ज्ञानसमाधि ( श्रुतसमाधि) प्राप्त कर लेता है - ( १ ) विशुद्ध ज्ञान (श्रुतज्ञान) होना । अर्थात् ज्ञान के साथ रागादि विभावों की मिलावट न हो, चंचलता समाप्त करके विशुद्ध (कोरे) ज्ञान में स्थिर होना । (२) एकाग्रचित्त होना । अर्थात् ज्ञान में तन्मय व दत्तचित्त होना। (३) स्वयं सत्य (ज्ञानभाव ) में प्रतिष्ठित (स्थिर) होना । अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार से दृढ़ निश्चयपूर्वक ज्ञान स्वभाव में स्थित हो जाना । (४) दूसरों को ज्ञानभाव में स्थिर करना । यही ज्ञानसमाधि है। इससे साधक का उपयोग सतत आत्मा के ज्ञान स्वभाव में स्थिर रहता है। ऐसी स्थिति में जब परभावों, विभावों या कर्मोपाधिकजन्य परिस्थितियों को ममत्ववश अपने मानकर अपनाने की कामना, स्पृहा, वासना या लालसा नहीं रहती, तब वह आत्म-तृप्त, आत्म सन्तुष्ट और आत्मरति बन जाता है। आत्मा के ज्ञान-स्वभाव में सतत स्थित रहने की यही कुंजी है ।
परमात्मभाव का द्वितीय गुणात्मक स्वभाव : अनन्त दर्शन
निराकार सामान्य ज्ञान दर्शन है। यानी दर्शन होता है - अभेदात्मक चेतना से और ज्ञान होता हैभेदात्मक चेतना से । दर्शन का फलितार्थ है- सामान्य बोध । सामान्य बोध भी दर्शनावरणीय कर्म के उदय से आवृत, कुण्ठित और सुषुप्त हो जाता है । निश्चयनय की दृष्टि से प्रत्येक आत्मा को परमात्मा के समान अनन्त ज्ञान की तरह अनन्त दर्शन की शक्ति प्राप्त है, किन्तु उक्त दर्शन-स्वभाव पर आवरण आ जाने से सामान्य अवबोध भी नहीं होता । ज्ञानावरणीय कर्म की तरह दर्शनावरणीय कर्म के आम्रव और बन्ध के भी छह कारण हैं - ( १ ) दर्शन- प्रत्यनीकता से, (२) दर्शन का निह्नव करने ( छिपाने) से, (३) दर्शन-प्राप्ति में अन्तराय डालने से, (४) सम्यग्दर्शन में दोष निकालने से, (५) सम्यग्दर्शन या दर्शनी की अविनय - आशातना करने से, और (६) सद्दर्शन में व्यर्थ का वाद-विवाद करने से। इन कारणों से अनन्त सद्दर्शन की शक्ति होते हुए भी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती । तत्त्वार्थसूत्रानुसार इनका विशेष स्पष्टीकरण भी कर्मविज्ञान ने किया है।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org