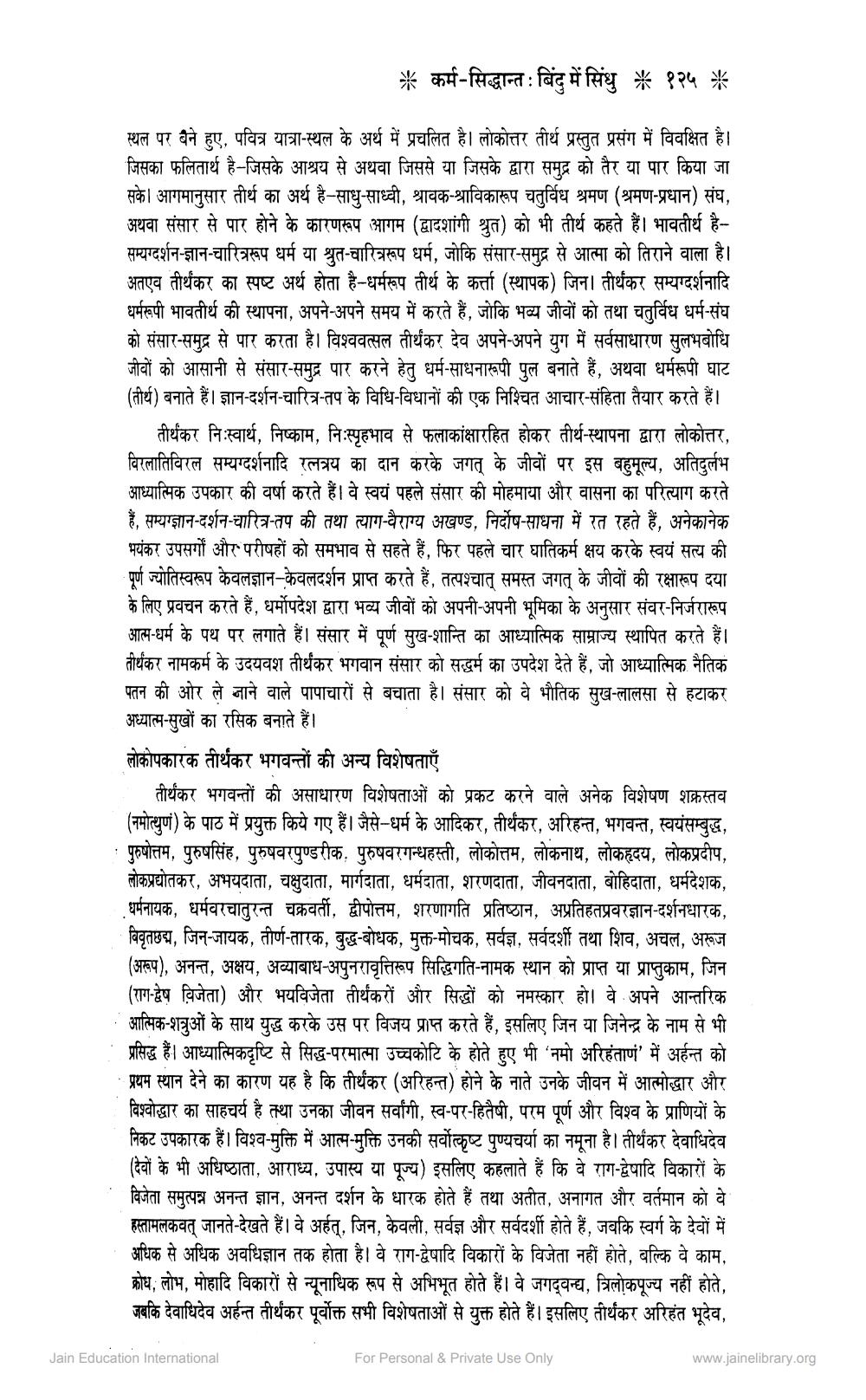________________
* कर्म - सिद्धान्त: बिंदु में सिंधु * १२५ *
स्थल पर बने हुए, पवित्र यात्रा - स्थल के अर्थ में प्रचलित है। लोकोत्तर तीर्थ प्रस्तुत प्रसंग में विवक्षित है। जिसका फलितार्थ है-जिसके आश्रय से अथवा जिससे या जिसके द्वारा समुद्र को तैर या पार किया जा सके। आगमानुसार तीर्थ का अर्थ है - साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकारूप चतुर्विध श्रमण ( श्रमण-प्रधान) संघ, अथवा संसार से पार होने के कारणरूप आगम ( द्वादशांगी श्रुत) को भी तीर्थ कहते हैं । भावतीर्थ हैसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप धर्म या श्रुत चारित्ररूप धर्म, जोकि संसार-समुद्र से आत्मा को तिराने वाला है। अतएव तीर्थंकर का स्पष्ट अर्थ होता है - धर्मरूप तीर्थ के कर्ता (स्थापक ) जिन । तीर्थंकर सम्यग्दर्शनादि धर्मरूपी भावतीर्थ की स्थापना, अपने-अपने समय में करते हैं, जोकि भव्य जीवों को तथा चतुर्विध धर्म-संघ को संसार-समुद्र से पार करता है । विश्ववत्सल तीर्थंकर देव अपने-अपने युग में सर्वसाधारण सुलभबोधि जीवों को आसानी से संसार-समुद्र पार करने हेतु धर्म-साधनारूपी पुल बनाते हैं, अथवा धर्मरूपी घट (तीर्थ) बनाते हैं। ज्ञान-दर्शन -चारित्र तप के विधि-विधानों की एक निश्चित आचार संहिता तैयार करते हैं।
तीर्थंकर निःस्वार्थ, निष्काम, निःस्पृहभाव से फलाकांक्षारहित होकर तीर्थ स्थापना द्वारा लोकोत्तर, विरलातिविरल सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय का दान करके जगत् के जीवों पर इस बहुमूल्य, अतिदुर्लभ आध्यात्मिक उपकार की वर्षा करते हैं। वे स्वयं पहले संसार की मोहमाया और वासना का परित्याग करते हैं, सम्यग्ज्ञान-दर्शनचारित्र-तप की तथा त्याग - वैराग्य अखण्ड, निर्दोष-साधना में रत रहते हैं, अनेकानेक भयंकर उपसर्गों और परीषहों को समभाव से सहते हैं, फिर पहले चार घातिकर्म क्षय करके स्वयं सत्य की पूर्ण ज्योतिस्वरूप केवलज्ञान- केवलदर्शन प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात् समस्त जगत् के जीवों की रक्षारूप दया के लिए प्रवचन करते हैं, धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवों को अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार संवर - निर्जरारूप आत्म-धर्म के पथ पर लगाते हैं। संसार में पूर्ण सुख-शान्ति का आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करते हैं। तीर्थंकर नामकर्म के उदयवश तीर्थंकर भगवान संसार को सद्धर्म का उपदेश देते हैं, जो आध्यात्मिक नैतिक पतन की ओर ले जाने वाले पापाचारों से बचाता है। संसार को वे भौतिक सुख-लालसा से हटाकर अध्यात्म-सुखों का रसिक बनाते हैं।
लोकोपकारक तीर्थंकर भगवन्तों की अन्य विशेषताएँ
तीर्थंकर भगवन्तों की असाधारण विशेषताओं को प्रकट करने वाले अनेक विशेषण शक्रस्तव (नमोत्थु ) के पाठ में प्रयुक्त किये गए हैं। जैसे- धर्म के आदिकर, तीर्थंकर, अरिहन्त, भगवन्त, स्वयंसम्बुद्ध, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषवरपुण्डरीक, पुरुषवरगन्धहस्ती, लोकोत्तम, लोकनाथ, लोकहृदय, लोकप्रदीप, लोकप्रद्योतकर, अभयदाता, चक्षुदाता, मार्गदाता, धर्मदाता, शरणदाता, जीवनदाता, बोहिदाता, धर्मदेशक, . धर्मनायक, धर्मवरचातुरन्त चक्रवर्ती, द्वीपोत्तम, शरणागति प्रतिष्ठान, अप्रतिहतप्रवरज्ञान-दर्शनधारक, विवृतछद्म, जिन-जायक, तीर्ण- तारक, बुद्ध-बोधक, मुक्त-मोचक, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तथा शिव, अचल, अरूज (अरूप), अनन्त, अक्षय, अव्याबाध - अपुनरावृत्तिरूप सिद्धिगति - नामक स्थान को प्राप्त या प्राप्तुकाम, जिन ( राग-द्वेष विजेता) और भयविजेता तीर्थंकरों और सिद्धों को नमस्कार हो । वे अपने आन्तरिक आत्मिक-शत्रुओं के साथ युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए जिन या जिनेन्द्र के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आध्यात्मिकदृष्टि से सिद्ध- परमात्मा उच्चकोटि के होते हुए भी 'नमो अरिहंताणं' में अर्हन्त को प्रथम स्थान देने का कारण यह है कि तीर्थंकर ( अरिहन्त ) होने के नाते उनके जीवन में आत्मोद्धार और विश्वोद्धार का साहचर्य है तथा उनका जीवन सर्वांगी, स्व-पर-हितैषी, परम पूर्ण और विश्व के प्राणियों के निकट उपकारक हैं। विश्व-मुक्ति में आत्म-मुक्ति उनकी सर्वोत्कृष्ट पुण्यचर्या का नमूना है। तीर्थंकर देवाधिदेव (देवों के भी अधिष्ठाता, आराध्य, उपास्य या पूज्य) इसलिए कहलाते हैं कि वे राग-द्वेषादि विकारों के विजेता समुत्पन्न अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन के धारक होते हैं तथा अतीत, अनागत और वर्तमान को वे हस्तामलकवत् जानते-देखते हैं। वे अर्हत्, जिन, केवली, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं, जबकि स्वर्ग के देवों में अधिक से अधिक अवधिज्ञान तक होता है। वे राग-द्वेषादि विकारों के विजेता नहीं होते, बल्कि वे काम, क्रोध, लोभ, मोहादि विकारों से न्यूनाधिक रूप से अभिभूत होते हैं। वे जगद्वन्द्य, त्रिलोकपूज्य नहीं होते, जबकि देवाधिदेव अर्हन्त तीर्थंकर पूर्वोक्त सभी विशेषताओं से युक्त होते हैं। इसलिए तीर्थंकर अरिहंत भूदेव,
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org