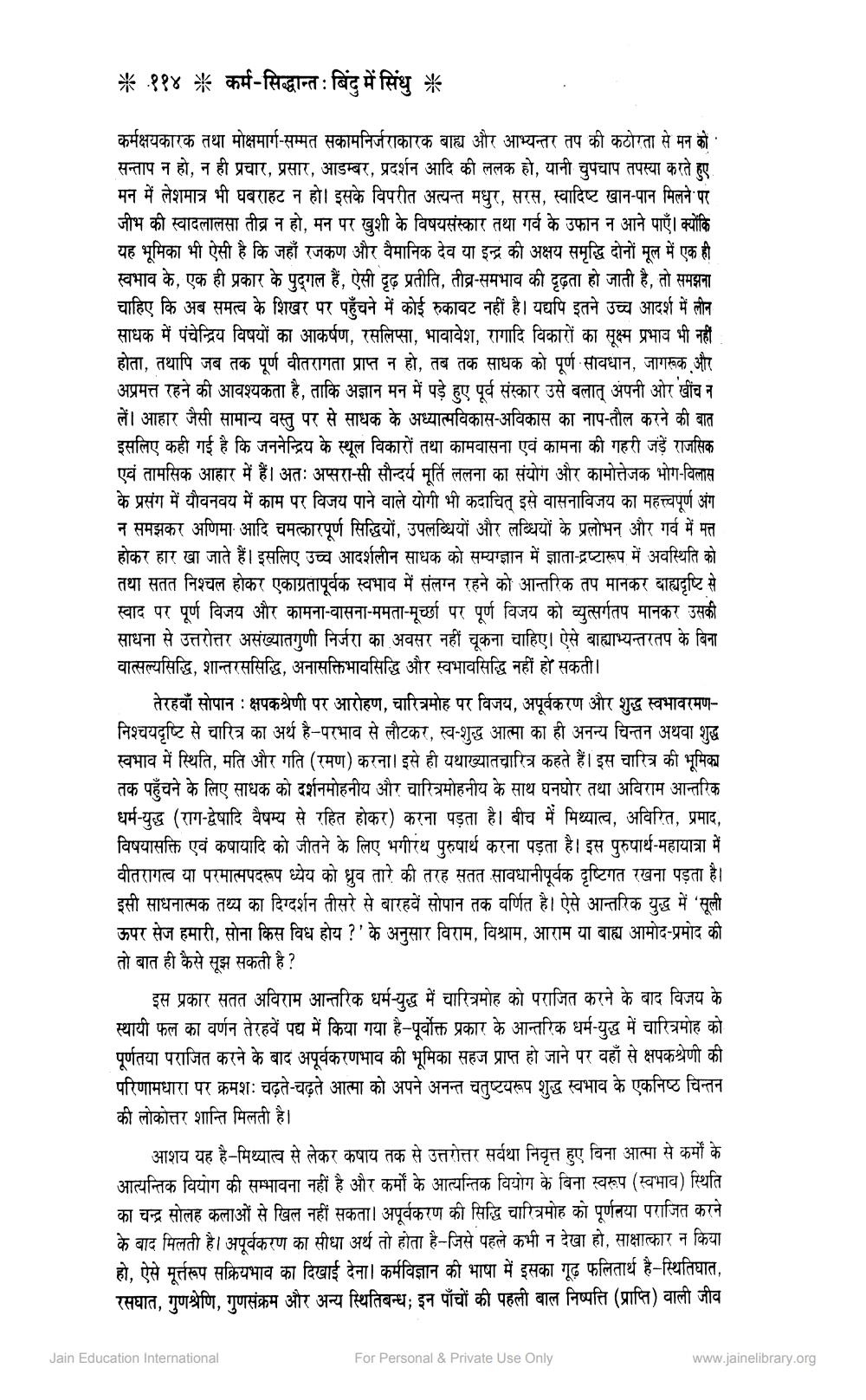________________
* ११४ * कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु *
कर्मक्षयकारक तथा मोक्षमार्ग-सम्मत सकामनिर्जराकारक बाह्य और आभ्यन्तर तप की कठोरता से मन को । सन्ताप न हो, न ही प्रचार, प्रसार, आडम्बर, प्रदर्शन आदि की ललक हो, यानी चुपचाप तपस्या करते हुए मन में लेशमात्र भी घबराहट न हो। इसके विपरीत अत्यन्त मधुर, सरस, स्वादिष्ट खान-पान मिलने पर जीभ की स्वादलालसा तीव्र न हो, मन पर खुशी के विषयसंस्कार तथा गर्व के उफान न आने पाएँ। क्योंकि यह भूमिका भी ऐसी है कि जहाँ रजकण और वैमानिक देव या इन्द्र की अक्षय समृद्धि दोनों मूल में एक ही स्वभाव के, एक ही प्रकार के पुद्गल हैं, ऐसी दृढ़ प्रतीति, तीव्र-समभाव की दृढ़ता हो जाती है, तो समझना चाहिए कि अब समत्व के शिखर पर पहुँचने में कोई रुकावट नहीं है। यद्यपि इतने उच्च आदर्श में लीन साधक में पंचेन्द्रिय विषयों का आकर्षण, रसलिप्सा, भावावेश, रागादि विकारों का सूक्ष्म प्रभाव भी नहीं होता, तथापि जब तक पूर्ण वीतरागता प्राप्त न हो, तब तक साधक को पूर्ण सावधान, जागरूक और अप्रमत्त रहने की आवश्यकता है, ताकि अज्ञान मन में पड़े हुए पूर्व संस्कार उसे बलात् अपनी ओर खींच न लें। आहार जैसी सामान्य वस्तु पर से साधक के अध्यात्मविकास-अविकास का नाप-तौल करने की बात इसलिए कही गई है कि जननेन्द्रिय के स्थूल विकारों तथा कामवासना एवं कामना की गहरी जड़ें राजसिक एवं तामसिक आहार में हैं। अतः अप्सरा-सी सौन्दर्य मूर्ति ललना का संयोग और कामोत्तेजक भोग-विलास के प्रसंग में यौवनवय में काम पर विजय पाने वाले योगी भी कदाचित् इसे वासनाविजय का महत्त्वपूर्ण अंग न समझकर अणिमा आदि चमत्कारपूर्ण सिद्धियों, उपलब्धियों और लब्धियों के प्रलोभन और गर्व में मत्त होकर हार खा जाते हैं। इसलिए उच्च आदर्शलीन साधक को सम्यग्ज्ञान में ज्ञाता-द्रष्टारूप में अवस्थिति को तथा सतत निश्चल होकर एकाग्रतापूर्वक स्वभाव में संलग्न रहने को आन्तरिक तप मानकर बाह्यदृष्टि से स्वाद पर पूर्ण विजय और कामना-वासना-ममता-मूर्छा पर पूर्ण विजय को व्युत्सर्गतप मानकर उसकी साधना से उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा का अवसर नहीं चूकना चाहिए। ऐसे बाह्याभ्यन्तरतप के बिना वात्सल्यसिद्धि, शान्तरससिद्धि, अनासक्तिभावसिद्धि और स्वभावसिद्धि नहीं हो सकती।
तेरहवाँ सोपान : क्षपकश्रेणी पर आरोहण, चारित्रमोह पर विजय, अपूर्वकरण और शुद्ध स्वभावरमणनिश्चयदृष्टि से चारित्र का अर्थ है-परभाव से लौटकर, स्व-शुद्ध आत्मा का ही अनन्य चिन्तन अथवा शुद्ध स्वभाव में स्थिति, मति और गति (रमण) करना। इसे ही यथाख्यातचारित्र कहते हैं। इस चारित्र की भूमिका तक पहुँचने के लिए साधक को दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय के साथ घनघोर तथा अविराम आन्तरिक धर्म-युद्ध (राग-द्वेषादि वैषम्य से रहित होकर) करना पड़ता है। बीच में मिथ्यात्व, अविरित, प्रमाद, विषयासक्ति एवं कषायादि को जीतने के लिए भगीरथ पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस पुरुषार्थ-महायात्रा में वीतरागत्व या परमात्मपदरूप ध्येय को ध्रुव तारे की तरह सतत सावधानीपूर्वक दृष्टिगत रखना पड़ता है। इसी साधनात्मक तथ्य का दिग्दर्शन तीसरे से बारहवें सोपान तक वर्णित है। ऐसे आन्तरिक युद्ध में ‘सूली ऊपर सेज हमारी, सोना किस विध होय ?' के अनुसार विराम, विश्राम, आराम या बाह्य आमोद-प्रमोद की तो बात ही कैसे सूझ सकती है ? ___इस प्रकार सतत अविराम आन्तरिक धर्म-युद्ध में चारित्रमोह को पराजित करने के बाद विजय के स्थायी फल का वर्णन तेरहवें पद्य में किया गया है-पूर्वोक्त प्रकार के आन्तरिक धर्म-युद्ध में चारित्रमोह को पूर्णतया पराजित करने के बाद अपूर्वकरणभाव की भूमिका सहज प्राप्त हो जाने पर वहाँ से क्षपकश्रेणी की परिणामधारा पर क्रमशः चढ़ते-चढ़ते आत्मा को अपने अनन्त चतुष्टयरूप शुद्ध स्वभाव के एकनिष्ठ चिन्तन की लोकोत्तर शान्ति मिलती है। ___ आशय यह है-मिथ्यात्व से लेकर कषाय तक से उत्तरोत्तर सर्वथा निवृत्त हुए बिना आत्मा से कर्मों के आत्यन्तिक वियोग की सम्भावना नहीं है और कर्मों के आत्यन्तिक वियोग के बिना स्वरूप (स्वभाव) स्थिति का चन्द्र सोलह कलाओं से खिल नहीं सकता। अपूर्वकरण की सिद्धि चारित्रमोह को पूर्णतया पराजित करने के बाद मिलती है। अपूर्वकरण का सीधा अर्थ तो होता है-जिसे पहले कभी न देखा हो, साक्षात्कार न किया हो, ऐसे मूर्तरूप सक्रियभाव का दिखाई देना। कर्मविज्ञान की भाषा में इसका गूढ फलितार्थ है-स्थितिघात, रसघात, गुणश्रेणि, गुणसंक्रम और अन्य स्थितिबन्ध; इन पाँचों की पहली बाल निष्पत्ति (प्राप्ति) वाली जीव
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org