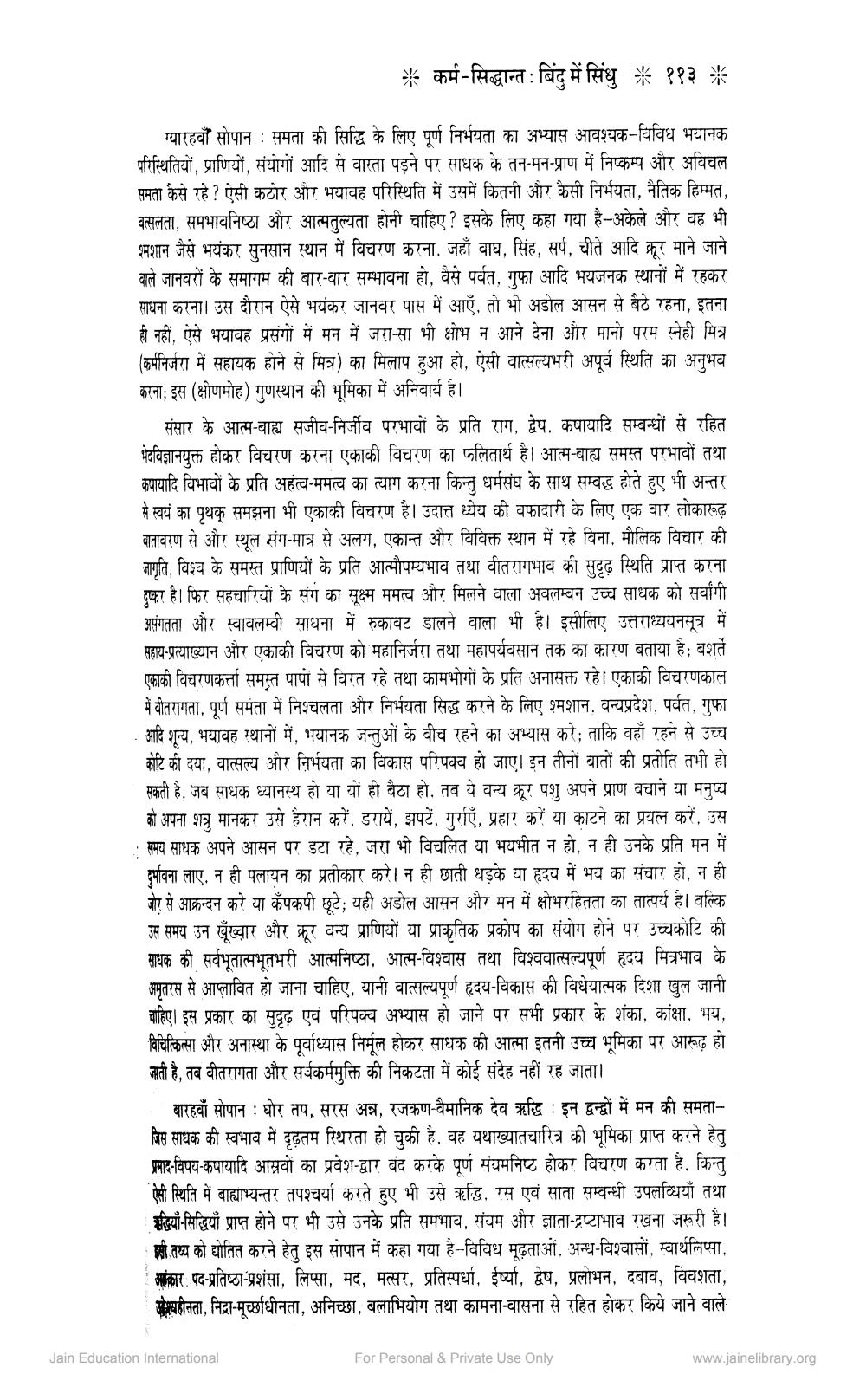________________
* कर्म-सिद्धान्त : बिंदु में सिंधु * ११३ *
ग्यारहवाँ सोपान : समता की सिद्धि के लिए पूर्ण निर्भयता का अभ्यास आवश्यक-विविध भयानक परिस्थितियों, प्राणियों, संयोगों आदि से वास्ता पड़ने पर साधक के तन-मन-प्राण में निष्कम्प और अविचल समता कैसे रहे ? ऐसी कठोर और भयावह परिस्थिति में उसमें कितनी और कैसी निर्भयता, नैतिक हिम्मत, वत्सलता, समभावनिष्ठा और आत्मतुल्यता होनी चाहिए? इसके लिए कहा गया है-अकेले और वह भी श्मशान जैसे भयंकर सुनसान स्थान में विचरण करना. जहाँ वाघ, सिंह, सर्प, चीते आदि क्रूर माने जाने वाले जानवरों के समागम की बार-बार सम्भावना हो, वैसे पर्वत, गुफा आदि भयजनक स्थानों में रहकर साधना करना। उस दौरान ऐसे भयंकर जानवर पास में आएँ, तो भी अडोल आसन से बैठे रहना, इतना ही नहीं, ऐसे भयावह प्रसंगों में मन में जरा-सा भी क्षोभ न आने देना और मानो परम स्नेही मित्र (कर्मनिर्जरा में सहायक होने से मित्र) का मिलाप हुआ हो, ऐसी वात्सल्यभरी अपूर्व स्थिति का अनुभव करना; इस (क्षीणमोह) गुणस्थान की भूमिका में अनिवार्य है।
संसार के आत्म-बाह्य सजीव-निर्जीव परभावों के प्रति राग, द्वेप. कपायादि सम्बन्धों से रहित भेदविज्ञानयुक्त होकर विचरण करना एकाकी विचरण का फलितार्थ है। आत्म-बाह्य समस्त परभावों तथा कषायादि विभावों के प्रति अहंत्व-ममत्व का त्याग करना किन्तु धर्मसंघ के साथ सम्बद्ध होते हुए भी अन्तर से स्वयं का पृथक् समझना भी एकाकी विचरण है। उदात्त ध्येय की वफादारी के लिए एक वार लोकारूढ़ वातावरण से और स्थूल संग-मात्र से अलग, एकान्त और विविक्त स्थान में रहे विना, मौलिक विचार की जागृति, विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति आत्मौपम्यभाव तथा वीतरागभाव की सुदृढ़ स्थिति प्राप्त करना दुष्कर है। फिर सहचारियों के संग का सूक्ष्म ममत्व और मिलने वाला अवलम्बन उच्च साधक को सर्वांगी असंगतता और स्वावलम्वी साधना में रुकावट डालने वाला भी है। इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र में सहाय-प्रत्याख्यान और एकाकी विचरण को महानिर्जरा तथा महापर्यवसान तक का कारण बताया है: बशर्ते एकाकी विचरणकर्ता समस्त पापों से विरत रहे तथा कामभोगों के प्रति अनासक्त रहे। एकाकी विचरणकाल में वीतरागता, पूर्ण समंता में निश्चलता और निर्भयता सिद्ध करने के लिए श्मशान. वन्यप्रदेश. पर्वत, गुफा आदि शून्य, भयावह स्थानों में, भयानक जन्तुओं के बीच रहने का अभ्यास करे; ताकि वहाँ रहने से उच्च कोटि की दया, वात्सल्य और निर्भयता का विकास परिपक्व हो जाए। इन तीनों वातों की प्रतीति तभी हो सकती है, जब साधक ध्यानस्थ हो या यों ही बैठा हो. तब ये वन्य क्रूर पशु अपने प्राण बचाने या मनुष्य को अपना शत्रु मानकर उसे हैरान करें. डरायें, झपटें, गुराएँ, प्रहार करें या काटने का प्रयत्न करें, उस : समय साधक अपने आसन पर डटा रहे, जरा भी विचलित या भयभीत न हो, न ही उनके प्रति मन में दुर्भावना लाए. न ही पलायन का प्रतीकार करे। न ही छाती धड़के या हृदय में भय का संचार हो, न ही जोर से आक्रन्दन करे या कँपकपी छूटे; यही अडोल आसन और मन में क्षोभरहितता का तात्पर्य है। बल्कि उस समय उन खूख्वार और क्रूर वन्य प्राणियों या प्राकृतिक प्रकोप का संयोग होने पर उच्चकोटि की साधक की सर्वभूतात्मभूतभरी आत्मनिष्ठा, आत्म-विश्वास तथा विश्ववात्सल्यपूर्ण हृदय मित्रभाव के अमृतरस से आप्लावित हो जाना चाहिए, यानी वात्सल्यपूर्ण हृदय-विकास की विधेयात्मक दिशा खुल जानी चाहिए। इस प्रकार का सुदृढ़ एवं परिपक्व अभ्यास हो जाने पर सभी प्रकार के शंका, कांक्षा, भय, विचित्कित्सा और अनास्था के पूर्वाध्यास निर्मूल होकर साधक की आत्मा इतनी उच्च भूमिका पर आरूढ़ हो जती है, तब वीतरागता और सर्वकर्ममुक्ति की निकटता में कोई संदेह नहीं रह जाता।
बारहवाँ सोपान : घोर तप, सरस अन्न, रजकण-वैमानिक देव ऋद्धि : इन द्वन्द्वों में मन की समताजिस साधक की स्वभाव में दृढ़तम स्थिरता हो चुकी है. वह यथाख्यातचारित्र की भूमिका प्राप्त करने हेतु प्रमाद-विषय-कषायादि आम्रवों का प्रवेश-द्वार बंद करके पूर्ण संयमनिष्ट होकर विचरण करता है, किन्तु ऐसी स्थिति में बाह्याभ्यन्तर तपश्चर्या करते हुए भी उसे ऋद्धि, ग्स एवं साता सम्बन्धी उपलब्धियाँ तथा सद्धियाँ-सिद्धियाँ प्राप्त होने पर भी उसे उनके प्रति समभाव, संयम और ज्ञाता-द्रप्टाभाव रखना जरूरी है। इसी तथ्य को द्योतित करने हेतु इस सोपान में कहा गया है-विविध मूढ़ताओं, अन्ध-विश्वासों, स्वार्थलिप्सा, अहंकार पद-प्रतिष्ठा-प्रशंसा, लिप्सा, मद, मत्सर, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, प्रलोभन, दबाव, विवशता, हेश्यहीनता, निद्रा-मूर्छाधीनता, अनिच्छा, बलाभियोग तथा कामना-वासना से रहित होकर किये जाने वाले
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org