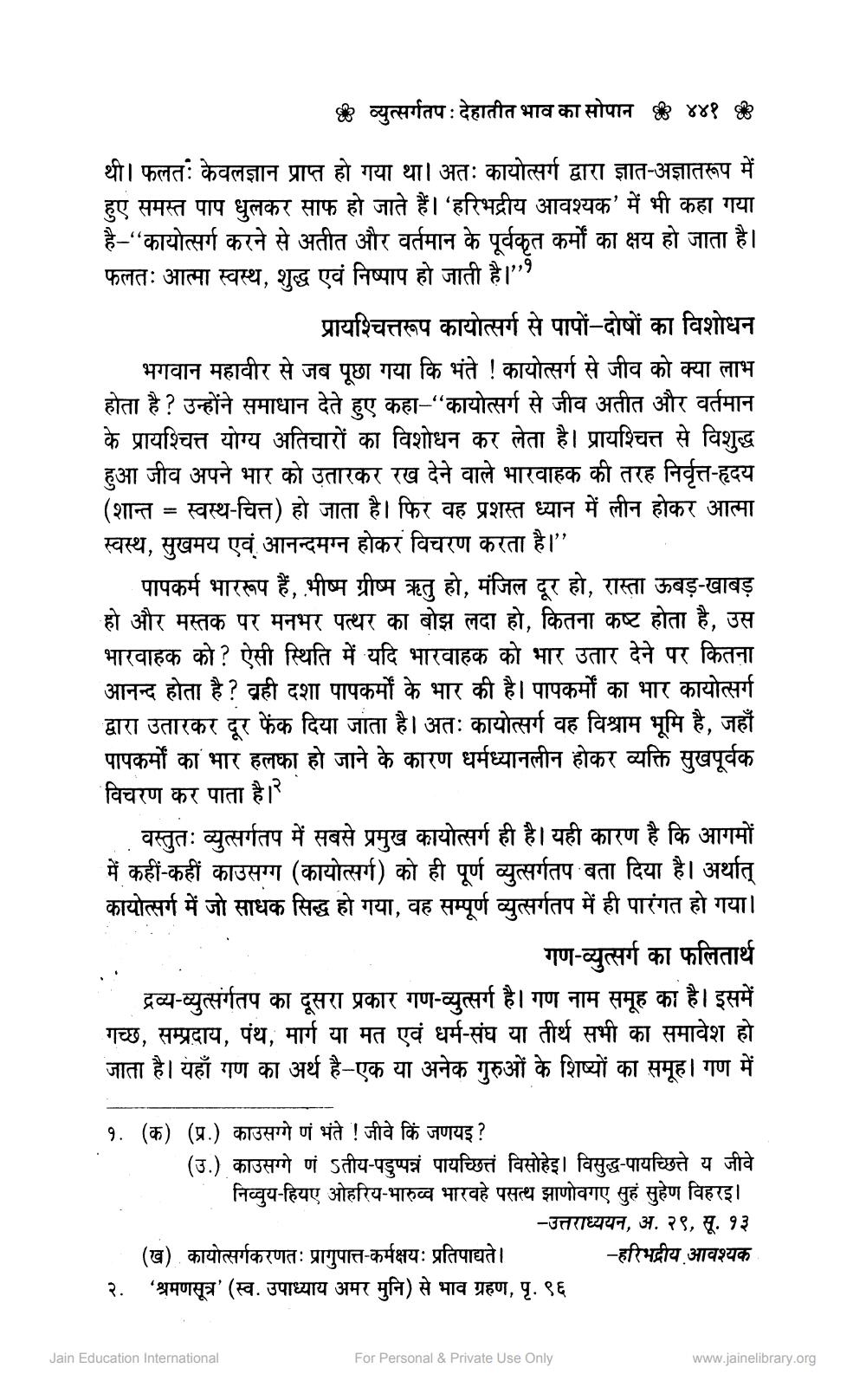________________
* व्युत्सर्गतप : देहातीत भाव का सोपान ॐ ४४१ *
थी। फलतः केवलज्ञान प्राप्त हो गया था। अतः कायोत्सर्ग द्वारा ज्ञात-अज्ञातरूप में हुए समस्त पाप धुलकर साफ हो जाते हैं। ‘हरिभद्रीय आवश्यक' में भी कहा गया है-“कायोत्सर्ग करने से अतीत और वर्तमान के पूर्वकृत कर्मों का क्षय हो जाता है। फलतः आत्मा स्वस्थ, शुद्ध एवं निष्पाप हो जाती है।"
प्रायश्चित्तरूप कायोत्सर्ग से पापों-दोषों का विशोधन भगवान महावीर से जब पूछा गया कि भंते ! कायोत्सर्ग से जीव को क्या लाभ होता है ? उन्होंने समाधान देते हुए कहा-“कायोत्सर्ग से जीव अतीत और वर्तमान के प्रायश्चित्त योग्य अतिचारों का विशोधन कर लेता है। प्रायश्चित्त से विशुद्ध हुआ जीव अपने भार को उतारकर रख देने वाले भारवाहक की तरह निवृत्त-हृदय (शान्त = स्वस्थ-चित्त) हो जाता है। फिर वह प्रशस्त ध्यान में लीन होकर आत्मा स्वस्थ, सुखमय एवं आनन्दमग्न होकर विचरण करता है।" ___ पापकर्म भाररूप हैं, भीष्म ग्रीष्म ऋत हो, मंजिल दूर हो, रास्ता ऊबड़-खाबड़ हो और मस्तक पर मनभर पत्थर का बोझ लदा हो, कितना कष्ट होता है, उस भारवाहक को ? ऐसी स्थिति में यदि भारवाहक को भार उतार देने पर कितना आनन्द होता है? वही दशा पापकर्मों के भार की है। पापकर्मों का भार कायोत्सर्ग द्वारा उतारकर दूर फेंक दिया जाता है। अतः कायोत्सर्ग वह विश्राम भूमि है, जहाँ पापकर्मों का भार हलका हो जाने के कारण धर्मध्यानलीन होकर व्यक्ति सुखपूर्वक विचरण कर पाता है। ... वस्तुतः व्युत्सर्गतप में सबसे प्रमुख कायोत्सर्ग ही है। यही कारण है कि आगमों में कहीं-कहीं काउसग्ग (कायोत्सर्ग) को ही पूर्ण व्युत्सर्गतप बता दिया है। अर्थात् कायोत्सर्ग में जो साधक सिद्ध हो गया, वह सम्पूर्ण व्युत्सर्गतप में ही पारंगत हो गया।
गण-व्युत्सर्ग का फलितार्थ द्रव्य-व्युत्सर्गतप का दूसरा प्रकार गण-व्युत्सर्ग है। गण नाम समूह का है। इसमें गच्छ, सम्प्रदाय, पंथ, मार्ग या मत एवं धर्म-संघ या तीर्थ सभी का समावेश हो जाता है। यहाँ गण का अर्थ है-एक या अनेक गुरुओं के शिष्यों का समूह। गण में
१. (क) (प्र.) काउसग्गे णं भंते ! जीवे किं जणयइ?
(उ.) काउसग्गे णं ऽतीय-पडुप्पन्नं पायच्छित्तं विसोहेइ। विसुद्ध-पायच्छित्ते य जीवे निव्वुय-हियए ओहरिय-भारुव्व भारवहे पसत्थ झाणोवगए सुहं सुहेण विहरइ।
-उत्तराध्ययन, अ. २९, सू. १३ (ख) कायोत्सर्गकरणतः प्रागुपात्त-कर्मक्षयः प्रतिपाद्यते। -हरिभद्रीय आवश्यक २. 'श्रमणसूत्र' (स्व. उपाध्याय अमर मुनि) से भाव ग्रहण, पृ. ९६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org