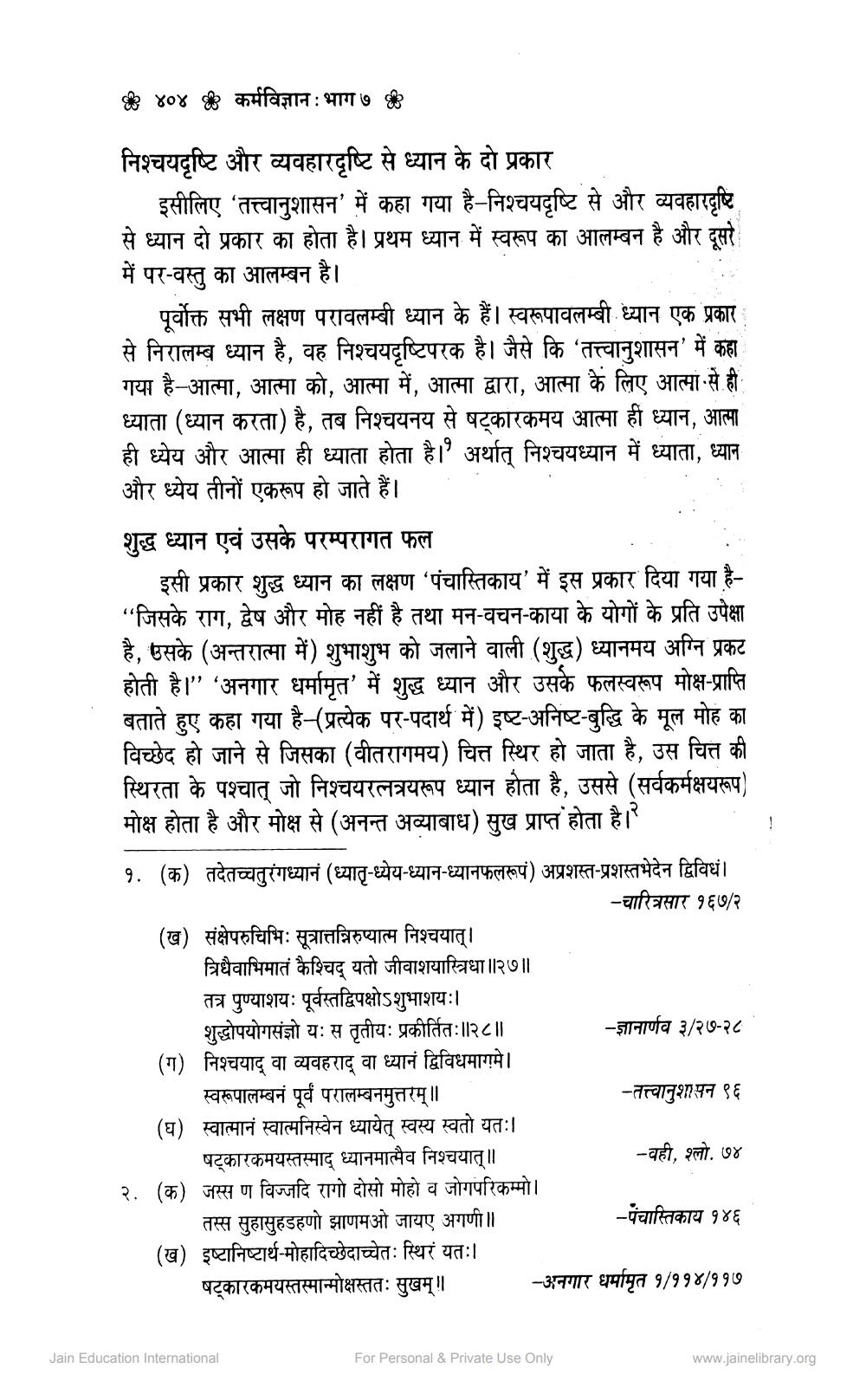________________
४०४ कर्मविज्ञान : भाग ७
निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि से ध्यान के दो प्रकार
इसीलिए 'तत्त्वानुशासन' में कहा गया है - निश्चयदृष्टि से और व्यवहारदृष्टि से ध्यान दो प्रकार का होता है। प्रथम ध्यान में स्वरूप का आलम्बन है और दूसरे में पर-वस्तु का आलम्बन है ।
पूर्वोक्त सभी लक्षण परावलम्बी ध्यान के हैं। स्वरूपावलम्बी ध्यान एक प्रकार से निरालम्ब ध्यान है, वह निश्चयदृष्टिपरक है। जैसे कि 'तत्त्वानुशासन' में कहा गया है- आत्मा, आत्मा को, आत्मा में, आत्मा द्वारा, आत्मा के लिए आत्मा से ही ध्याता (ध्यान करता) है, तब निश्चयनय से षट्कारकमय आत्मा ही ध्यान, आत्मा ही ध्येय और आत्मा ही ध्याता होता है ।' अर्थात् निश्चयध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एकरूप हो जाते हैं।
शुद्ध ध्यान एवं उसके परम्परागत फल
इसी प्रकार शुद्ध ध्यान का लक्षण 'पंचास्तिकाय' में इस प्रकार दिया गया है" जिसके राग, द्वेष और मोह नहीं है तथा मन-वचन-काया के योगों के प्रति उपेक्षा है, उसके (अन्तरात्मा में ) शुभाशुभ को जलाने वाली (शुद्ध) ध्यानमय अग्नि प्रकट होती है।” 'अनगार धर्मामृत' में शुद्ध ध्यान और उसके फलस्वरूप मोक्ष-प्राप्ति बताते हुए कहा गया है - ( प्रत्येक पर - पदार्थ में ) इष्ट-अनिष्ट - बुद्धि के मूल मोह का विच्छेद हो जाने से जिसका ( वीतरागमय) चित्त स्थिर हो जाता है, उस चित्त की स्थिरता के पश्चात् जो निश्चयरत्नत्रयरूप ध्यान होता है, उससे (सर्वकर्मक्षयरूप) मोक्ष होता है और मोक्ष से ( अनन्त अव्याबाध) सुख प्राप्त होता है ।
१. (क) तदेतच्चतुरंगध्यानं (ध्यातृ-ध्येय-ध्यान-ध्यानफलरूपं) अप्रशस्त - प्रशस्तभेदेन द्विविधं । - चारित्रसार १६७ / २
(ख) संक्षेपरुचिभिः सूत्रात्तन्निरूप्यात्म निश्चयात् । त्रिधैवाभिमतं कैश्चिद्यतो जीवाशयास्त्रिधा ॥ २७ ॥ तत्र पुण्याशयः पूर्वस्तद्विपक्षोऽशुभाशयः । शुद्धोपयोगसंज्ञो यः स तृतीयः प्रकीर्तितः ॥ २८ ॥ (ग) निश्चयाद् वा व्यवहराद् वा ध्यानं द्विविधमागमे ।
स्वरूपालम्बनं पूर्वं परालम्बनमुत्तरम् ॥
(घ) स्वात्मानं स्वात्मनिस्वेन ध्यायेत् स्वस्य स्वतो यतः । षट्कारकमयस्तस्माद् ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ २. (क) जस्स ण विज्जदि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो ।
तस्स सुहासुहडहणो झाणमओ जायए अगणी ॥ (ख) इष्टानिष्टार्थ - मोहादिच्छेदाच्चेतः स्थिरं यतः । षट्कारकमयस्तस्मान्मोक्षस्ततः सुखम् ॥
Jain Education International
- तत्त्वानुशासन ९६
- वही, श्लो. ७४
— पंचास्तिकाय १४६
- अनगार धर्मामृत १/११४/११७
- ज्ञानार्णव ३/२७-२८
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org