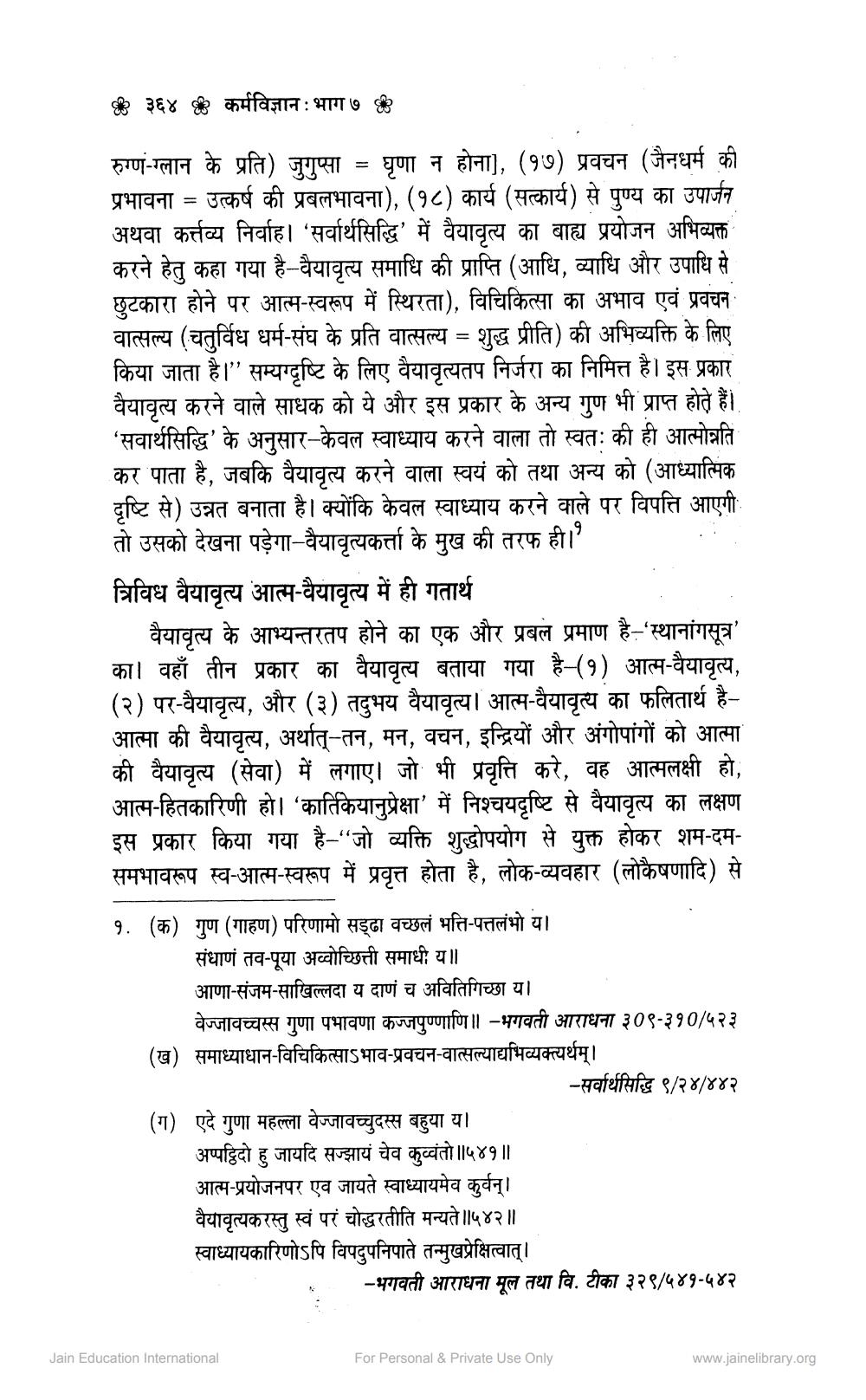________________
३६४ कर्मविज्ञान : भाग ७
प्रभावना
रुग्ण - ग्लान के प्रति ) जुगुप्सा घृणा न होना], (१७) प्रवचन (जैनधर्म की उत्कर्ष की प्रबलभावना), (१८) कार्य (सत्कार्य) से पुण्य का उपार्जन अथवा कर्त्तव्य निर्वाह । 'सर्वार्थसिद्धि' में वैयावृत्य का बाह्य प्रयोजन अभिव्यक्त करने हेतु कहा गया है - वैयावृत्य समाधि की प्राप्ति (आधि, व्याधि और उपाधि से छुटकारा होने पर आत्म - स्वरूप में स्थिरता ), विचिकित्सा का अभाव एवं प्रवचन वात्सल्य (चतुर्विध धर्म-संघ के प्रति वात्सल्य शुद्ध प्रीति) की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है।” सम्यग्दृष्टि के लिए वैयावृत्यतप निर्जरा का निमित्त है। इस प्रकार वैयावृत्य करने वाले साधक को ये और इस प्रकार के अन्य गुण भी प्राप्त होते हैं। 'सवार्थसिद्धि' के अनुसार - केवल स्वाध्याय करने वाला तो स्वतः की ही आत्मोन्नति कर पाता है, जबकि वैयावृत्य करने वाला स्वयं को तथा अन्य को (आध्यात्मिक दृष्टि से ) उन्नत बनाता है। क्योंकि केवल स्वाध्याय करने वाले पर विपत्ति आएगी. तो उसको देखना पड़ेगा-वैयावृत्यकर्त्ता के मुख की तरफ ही । '
=
ख
=
त्रिविध वैयावृत्य आत्म-वैयावृत्य में ही गतार्थ
वैयावृत्य के आभ्यन्तरतप होने का एक और प्रबल प्रमाण है - ' स्थानांगसूत्र' का। वहाँ तीन प्रकार का वैयावृत्य बताया गया है - ( 9 ) आत्म - वैयावृत्य, (२) पर - वैयावृत्य, और (३) तदुभय वैयावृत्य । आत्म-वैयावृत्य का फलितार्थ हैआत्मा की वैयावृत्य, अर्थात् - तन, मन, वचन, इन्द्रियों और अंगोपांगों को आत्मा की वैयावृत्य (सेवा) में लगाए । जो भी प्रवृत्ति करे, वह आत्मलक्षी हो, आत्म-हितकारिणी हो। ‘कार्तिकेयानुप्रेक्षा' में निश्चयदृष्टि से वैयावृत्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है - " जो व्यक्ति शुद्धोपयोग से युक्त होकर शम-दमसमभावरूप स्व-आत्म-स्वरूप में प्रवृत्त होता है, लोक व्यवहार ( लोकैषणादि) से
=
9. (क) गुण (गाहण) परिणामो सड्ढा वच्छलं भत्ति - पत्तलंभो य ।
संधाणं तव-पूया अव्वोच्छित्ती समाधी य ॥
आणा -संजम - साखिल्लदा य दाणं च अवितिगिच्छा य ।
वेज्जावच्च गुणा पभावणा कज्जपुण्णाणि ॥ - भगवती आराधना ३०९-३१०/५२३ समाध्याधान-विचिकित्साऽभाव-प्रवचन-वात्सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थम् ।
- सर्वार्थसिद्धि ९/२४/४४२
Jain Education International
(ग) एदे गुणा महल्ला वेज्जावच्चुदस्स बहुया य । अप्पट्ठिदो हु जायदि सज्झायं चेव कुव्वंतो ॥५४१ ॥ आत्म-प्रयोजनपर एव जायते स्वाध्यायमेव कुर्वन् । वैयावृत्यकरस्तु स्वं परं चोद्धरतीति मन्यते ॥५४२॥ स्वाध्यायकारिणोऽपि विपदुपनिपाते तन्मुखप्रेक्षित्वात् ।
-भगवती आराधना मूल तथा वि. टीका ३२९/५४१-५४२
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org