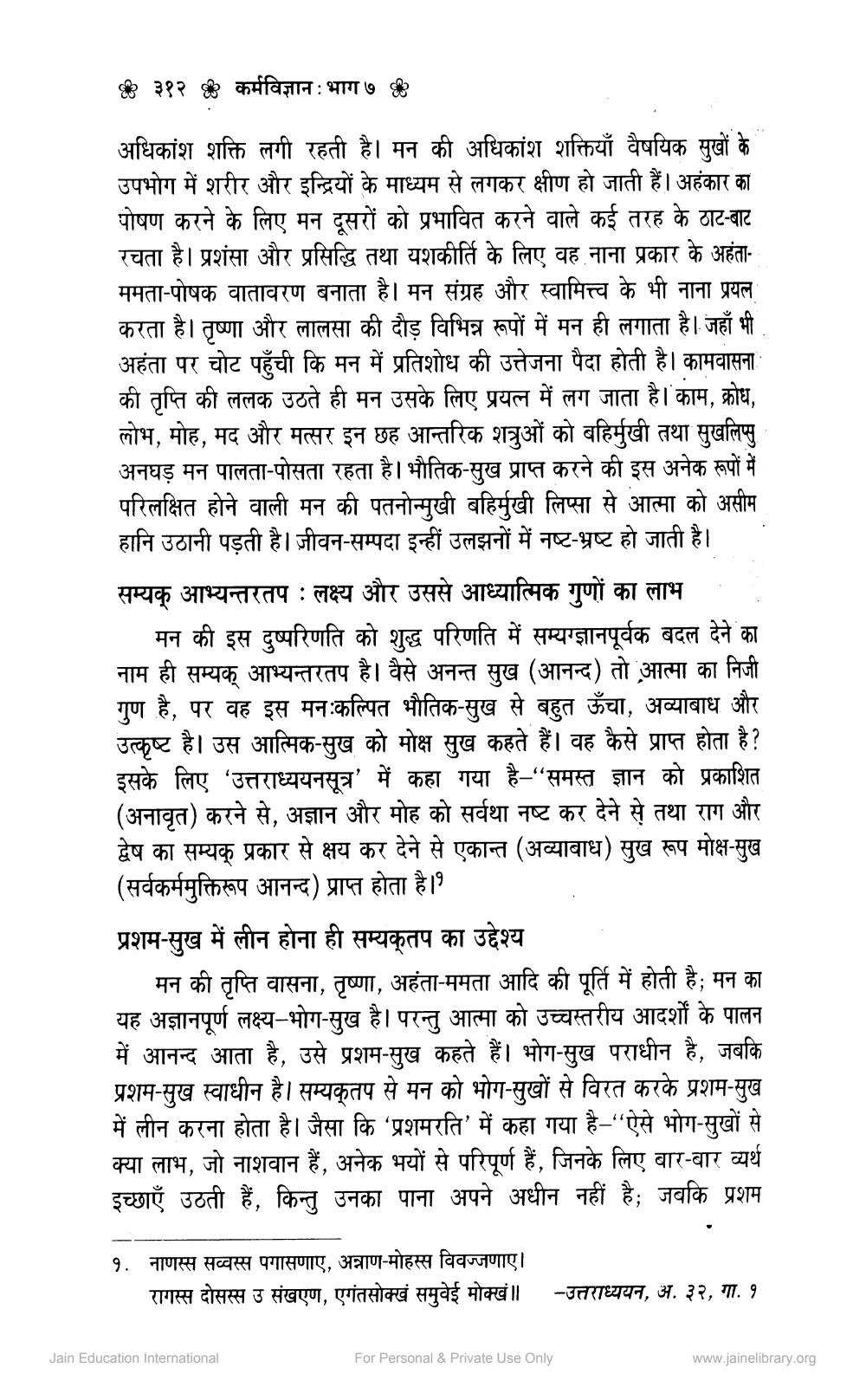________________
ॐ ३१२ ® कर्मविज्ञान : भाग ७ 8
अधिकांश शक्ति लगी रहती है। मन की अधिकांश शक्तियाँ वैषयिक सुखों के उपभोग में शरीर और इन्द्रियों के माध्यम से लगकर क्षीण हो जाती हैं। अहंकार का पोषण करने के लिए मन दूसरों को प्रभावित करने वाले कई तरह के ठाट-बाट रचता है। प्रशंसा और प्रसिद्धि तथा यशकीर्ति के लिए वह नाना प्रकार के अहंताममता-पोषक वातावरण बनाता है। मन संग्रह और स्वामित्त्व के भी नाना प्रयत्न करता है। तृष्णा और लालसा की दौड़ विभिन्न रूपों में मन ही लगाता है। जहाँ भी अहंता पर चोट पहुँची कि मन में प्रतिशोध की उत्तेजना पैदा होती है। कामवासना की तृप्ति की ललक उठते ही मन उसके लिए प्रयत्न में लग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छह आन्तरिक शत्रुओं को बहिर्मुखी तथा सुखलिप्सु अनघड़ मन पालता-पोसता रहता है। भौतिक-सुख प्राप्त करने की इस अनेक रूपों में परिलक्षित होने वाली मन की पतनोन्मुखी बहिर्मुखी लिप्सा से आत्मा को असीम हानि उठानी पड़ती है। जीवन-सम्पदा इन्हीं उलझनों में नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है। सम्यक् आभ्यन्तरतप : लक्ष्य और उससे आध्यात्मिक गुणों का लाभ
मन की इस दुष्परिणति को शुद्ध परिणति में सम्यग्ज्ञानपूर्वक बदल देने का नाम ही सम्यक् आभ्यन्तरतप है। वैसे अनन्त सुख (आनन्द) तो आत्मा का निजी गुण है, पर वह इस मनःकल्पित भौतिक-सुख से बहुत ऊँचा, अव्याबाध और उत्कृष्ट है। उस आत्मिक-सुख को मोक्ष सुख कहते हैं। वह कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए 'उत्तराध्ययनसूत्र' में कहा गया है-“समस्त ज्ञान को प्रकाशित (अनावृत) करने से, अज्ञान और मोह को सर्वथा नष्ट कर देने से तथा राग और द्वेष का सम्यक् प्रकार से क्षय कर देने से एकान्त (अव्याबाध) सुख रूप मोक्ष-सुख (सर्वकर्ममुक्तिरूप आनन्द) प्राप्त होता है। प्रशम-सुख में लीन होना ही सम्यक्तप का उद्देश्य
मन की तृप्ति वासना, तृष्णा, अहंता-ममता आदि की पूर्ति में होती है; मन का यह अज्ञानपूर्ण लक्ष्य-भोग-सुख है। परन्तु आत्मा को उच्चस्तरीय आदर्शों के पालन में आनन्द आता है, उसे प्रशम-सुख कहते हैं। भोग-सुख पराधीन है, जबकि प्रशम-सुख स्वाधीन है। सम्यक्तप से मन को भोग-सुखों से विरत करके प्रशम-सुख में लीन करना होता है। जैसा कि 'प्रशमरति' में कहा गया है-“ऐसे भोग-सुखों से क्या लाभ, जो नाशवान हैं, अनेक भयों से परिपूर्ण हैं, जिनके लिए बार-बार व्यर्थ इच्छाएँ उठती हैं, किन्तु उनका पाना अपने अधीन नहीं है। जबकि प्रशम
१. नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, अन्नाण-मोहस्स विवज्जणाए।
रागस्स दोसस्स उ संखएण, एगंतसोखं समुवेई मोक्खं॥
-उत्तराध्ययन, अ. ३२, गा. १
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org