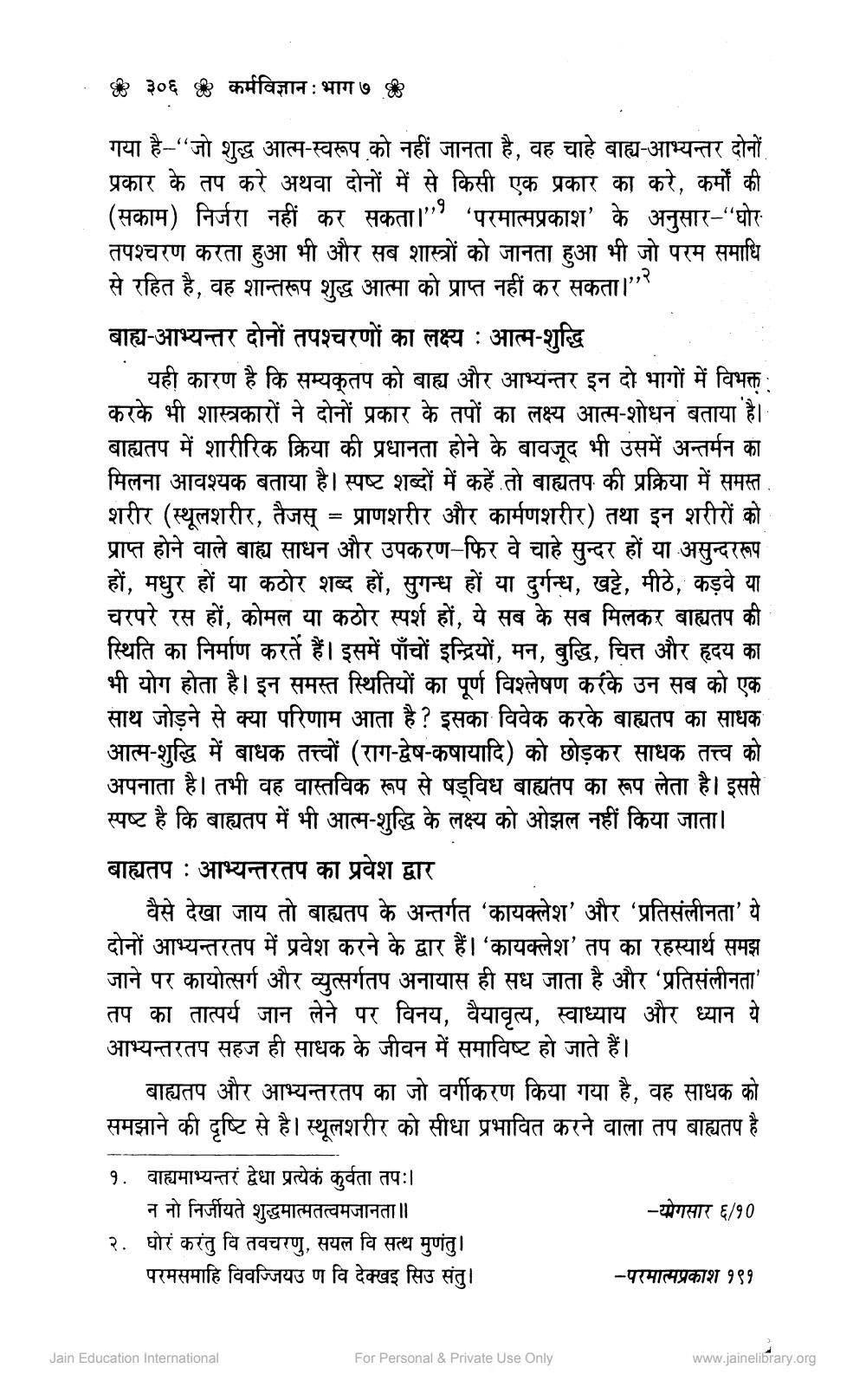________________
ॐ ३०६ 8 कर्मविज्ञान : भाग ७ *
गया है-"जो शुद्ध आत्म-स्वरूप को नहीं जानता है, वह चाहे बाह्य-आभ्यन्तर दोनों प्रकार के तप करे अथवा दोनों में से किसी एक प्रकार का करे, कर्मों की (सकाम) निर्जरा नहीं कर सकता।" ‘परमात्मप्रकाश' के अनुसार-"घोर तपश्चरण करता हुआ भी और सब शास्त्रों को जानता हुआ भी जो परम समाधि से रहित है, वह शान्तरूप शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता।" बाह्य-आभ्यन्तर दोनों तपश्चरणों का लक्ष्य : आत्म-शद्धि - यही कारण है कि सम्यक्तप को बाह्य और आभ्यन्तर इन दो भागों में विभक्त करके भी शास्त्रकारों ने दोनों प्रकार के तपों का लक्ष्य आत्म-शोधन बताया है। बाह्यतप में शारीरिक क्रिया की प्रधानता होने के बावजूद भी उसमें अन्तर्मन का मिलना आवश्यक बताया है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो बाह्यतप की प्रक्रिया में समस्त शरीर (स्थूलशरीर, तैजस = प्राणशरीर और कार्मणशरीर) तथा इन शरीरों को प्राप्त होने वाले बाह्य साधन और उपकरण-फिर वे चाहे सुन्दर हों या असुन्दररूप हों, मधुर हों या कठोर शब्द हों, सुगन्ध हों या दुर्गन्ध, खट्टे, मीठे, कड़वे या चरपरे रस हों, कोमल या कठोर स्पर्श हों, ये सब के सब मिलकर बाह्यतप की स्थिति का निर्माण करते हैं। इसमें पाँचों इन्द्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और हृदय का भी योग होता है। इन समस्त स्थितियों का पूर्ण विश्लेषण करके उन सब को एक साथ जोड़ने से क्या परिणाम आता है ? इसका विवेक करके बाह्यतप का साधक आत्म-शुद्धि में बाधक तत्त्वों (राग-द्वेष-कषायादि) को छोड़कर साधक तत्त्व को अपनाता है। तभी वह वास्तविक रूप से षड्विध बाह्यतप का रूप लेता है। इससे स्पष्ट है कि बाह्यतप में भी आत्म-शुद्धि के लक्ष्य को ओझल नहीं किया जाता।
बाह्यतप : आभ्यन्तरतप का प्रवेश द्वार
वैसे देखा जाय तो बाह्यतप के अन्तर्गत 'कायक्लेश' और 'प्रतिसंलीनता' ये दोनों आभ्यन्तरतप में प्रवेश करने के द्वार हैं। 'कायक्लेश' तप का रहस्यार्थ समझ जाने पर कायोत्सर्ग और व्युत्सर्गतप अनायास ही सध जाता है और प्रतिसंलीनता' तप का तात्पर्य जान लेने पर विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और ध्यान ये आभ्यन्तरतप सहज ही साधक के जीवन में समाविष्ट हो जाते हैं।
बाह्यतप और आभ्यन्तरतप का जो वर्गीकरण किया गया है, वह साधक को समझाने की दृष्टि से है। स्थूलशरीर को सीधा प्रभावित करने वाला तप बाह्यतप है १. वाह्यमाभ्यन्तरं द्वेधा प्रत्येकं कुर्वता तपः। न नो निर्जीयते शुद्धमात्मतत्वमजानता॥
-योगसार ६/१० २. घोरं करंतु वि तवचरणु, सयल वि सत्थ मुणंतु।
परमसमाहि विवज्जियउ ण वि देखइ सिउ संतु।
-परमात्मप्रकाश १९१
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org