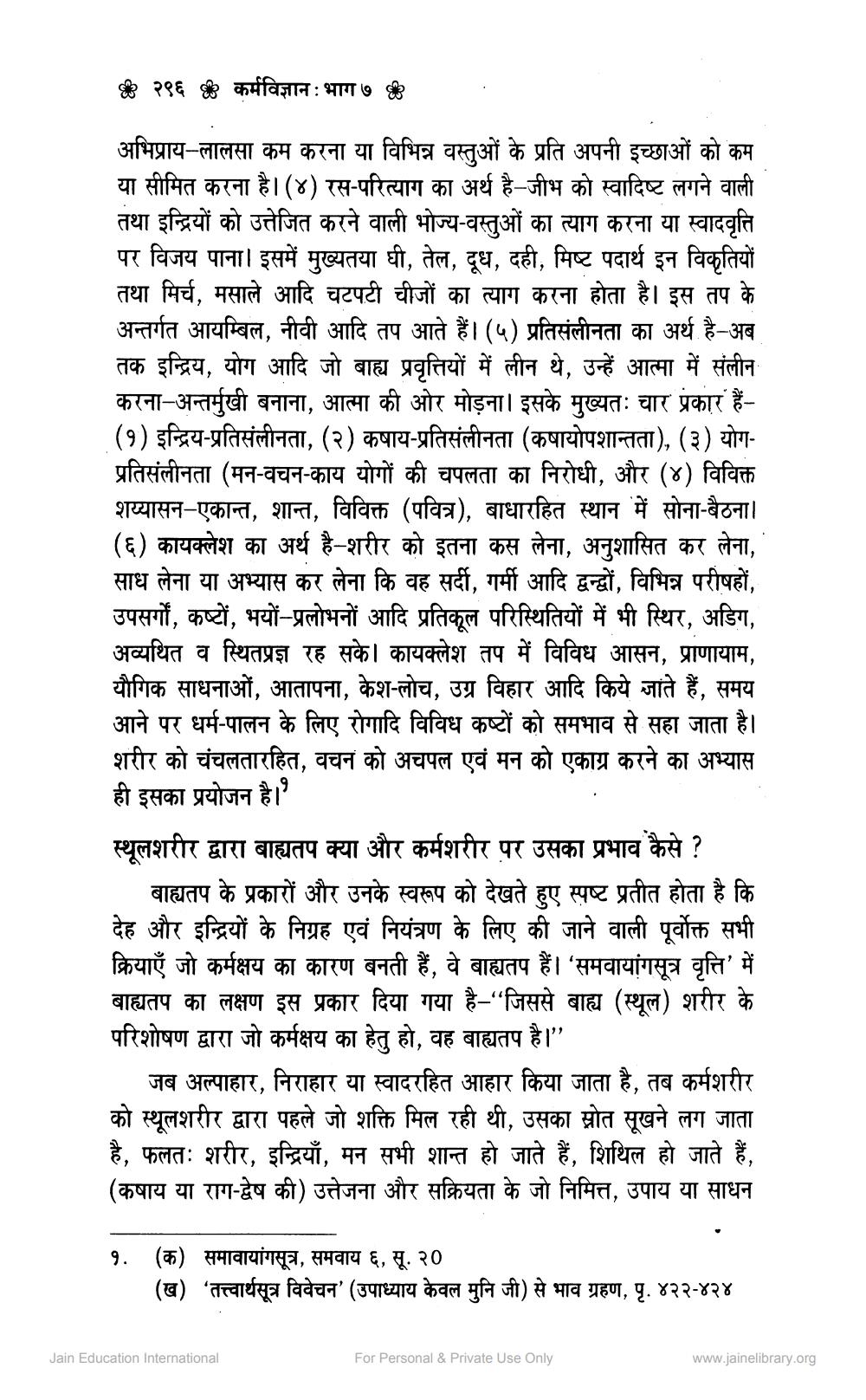________________
® २९६ ॐ कर्मविज्ञान : भाग ७ *
अभिप्राय-लालसा कम करना या विभिन्न वस्तुओं के प्रति अपनी इच्छाओं को कम या सीमित करना है। (४) रस-परित्याग का अर्थ है-जीभ को स्वादिष्ट लगने वाली तथा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाली भोज्य-वस्तुओं का त्याग करना या स्वादवृत्ति पर विजय पाना। इसमें मुख्यतया घी, तेल, दूध, दही, मिष्ट पदार्थ इन विकृतियों तथा मिर्च, मसाले आदि चटपटी चीजों का त्याग करना होता है। इस तप के अन्तर्गत आयम्बिल, नीवी आदि तप आते हैं। (५) प्रतिसंलीनता का अर्थ है-अब तक इन्द्रिय, योग आदि जो बाह्य प्रवृत्तियों में लीन थे, उन्हें आत्मा में संलीन करना-अन्तर्मुखी बनाना, आत्मा की ओर मोड़ना। इसके मुख्यतः चार प्रकार हैं(१) इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता, (२) कषाय-प्रतिसंलीनता (कषायोपशान्तता), (३) योगप्रतिसंलीनता (मन-वचन-काय योगों की चपलता का निरोधी, और (४) विविक्त शय्यासन-एकान्त, शान्त, विविक्त (पवित्र), बाधारहित स्थान में सोना-बैठना। (६) कायक्लेश का अर्थ है-शरीर को इतना कस लेना, अनुशासित कर लेना, साध लेना या अभ्यास कर लेना कि वह सर्दी, गर्मी आदि द्वन्द्वों, विभिन्न परीषहों, उपसर्गों, कष्टों, भयों-प्रलोभनों आदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर, अडिग, अव्यथित व स्थितप्रज्ञ रह सके। कायक्लेश तप में विविध आसन, प्राणायाम, यौगिक साधनाओं, आतापना, केश-लोच, उग्र विहार आदि किये जाते हैं, समय आने पर धर्म-पालन के लिए रोगादि विविध कष्टों को समभाव से सहा जाता है। शरीर को चंचलतारहित, वचन को अचपल एवं मन को एकाग्र करने का अभ्यास ही इसका प्रयोजन है।' स्थूलशरीर द्वारा बाह्यतप क्या और कर्मशरीर पर उसका प्रभाव कैसे ? ___ बाह्यतप के प्रकारों और उनके स्वरूप को देखते हुए स्पष्ट प्रतीत होता है कि देह और इन्द्रियों के निग्रह एवं नियंत्रण के लिए की जाने वाली पूर्वोक्त सभी क्रियाएँ जो कर्मक्षय का कारण बनती हैं, वे बाह्यतप हैं। 'समवायांगसूत्र वृत्ति' में बाह्यतप का लक्षण इस प्रकार दिया गया है-“जिससे बाह्य (स्थूल) शरीर के परिशोषण द्वारा जो कर्मक्षय का हेतु हो, वह बाह्यतप है।"
जब अल्पाहार, निराहार या स्वादरहित आहार किया जाता है, तब कर्मशरीर को स्थूलशरीर द्वारा पहले जो शक्ति मिल रही थी, उसका स्रोत सूखने लग जाता है, फलतः शरीर, इन्द्रियाँ, मन सभी शान्त हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, (कषाय या राग-द्वेष की) उत्तेजना और सक्रियता के जो निमित्त, उपाय या साधन
१. (क) समावायांगसूत्र, समवाय ६, सू. २०
(ख) 'तत्त्वार्थसूत्र विवेचन' (उपाध्याय केवल मुनि जी) से भाव ग्रहण, पृ. ४२२-४२४
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org