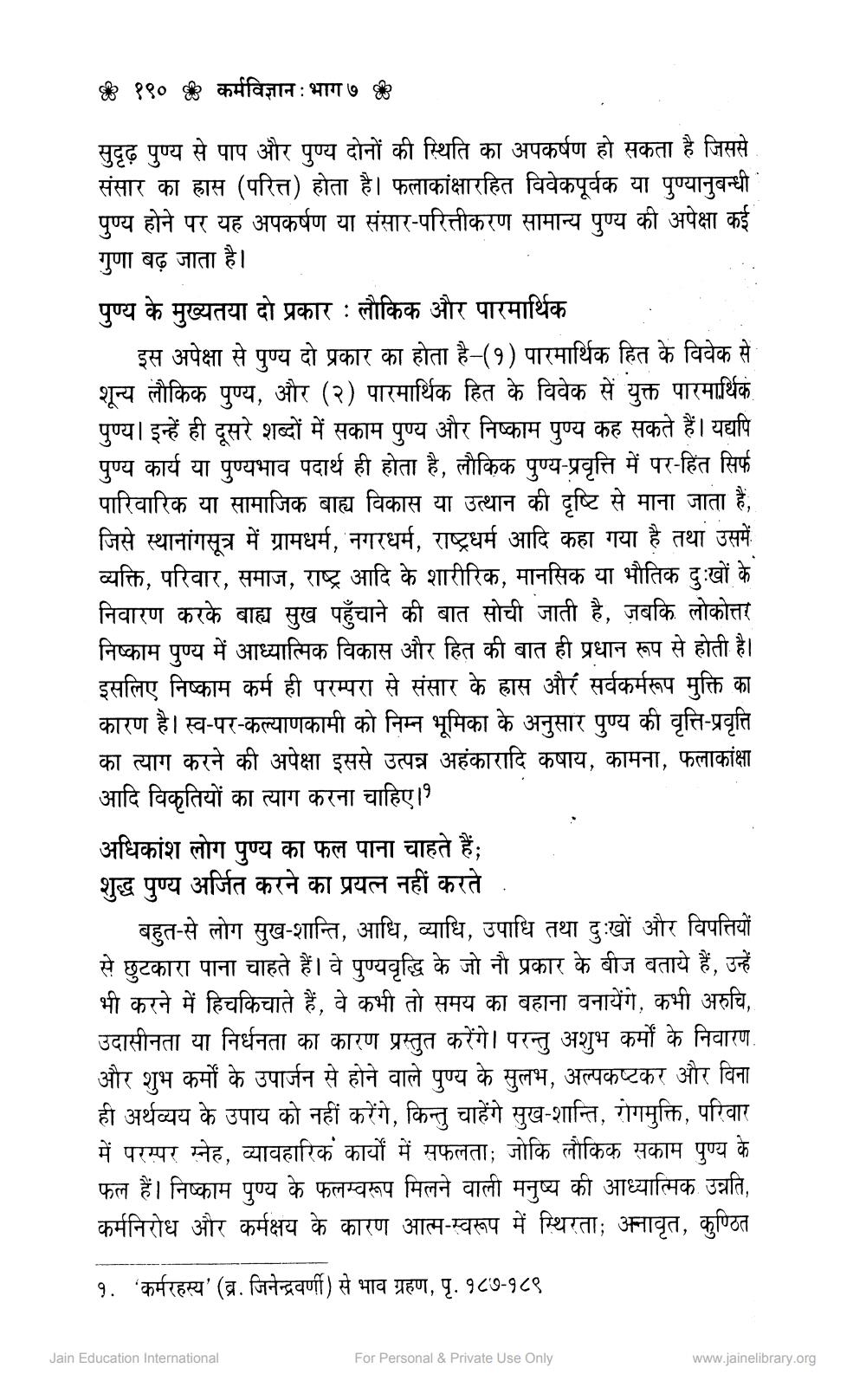________________
* १९० * कर्मविज्ञान : भाग ७ ॐ
सुदृढ़ पुण्य से पाप और पुण्य दोनों की स्थिति का अपकर्षण हो सकता है जिससे संसार का ह्रास (परित्त) होता है। फलाकांक्षारहित विवेकपूर्वक या पुण्यानुबन्धी पुण्य होने पर यह अपकर्षण या संसार-परित्तीकरण सामान्य पुण्य की अपेक्षा कई गुणा बढ़ जाता है। पुण्य के मुख्यतया दो प्रकार : लौकिक और पारमार्थिक __इस अपेक्षा से पुण्य दो प्रकार का होता है-(१) पारमार्थिक हित के विवेक से शून्य लौकिक पुण्य, और (२) पारमार्थिक हित के विवेक से युक्त पारमार्थिक पुण्य। इन्हें ही दूसरे शब्दों में सकाम पुण्य और निष्काम पुण्य कह सकते हैं। यद्यपि पुण्य कार्य या पुण्यभाव पदार्थ ही होता है, लौकिक पुण्य-प्रवृत्ति में पर-हित सिर्फ पारिवारिक या सामाजिक बाह्य विकास या उत्थान की दृष्टि से माना जाता हैं, जिसे स्थानांगसूत्र में ग्रामधर्म, नगरधर्म, राष्ट्रधर्म आदि कहा गया है तथा उसमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र आदि के शारीरिक, मानसिक या भौतिक दुःखों के निवारण करके बाह्य सुख पहुँचाने की बात सोची जाती है, जबकि लोकोत्तर निष्काम पुण्य में आध्यात्मिक विकास और हित की बात ही प्रधान रूप से होती है। इसलिए निष्काम कर्म ही परम्परा से संसार के ह्रास और सर्वकर्मरूप मुक्ति का कारण है। स्व-पर-कल्याणकामी को निम्न भूमिका के अनुसार पुण्य की वृत्ति-प्रवृत्ति का त्याग करने की अपेक्षा इससे उत्पन्न अहंकारादि कषाय, कामना, फलाकांक्षा आदि विकृतियों का त्याग करना चाहिए।' अधिकांश लोग पुण्य का फल पाना चाहते हैं; शुद्ध पुण्य अर्जित करने का प्रयत्न नहीं करते ___ बहुत-से लोग सुख-शान्ति, आधि, व्याधि, उपाधि तथा दुःखों और विपत्तियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वे पुण्यवृद्धि के जो नौ प्रकार के बीज बताये हैं, उन्हें भी करने में हिचकिचाते हैं, वे कभी तो समय का बहाना बनायेंगे, कभी अरुचि, उदासीनता या निर्धनता का कारण प्रस्तुत करेंगे। परन्तु अशुभ कर्मों के निवारण. और शुभ कर्मों के उपार्जन से होने वाले पुण्य के सुलभ, अल्पकष्टकर और विना ही अर्थव्यय के उपाय को नहीं करेंगे, किन्तु चाहेंगे सुख-शान्ति, रोगमुक्ति, परिवार में परस्पर स्नेह, व्यावहारिक कार्यों में सफलता; जोकि लौकिक सकाम पुण्य के फल हैं। निष्काम पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाली मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति, कर्मनिरोध और कर्मक्षय के कारण आत्म-स्वरूप में स्थिरता; अनावृत, कुण्ठित
१. 'कर्मरहस्य' (व्र. जिनेन्द्रवर्णी) से भाव ग्रहण, पृ. १८७-१८९
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org