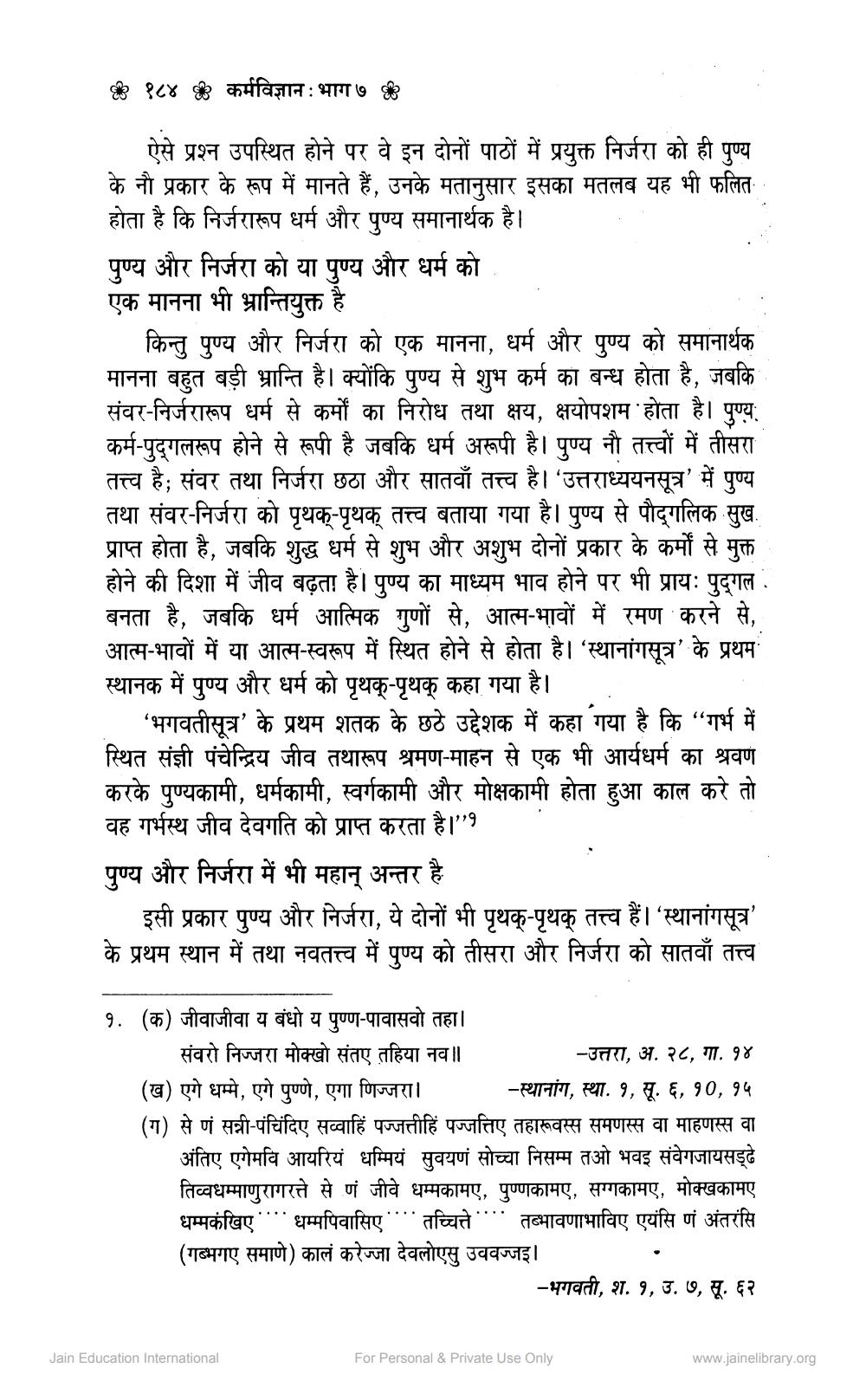________________
* १८४ ॐ कर्मविज्ञान : भाग ७ *
___ ऐसे प्रश्न उपस्थित होने पर वे इन दोनों पाठों में प्रयुक्त निर्जरा को ही पुण्य के नौ प्रकार के रूप में मानते हैं, उनके मतानुसार इसका मतलब यह भी फलित होता है कि निर्जरारूप धर्म और पुण्य समानार्थक है। पुण्य और निर्जरा को या पुण्य और धर्म को .. एक मानना भी भ्रान्तियुक्त है
किन्तु पुण्य और निर्जरा को एक मानना, धर्म और पुण्य को समानार्थक मानना बहुत बड़ी भ्रान्ति है। क्योंकि पुण्य से शुभ कर्म का बन्ध होता है, जबकि संवर-निर्जरारूप धर्म से कर्मों का निरोध तथा क्षय, क्षयोपशम होता है। पुण्यः कर्म-पुद्गलरूप होने से रूपी है जबकि धर्म अरूपी है। पुण्य नौ तत्त्वों में तीसरा तत्त्व है; संवर तथा निर्जरा छठा और सातवाँ तत्त्व है। ‘उत्तराध्ययनसूत्र' में पुण्य तथा संवर-निर्जरा को पृथक्-पृथक् तत्त्व बताया गया है। पुण्य से पौद्गलिक सुख. प्राप्त होता है, जबकि शुद्ध धर्म से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होने की दिशा में जीव बढ़ता है। पुण्य का माध्यम भाव होने पर भी प्रायः पुद्गल . बनता है, जबकि धर्म आत्मिक गुणों से, आत्म-भावों में रमण करने से, आत्म-भावों में या आत्म-स्वरूप में स्थित होने से होता है। 'स्थानांगसूत्र' के प्रथम स्थानक में पुण्य और धर्म को पृथक्-पृथक् कहा गया है।
__ 'भगवतीसूत्र' के प्रथम शतक के छठे उद्देशक में कहा गया है कि “गर्भ में स्थित संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव तथारूप श्रमण-माहन से एक भी आर्यधर्म का श्रवण करके पुण्यकामी, धर्मकामी, स्वर्गकामी और मोक्षकामी होता हुआ काल करे तो वह गर्भस्थ जीव देवगति को प्राप्त करता है।"१ । पुण्य और निर्जरा में भी महान् अन्तर है
इसी प्रकार पुण्य और निर्जरा, ये दोनों भी पृथक्-पृथक् तत्त्व हैं। 'स्थानांगसूत्र' के प्रथम स्थान में तथा नवतत्त्व में पुण्य को तीसरा और निर्जरा को सातवाँ तत्त्व
१. (क) जीवाजीवा य बंधो य पुण्ण-पावासवो तहा। संवरो निज्जरा मोक्खो संतए तहिया नव॥
-उत्तरा, अ. २८, गा.१४ (ख) एगे धम्मे, एगे पुण्णे, एगा णिज्जरा। -स्थानांग, स्था. १, सू. ६, १०, १५ (ग) से णं सन्नी-पंचिंदिए सव्वाहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तिए तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा
अंतिए एगेमवि आयरियं धम्मियं सुवयणं सोच्चा निसम्म तओ भवइ संवेगजायसड्ढे तिव्वधम्माणुरागरत्ते से णं जीवे धम्मकामए, पुण्णकामए, सग्गकामए, मोखकामए धम्मकंखिए धम्मपिवासिएतच्चित्ते तब्भावणाभाविए एयंसि णं अंतरंसि (गब्भगए समाणे) कालं करेज्जा देवलोएसु उववज्जइ।
-भगवती, श. १, उ. ७, सू. ६२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org