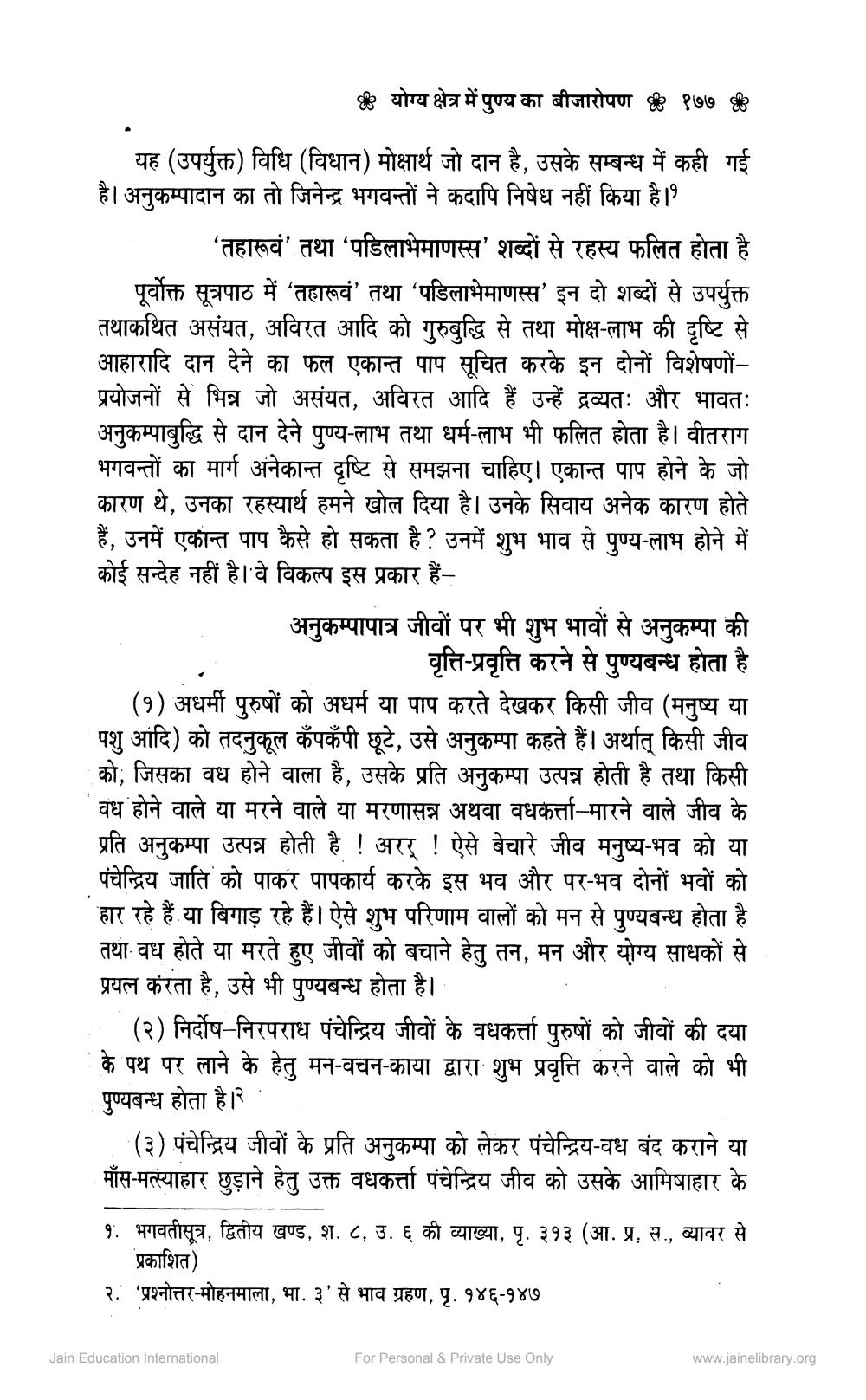________________
योग्य क्षेत्र में पुण्य का बीजारोपण ® १७७ 8
यह (उपर्युक्त) विधि (विधान) मोक्षार्थ जो दान है, उसके सम्बन्ध में कही गई है। अनुकम्पादान का तो जिनेन्द्र भगवन्तों ने कदापि निषेध नहीं किया है।
____ 'तहारूवं' तथा 'पडिला माणस्स' शब्दों से रहस्य फलित होता है पूर्वोक्त सूत्रपाठ में 'तहारूवं' तथा 'पडिलाभेमाणस्स' इन दो शब्दों से उपर्युक्त तथाकथित असंयत, अविरत आदि को गुरुबुद्धि से तथा मोक्ष-लाभ की दृष्टि से आहारादि दान देने का फल एकान्त पाप सूचित करके इन दोनों विशेषणोंप्रयोजनों से भिन्न जो असंयत, अविरत आदि हैं उन्हें द्रव्यतः और भावतः अनुकम्पाबुद्धि से दान देने पुण्य-लाभ तथा धर्म-लाभ भी फलित होता है। वीतराग भगवन्तों का मार्ग अनेकान्त दृष्टि से समझना चाहिए। एकान्त पाप होने के जो कारण थे, उनका रहस्यार्थ हमने खोल दिया है। उनके सिवाय अनेक कारण होते हैं, उनमें एकान्त पाप कैसे हो सकता है? उनमें शुभ भाव से पुण्य-लाभ होने में कोई सन्देह नहीं है। वे विकल्प इस प्रकार हैं
अनुकम्पापात्र जीवों पर भी शुभ भावों से अनुकम्पा की
वृत्ति-प्रवृत्ति करने से पुण्यबन्ध होता है (१) अधर्मी पुरुषों को अधर्म या पाप करते देखकर किसी जीव (मनुष्य या पशु आदि) को तदनुकूल कँपकँपी छूटे, उसे अनुकम्पा कहते हैं। अर्थात् किसी जीव को, जिसका वध होने वाला है, उसके प्रति अनुकम्पा उत्पन्न होती है तथा किसी वध होने वाले या मरने वाले या मरणासन्न अथवा वधकर्ता-मारने वाले जीव के प्रति अनुकम्पा उत्पन्न होती है ! अरर ! ऐसे बेचारे जीव मनुष्य-भव को या पंचेन्द्रिय जाति को पाकर पापकार्य करके इस भव और पर-भव दोनों भवों को हार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। ऐसे शुभ परिणाम वालों को मन से पुण्यबन्ध होता है तथा वध होते या मरते हुए जीवों को बचाने हेतु तन, मन और योग्य साधकों से प्रयत्न करता है, उसे भी पुण्यबन्ध होता है। - (२) निर्दोष-निरपराध पंचेन्द्रिय जीवों के वधकर्ता पुरुषों को जीवों की दया के पथ पर लाने के हेतु मन-वचन-काया द्वारा शुभ प्रवृत्ति करने वाले को भी पुण्यबन्ध होता है। . (३) पंचेन्द्रिय जीवों के प्रति अनुकम्पा को लेकर पंचेन्द्रिय-वध बंद कराने या माँस-मत्स्याहार छुड़ाने हेतु उक्त वधकर्ता पंचेन्द्रिय जीव को उसके आमिषाहार के १. भगवतीसूत्र, द्वितीय खण्ड, श. ८, उ. ६ की व्याख्या, पृ. ३१३ (आ. प्र. स., व्यावर से
प्रकाशित) २. 'प्रश्नोत्तर-मोहनमाला, भा. ३' से भाव ग्रहण, पृ. १४६-१४७
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org