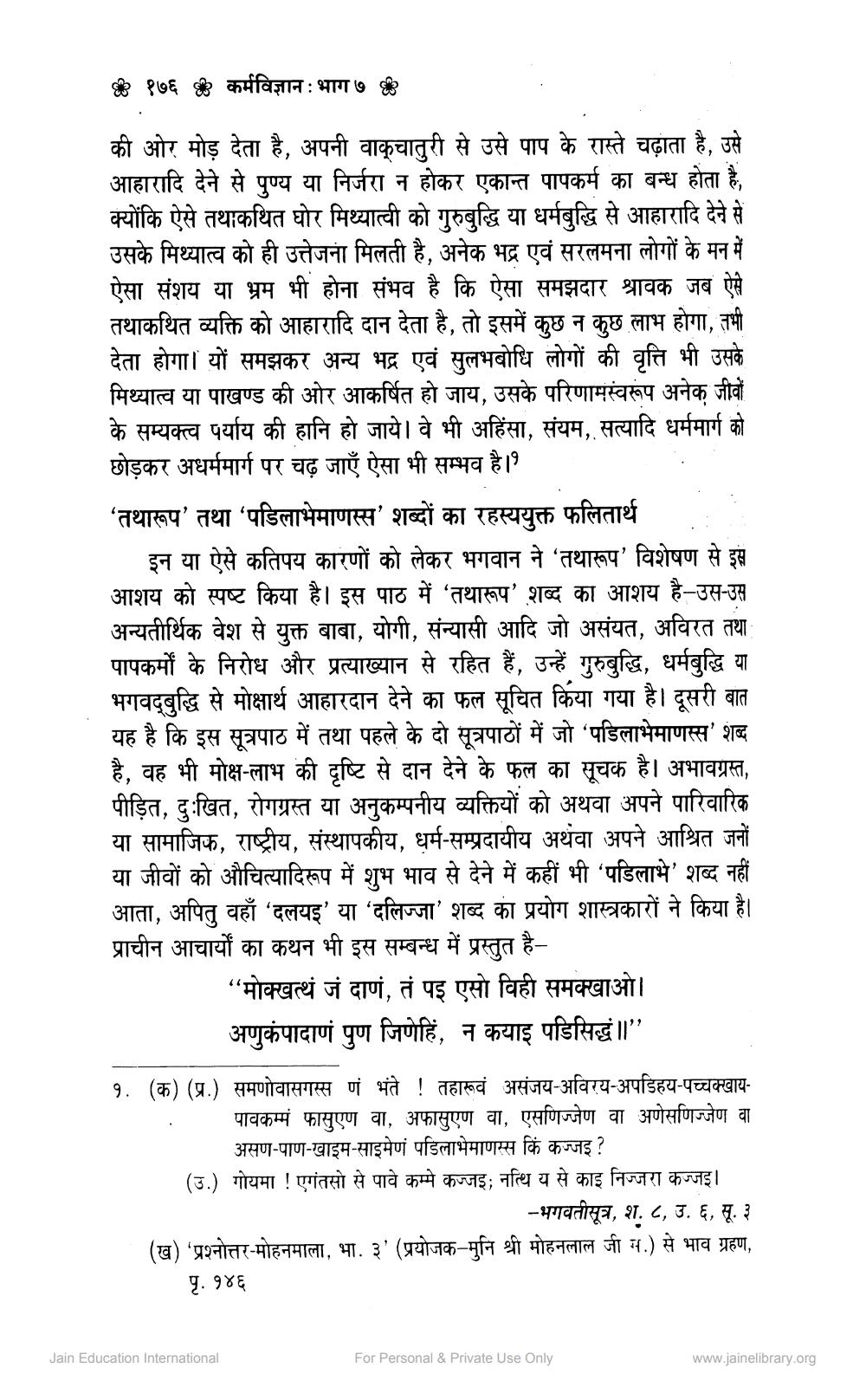________________
ॐ १७६ ® कर्मविज्ञान : भाग ७ ॐ
की ओर मोड़ देता है, अपनी वाक्चातुरी से उसे पाप के रास्ते चढ़ाता है, उसे आहारादि देने से पुण्य या निर्जरा न होकर एकान्त पापकर्म का बन्ध होता है, क्योंकि ऐसे तथाकथित घोर मिथ्यात्वी को गुरुबुद्धि या धर्मबुद्धि से आहारादि देने से उसके मिथ्यात्व को ही उत्तेजना मिलती है, अनेक भद्र एवं सरलमना लोगों के मन में ऐसा संशय या भ्रम भी होना संभव है कि ऐसा समझदार श्रावक जब ऐसे तथाकथित व्यक्ति को आहारादि दान देता है, तो इसमें कुछ न कुछ लाभ होगा, तभी देता होगा। यों समझकर अन्य भद्र एवं सुलभबोधि लोगों की वृत्ति भी उसके मिथ्यात्व या पाखण्ड की ओर आकर्षित हो जाय, उसके परिणामस्वरूप अनेक जीवों के सम्यक्त्व पर्याय की हानि हो जाये। वे भी अहिंसा, संयम, सत्यादि धर्ममार्ग को छोड़कर अधर्ममार्ग पर चढ़ जाएँ ऐसा भी सम्भव है।' 'तथारूप' तथा 'पडिला माणस्स' शब्दों का रहस्ययुक्त फलितार्थ
इन या ऐसे कतिपय कारणों को लेकर भगवान ने 'तथारूप' विशेषण से इस आशय को स्पष्ट किया है। इस पाठ में 'तथारूप' शब्द का आशय है-उस-उस अन्यतीर्थिक वेश से युक्त बाबा, योगी, संन्यासी आदि जो असंयत, अविरत तथा पापकर्मों के निरोध और प्रत्याख्यान से रहित हैं, उन्हें गुरुबुद्धि, धर्मबुद्धि या भगवद्बुद्धि से मोक्षार्थ आहारदान देने का फल सूचित किया गया है। दूसरी बात यह है कि इस सूत्रपाठ में तथा पहले के दो सूत्रपाठों में जो ‘पडिलाभेमाणस्स' शब्द है, वह भी मोक्ष-लाभ की दृष्टि से दान देने के फल का सूचक है। अभावग्रस्त, पीड़ित, दुःखित, रोगग्रस्त या अनुकम्पनीय व्यक्तियों को अथवा अपने पारिवारिक या सामाजिक, राष्ट्रीय, संस्थापकीय, धर्म-सम्प्रदायीय अर्थवा अपने आश्रित जनों या जीवों को औचित्यादिरूप में शुभ भाव से देने में कहीं भी ‘पडिलाभे' शब्द नहीं आता, अपितु वहाँ ‘दलयइ' या 'दलिज्जा' शब्द का प्रयोग शास्त्रकारों ने किया है। प्राचीन आचार्यों का कथन भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है
“मोक्खत्थं जं दाणं, तं पइ एसो विही समक्खाओ। अणुकंपादाणं पुण जिणेहिं, न कयाइ पडिसिद्धं ॥"
१. (क) (प्र.) समणोवासगस्स णं भंते ! तहारूवं असंजय-अविरय-अपडिहय-पच्चक्खाय
पावकम्मं फासुएण वा, अफासुएण वा, एसणिज्जेण वा अणेसणिज्जेण वा
असण-पाण-खाइम-साइमेणं पडिला माणस्स किं कज्जइ? (उ.) गोयमा ! एगंतसो से पावे कम्मे कज्जइ; नत्थि य से काइ निज्जरा कज्जइ।
-भगवतीसूत्र, श. ८, उ. ६, सू. ३ (ख) 'प्रश्नोत्तर-मोहनमाला, भा. ३' (प्रयोजक-मुनि श्री मोहनलाल जी म.) से भाव ग्रहण,
पृ. १४६
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org