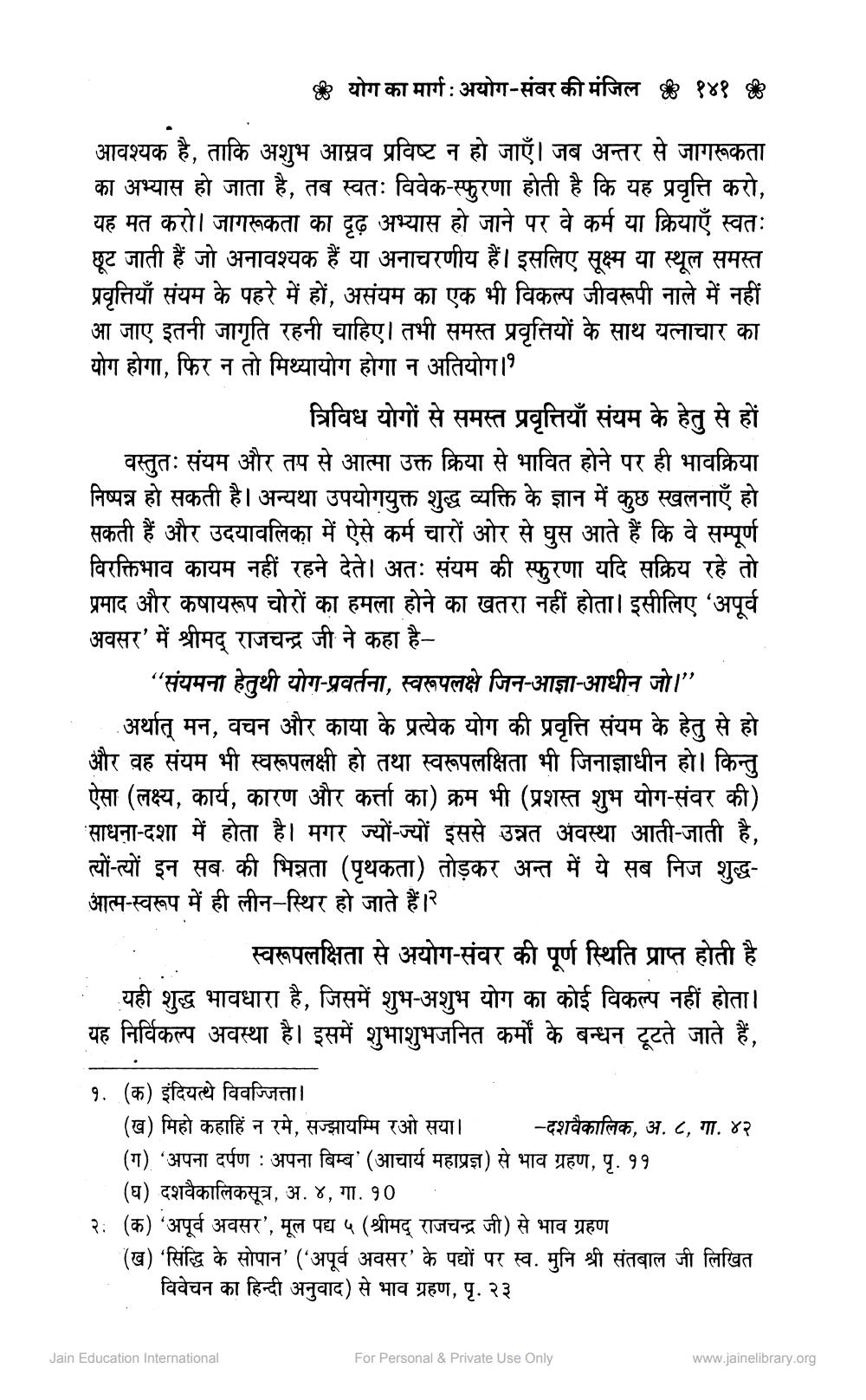________________
* योग का मार्ग : अयोग-संवर की मंजिल १४१
आवश्यक है, ताकि अशुभ आस्रव प्रविष्ट न हो जाएँ । जब अन्तर से जागरूकता का अभ्यास हो जाता है, तब स्वतः विवेक-स्फुरणा होती है कि यह प्रवृत्ति करो, यह मत करो। जागरूकता का दृढ़ अभ्यास हो जाने पर वे कर्म या क्रियाएँ स्वतः छूट जाती हैं जो अनावश्यक हैं या अनाचरणीय हैं। इसलिए सूक्ष्म या स्थूल समस्त प्रवृत्तियाँ संयम के पहरे में हों, असंयम का एक भी विकल्प जीवरूपी नाले में नहीं आ जाए इतनी जागृति रहनी चाहिए। तभी समस्त प्रवृत्तियों के साथ यत्नाचार का योग होगा, फिर न तो मिथ्यायोग होगा न अतियोग ।'
त्रिविध योगों से समस्त प्रवृत्तियाँ संयम के हेतु से हों
वस्तुतः संयम और तप से आत्मा उक्त क्रिया से भावित होने पर ही भावक्रिया निष्पन्न हो सकती है। अन्यथा उपयोगयुक्त शुद्ध व्यक्ति के ज्ञान में कुछ स्खलनाएँ हो सकती हैं और उदयावलिका में ऐसे कर्म चारों ओर से घुस आते हैं कि वे सम्पूर्ण विरक्तिभाव कायम नहीं रहने देते । अतः संयम की स्फुरणा यदि सक्रिय रहे तो प्रमाद और कषायरूप चोरों का हमला होने का खतरा नहीं होता। इसीलिए 'अपूर्व अवसर' में श्रीमद् राजचन्द्र जी ने कहा है
"संयमना हेतुथी योग-प्रवर्तना, स्वरूपलक्षे जिन - आज्ञा - आधीन जो ।”
• अर्थात् मन, वचन और काया के प्रत्येक योग की प्रवृत्ति संयम के हेतु से हो और वह संयम भी स्वरूपलक्षी हो तथा स्वरूपलक्षिता भी जिनाज्ञाधीन हो । किन्तु ऐसा (लक्ष्य, कार्य, कारण और कर्त्ता का) क्रम भी ( प्रशस्त शुभ योग - संवर की ) साधना - दशा में होता है। मगर ज्यों-ज्यों इससे उन्नत अवस्था आती जाती है, त्यों-त्यों इन सब की भिन्नता ( पृथकता ) तोड़कर अन्त में ये सब निज शुद्धआत्म-स्वरूप में ही लीन - स्थिर हो जाते हैं । २
स्वरूपलक्षिता से अयोग-संवर की पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है
यही शुद्ध भावधारा है, जिसमें शुभ-अशुभ योग का कोई विकल्प नहीं होता । यह निर्विकल्प अवस्था है। इसमें शुभाशुभजनित कर्मों के बन्धन टूटते जाते हैं,
१. (क) इंदियत्थे विवज्जित्ता ।
(ख) मिहो कहाहिं न रमे, सज्झायम्मि रओ सया ।
(ग) अपना दर्पण : अपना बिम्ब' (आचार्य महाप्रज्ञ) से भाव ग्रहण, पृ. ११ (घ) दशवैकालिकसूत्र, अ. ४, गा. १०
२. (क) 'अपूर्व अवसर', मूल पद्य ५ ( श्रीमद् राजचन्द्र जी ) से भाव ग्रहण
(ख) 'सिद्धि के सोपान' ('अपूर्व अवसर' के पद्यों पर स्व. मुनि श्री संतबाल जी लिखित विवेचन का हिन्दी अनुवाद) से भाव ग्रहण, पृ. २३
Jain Education International
- दशवैकालिक, अ. ८, गा. ४२
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org