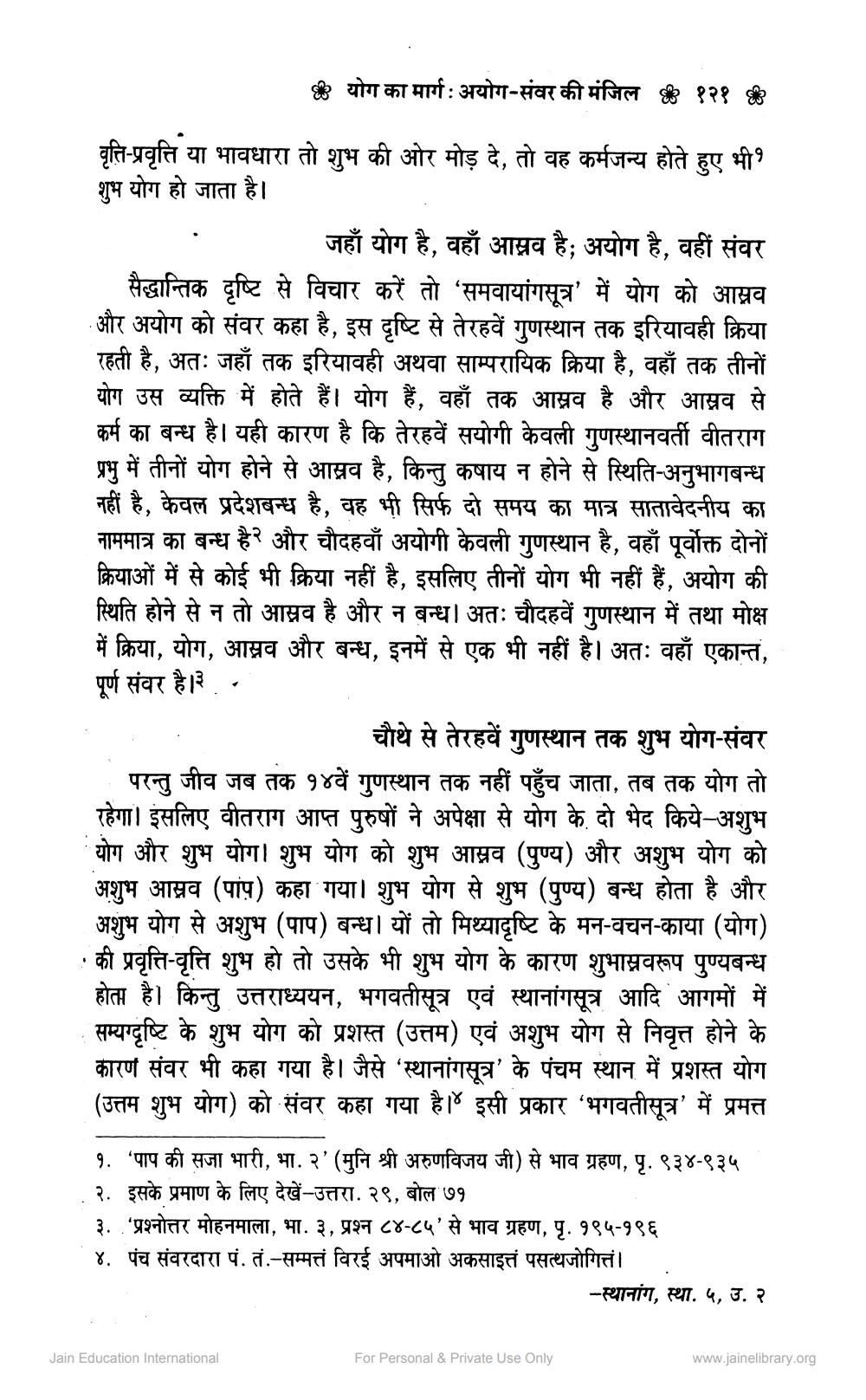________________
ॐ योग का मार्ग : अयोग-संवर की मंजिल ॐ १२१ ®
वृत्ति-प्रवृत्ति या भावधारा तो शुभ की ओर मोड़ दे, तो वह कर्मजन्य होते हुए भी शुभ योग हो जाता है।
जहाँ योग है, वहाँ आम्रव है; अयोग है, वहीं संवर सैद्धान्तिक दृष्टि से विचार करें तो 'समवायांगसूत्र' में योग को आसव और अयोग को संवर कहा है, इस दृष्टि से तेरहवें गुणस्थान तक इरियावही क्रिया रहती है, अतः जहाँ तक इरियावही अथवा साम्परायिक क्रिया है, वहाँ तक तीनों योग उस व्यक्ति में होते हैं। योग हैं, वहाँ तक आस्रव है और आस्रव से कर्म का बन्ध है। यही कारण है कि तेरहवें सयोगी केवली गुणस्थानवर्ती वीतराग प्रभु में तीनों योग होने से आस्रव है, किन्तु कषाय न होने से स्थिति-अनुभागबन्ध नहीं है, केवल प्रदेशबन्ध है, वह भी सिर्फ दो समय का मात्र सातावेदनीय का नाममात्र का बन्ध है और चौदहवाँ अयोगी केवली गुणस्थान है, वहाँ पूर्वोक्त दोनों क्रियाओं में से कोई भी क्रिया नहीं है, इसलिए तीनों योग भी नहीं हैं, अयोग की स्थिति होने से न तो आस्रव है और न बन्ध। अतः चौदहवें गुणस्थान में तथा मोक्ष में क्रिया, योग, आस्रव और बन्ध, इनमें से एक भी नहीं है। अतः वहाँ एकान्त, पूर्ण संवर है।३ .
चौथे से तेरहवें गुणस्थान तक शुभ योग-संवर . परन्तु जीव जब तक १४वें गुणस्थान तक नहीं पहुँच जाता, तब तक योग तो रहेगा। इसलिए वीतराग आप्त पुरुषों ने अपेक्षा से योग के दो भेद किये-अशुभ योग और शुभ योग। शुभ योग को शुभ आस्रव (पुण्य) और अशुभ योग को अशुभ आस्रव (पाप) कहा गया। शुभ योग से शुभ (पुण्य) बन्ध होता है और
अशुभ योग से अशुभ (पाप) बन्ध। यों तो मिथ्यादृष्टि के मन-वचन-काया (योग) • की प्रवृत्ति-वृत्ति शुभ हो तो उसके भी शुभ योग के कारण शुभानवरूप पुण्यबन्ध होता है। किन्तु उत्तराध्ययन, भगवतीसूत्र एवं स्थानांगसूत्र आदि आगमों में सम्यग्दृष्टि के शुभ योग को प्रशस्त (उत्तम) एवं अशुभ योग से निवृत्त होने के कारणं संवर भी कहा गया है। जैसे 'स्थानांगसूत्र' के पंचम स्थान में प्रशस्त योग (उत्तम शुभ योग) को संवर कहा गया है। इसी प्रकार ‘भगवतीसूत्र' में प्रमत्त १. ‘पाप की सजा भारी, भा. २' (मुनि श्री अरुणविजय जी) से भाव ग्रहण, पृ. ९३४-९३५ २. इसके प्रमाण के लिए देखें-उत्तरा. २९, बोल ७१ ३. 'प्रश्नोत्तर मोहनमाला, भा. ३, प्रश्न ८४-८५' से भाव ग्रहण, पृ. १९५-१९६ ४. पंच संवरदारा पं. तं.-सम्मत्तं विरई अपमाओ अकसाइत्तं पसत्थजोगित्तं।।
-स्थानांग, स्था. ५, उ. २
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org