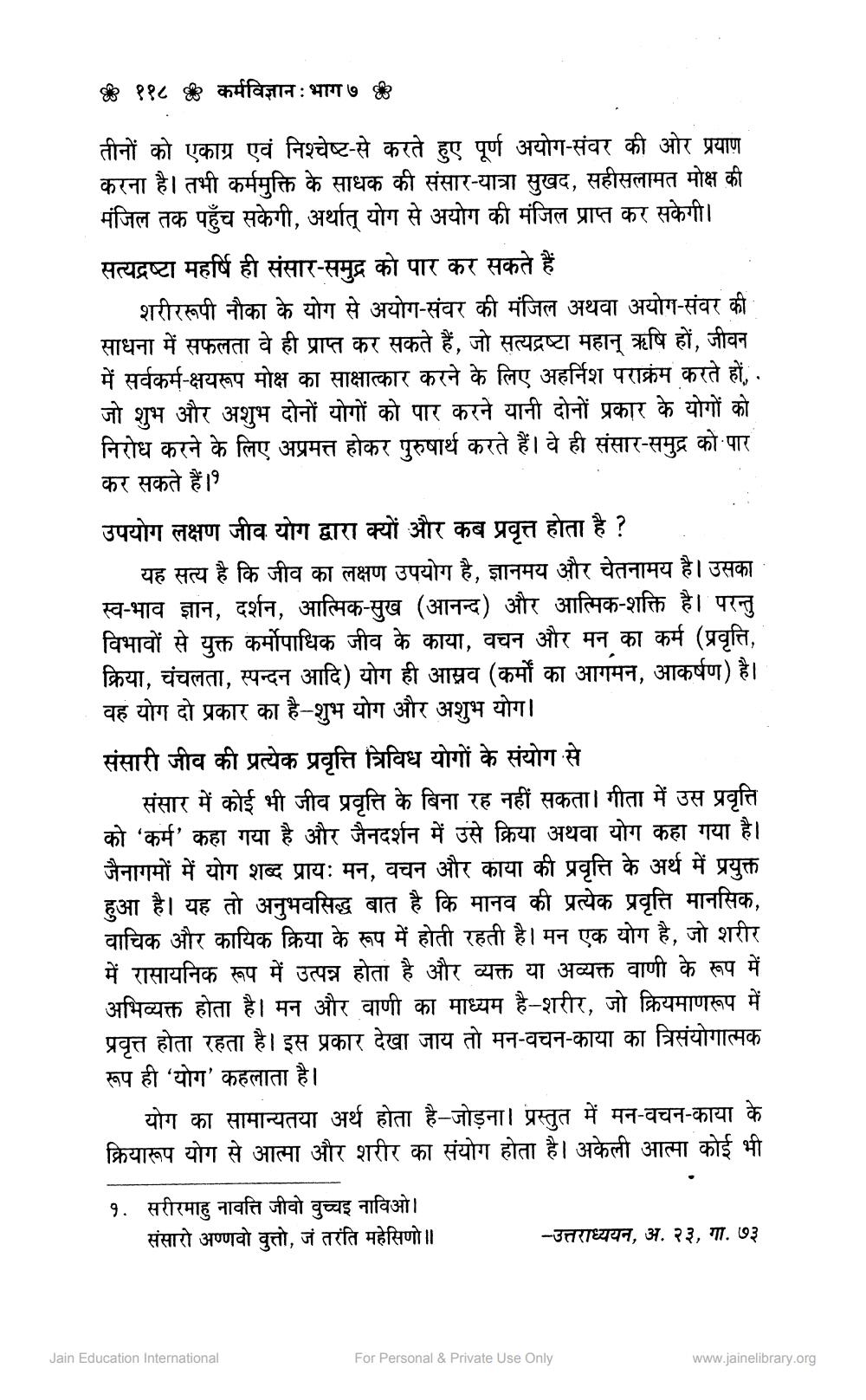________________
* ११८ कर्मविज्ञान : भाग ७
तीनों को एकाग्र एवं निश्चेष्ट से करते हुए पूर्ण अयोग-संवर की ओर प्रयाण करना है । तभी कर्ममुक्ति के साधक की संसार - यात्रा सुखद, सहीसलामत मोक्ष की मंजिल तक पहुँच सकेगी, अर्थात् योग से अयोग की मंजिल प्राप्त कर सकेगी।
सत्यद्रष्टा महर्षि ही संसार - समुद्र को पार कर सकते हैं
शरीररूपी नौका के योग से अयोग-संवर की मंजिल अथवा अयोग - संवर की साधना में सफलता वे ही प्राप्त कर सकते हैं, जो सत्यद्रष्टा महान् ऋषि हों, जीवन में सर्वकर्म-क्षयरूप मोक्ष का साक्षात्कार करने के लिए अहर्निश पराक्रम करते हों, . जो शुभ और अशुभ दोनों योगों को पार करने यानी दोनों प्रकार के योगों को निरोध करने के लिए अप्रमत्त होकर पुरुषार्थ करते हैं । वे ही संसार - समुद्र को पार कर सकते हैं । "
उपयोग लक्षण जीव योग द्वारा क्यों और कब प्रवृत्त होता है ?
यह सत्य है कि जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञानमय और चेतनामय है । उसका स्व-भाव ज्ञान, दर्शन, आत्मिक सुख (आनन्द) और आत्मिक शक्ति है। परन्तु विभावों से युक्त कर्मोपाधिक जीव के काया, वचन और मन का कर्म ( प्रवृत्ति, क्रिया, चंचलता, स्पन्दन आदि) योग ही आम्रव (कर्मों का आगमन, आकर्षण) है। वह योग दो प्रकार का है -शुभ योग और अशुभ योग ।
संसारी जीव की प्रत्येक प्रवृत्ति त्रिविध योगों के संयोग से
संसार में कोई भी जीव प्रवृत्ति के बिना रह नहीं सकता। गीता में उस प्रवृत्ति को 'कर्म' कहा गया है और जैनदर्शन में उसे क्रिया अथवा योग कहा गया है। जैनागमों में योग शब्द प्रायः मन, वचन और काया की प्रवृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह तो अनुभवसिद्ध बात है कि मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया के रूप में होती रहती है । मन एक योग है, जो शरीर में रासायनिक रूप में उत्पन्न होता है और व्यक्त या अव्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त होता है। मन और वाणी का माध्यम है- शरीर, जो क्रियमाणरूप में प्रवृत्त होता रहता है। इस प्रकार देखा जाय तो मन-वचन-काया का त्रिसंयोगात्मक रूप ही 'योग' कहलाता है।
योग का सामान्यतया अर्थ होता है - जोड़ना । प्रस्तुत में मन-वचन-काया के क्रियारूप योग से आत्मा और शरीर का संयोग होता है। अकेली आत्मा कोई भी
१. सरीरमाहु नावत्ति जीवो वुच्चइ नाविओ । संसारो अण्णवो वृत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥
Jain Education International
- उत्तराध्ययन, अ. २३, गा. ७३
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org