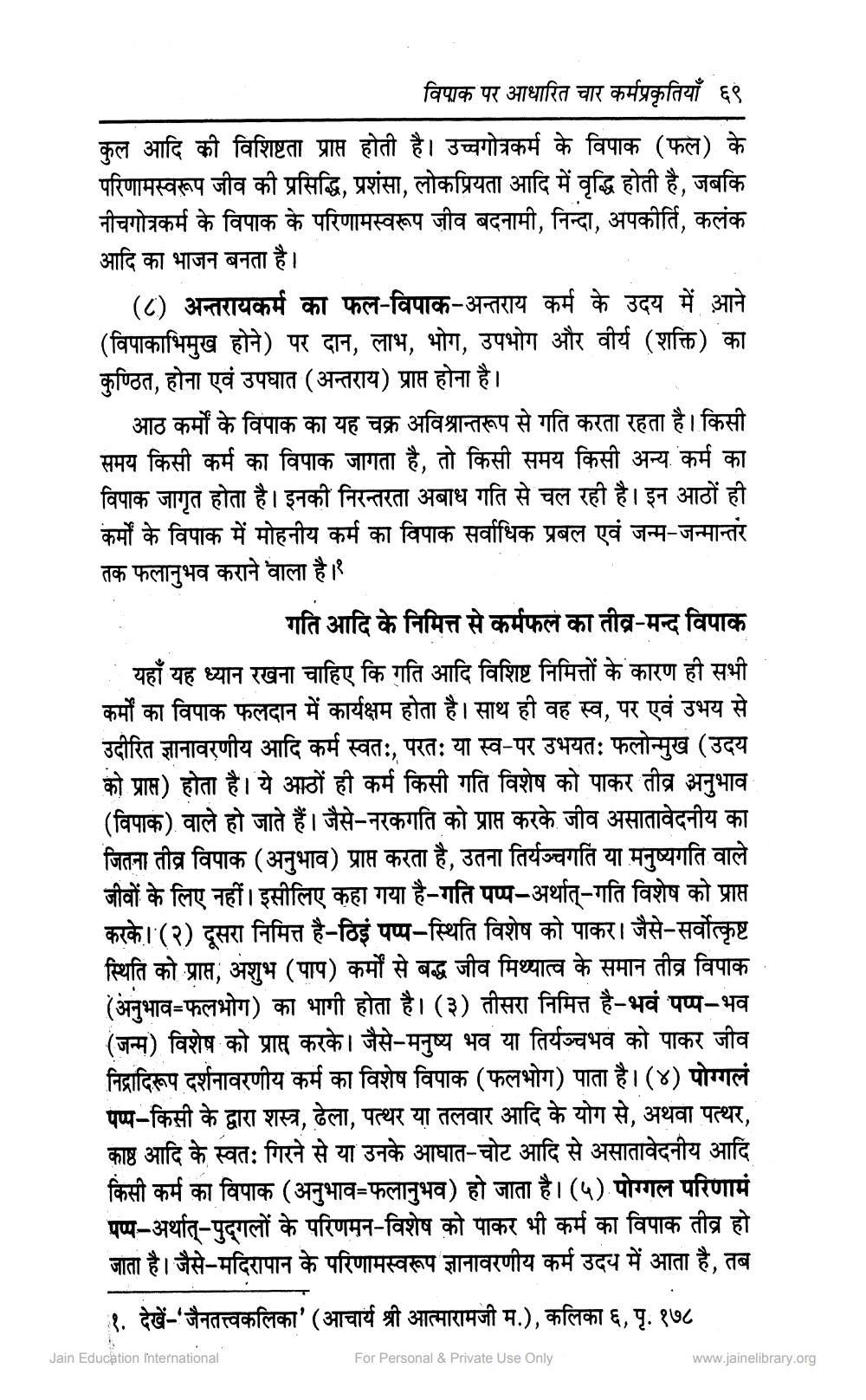________________
विपाक पर आधारित चार कर्मप्रकृतियाँ ६९ कुल आदि की विशिष्टता प्राप्त होती है। उच्चगोत्रकर्म के विपाक (फल) के परिणामस्वरूप जीव की प्रसिद्धि, प्रशंसा, लोकप्रियता आदि में वृद्धि होती है, जबकि नीचगोत्रकर्म के विपाक के परिणामस्वरूप जीव बदनामी, निन्दा, अपकीर्ति, कलंक आदि का भाजन बनता है।
(८) अन्तरायकर्म का फल-विपाक-अन्तराय कर्म के उदय में आने (विपाकाभिमुख होने) पर दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य (शक्ति) का कुण्ठित, होना एवं उपघात (अन्तराय) प्राप्त होना है।
आठ कर्मों के विपाक का यह चक्र अविश्रान्तरूप से गति करता रहता है। किसी समय किसी कर्म का विपाक जागता है, तो किसी समय किसी अन्य कर्म का विपाक जागृत होता है। इनकी निरन्तरता अबाध गति से चल रही है। इन आठों ही कर्मों के विपाक में मोहनीय कर्म का विपाक सर्वाधिक प्रबल एवं जन्म-जन्मान्तर तक फलानुभव कराने वाला है।
गति आदि के निमित्त से कर्मफल का तीव्र-मन्द विपाक - यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि गति आदि विशिष्ट निमित्तों के कारण ही सभी कर्मों का विपाक फलदान में कार्यक्षम होता है। साथ ही वह स्व, पर एवं उभय से उदीरित ज्ञानावरणीय आदि कर्म स्वतः, परतः या स्व-पर उभयतः फलोन्मुख (उदय को प्राप्त) होता है। ये आठों ही कर्म किसी गति विशेष को पाकर तीव्र अनुभाव (विपाक) वाले हो जाते हैं। जैसे-नरकगति को प्राप्त करके जीव असातावेदनीय का जितना तीव्र विपाक (अनुभाव) प्राप्त करता है, उतना तिर्यञ्चगति या मनुष्यगति वाले जीवों के लिए नहीं। इसीलिए कहा गया है-गति पप्प-अर्थात्-गति विशेष को प्राप्त करके। (२) दूसरा निमित्त है-ठिई पप्प-स्थिति विशेष को पाकर। जैसे-सर्वोत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त, अशुभ (पाप) कर्मों से बद्ध जीव मिथ्यात्व के समान तीव्र विपाक (अनुभाव=फलभोग) का भागी होता है। (३) तीसरा निमित्त है-भवं पप्प-भव (जन्म) विशेष को प्राप्त करके। जैसे-मनुष्य भव या तिर्यञ्चभव को पाकर जीव निद्रादिरूप दर्शनावरणीय कर्म का विशेष विपाक (फलभोग) पाता है। (४) पोग्गलं पप्प-किसी के द्वारा शस्त्र, ढेला, पत्थर या तलवार आदि के योग से, अथवा पत्थर, काष्ठ आदि के स्वतः गिरने से या उनके आघात-चोट आदि से असातावेदनीय आदि किसी कर्म का विपाक (अनुभाव=फलानुभव) हो जाता है। (५) पोग्गल परिणाम पप्प-अर्थात-पुद्गलों के परिणमन-विशेष को पाकर भी कर्म का विपाक तीव्र हो जाता है। जैसे-मदिरापान के परिणामस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आता है, तब
१. देखें-'जैनतत्त्वकलिका' (आचार्य श्री आत्मारामजी म.), कलिका ६, पृ. १७८ Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org