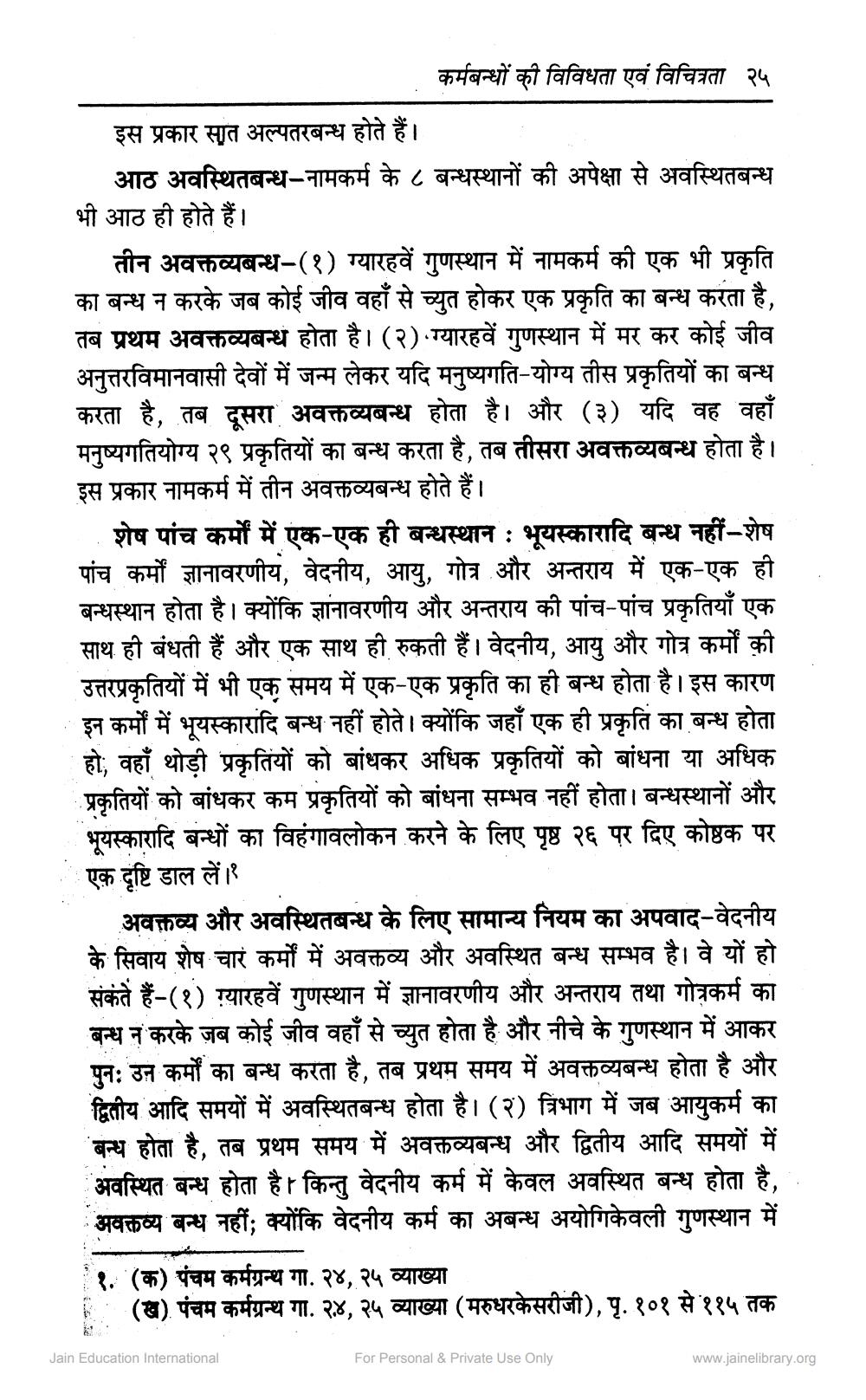________________
कर्मबन्धों की विविधता एवं विचित्रता २५
इस प्रकार सात अल्पतरबन्ध होते हैं।
आठ अवस्थितबन्ध - नामकर्म के ८ बन्धस्थानों की अपेक्षा से अवस्थितबन्ध भी आठ ही होते हैं ।
तीन अवक्तव्यबन्ध - (१) ग्यारहवें गुणस्थान में नामकर्म की एक भी प्रकृति का बन्ध न करके जब कोई जीव वहाँ से च्युत होकर एक प्रकृति का बन्ध करता है, तब प्रथम अवक्तव्यबन्ध होता है । (२) ग्यारहवें गुणस्थान में मर कर कोई जीव अनुत्तरविमानवासी देवों में जन्म लेकर यदि मनुष्यगति-योग्य तीस प्रकृतियों का बन्ध करता है, तब दूसरा अवक्तव्यबन्ध होता है। और (३) यदि वह वहाँ मनुष्यगतियोग्य २९ प्रकृतियों का बन्ध करता है, तब तीसरा अवक्तव्यबन्ध होता है । इस प्रकार नामकर्म में तीन अवक्तव्यबन्ध होते हैं ।
शेष पांच कर्मों में एक-एक ही बन्धस्थान : भूयस्कारादि बन्ध नहीं - शेष पांच कर्मों ज्ञानावरणीयं, वेदनीय, आयु, गोत्र और अन्तराय में एक-एक ही बन्धस्थान होता है। क्योंकि ज्ञानावरणीय और अन्तराय की पांच-पांच प्रकृतियाँ एक साथ ही बंधती हैं और एक साथ ही रुकती हैं। वेदनीय, आयु और गोत्र कर्मों की उत्तरप्रकृतियों में भी एक समय में एक-एक प्रकृति का ही बन्ध होता है । इस कारण इन कर्मों में भूयस्कारादि बन्ध नहीं होते। क्योंकि जहाँ एक ही प्रकृति का बन्ध होता हो, वहाँ थोड़ी प्रकृतियों को बांधकर अधिक प्रकृतियों को बांधना या अधिक प्रकृतियों को बांधकर कम प्रकृतियों को बांधना सम्भव नहीं होता । बन्धस्थानों और भूस्कारादि बन्धों का विहंगावलोकन करने के लिए पृष्ठ २६ पर दिए कोष्ठक पर एक दृष्टि डाल लें।
अवक्तव्य और अवस्थितबन्ध के लिए सामान्य नियम का अपवाद - वेदनीय के सिवाय शेष चार कर्मों में अवक्तव्य और अवस्थित बन्ध सम्भव है। वे यों हो संकते हैं-(१) ग्यारहवें गुणस्थान में ज्ञानावरणीय और अन्तराय तथा गोत्रकर्म का बन्ध न करके जब कोई जीव वहाँ से च्युत होता है और नीचे के में आकर गुणस्थान पुनः उन कर्मों का बन्ध करता है, तब प्रथम समय में अवक्तव्यबन्ध होता है और द्वितीय आदि समयों में अवस्थितबन्ध होता है । (२) त्रिभाग में जब आयुकर्म का बन्ध होता है, तब प्रथम समय में अवक्तव्यबन्ध और द्वितीय आदि समयों में अवस्थित बन्ध होता है । किन्तु वेदनीय कर्म में केवल अवस्थित बन्ध होता है, अवक्तव्य बन्ध नहीं; क्योंकि वेदनीय कर्म का अबन्ध अयोगिकेवली गुणस्थान में
१. (क) पंचम कर्मग्रन्थ गा. २४, २५ व्याख्या
. पंचम कर्मग्रन्थ गा. २.४, २५ व्याख्या ( मरुधरकेसरीजी), पृ. १०१ से ११५ तक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org