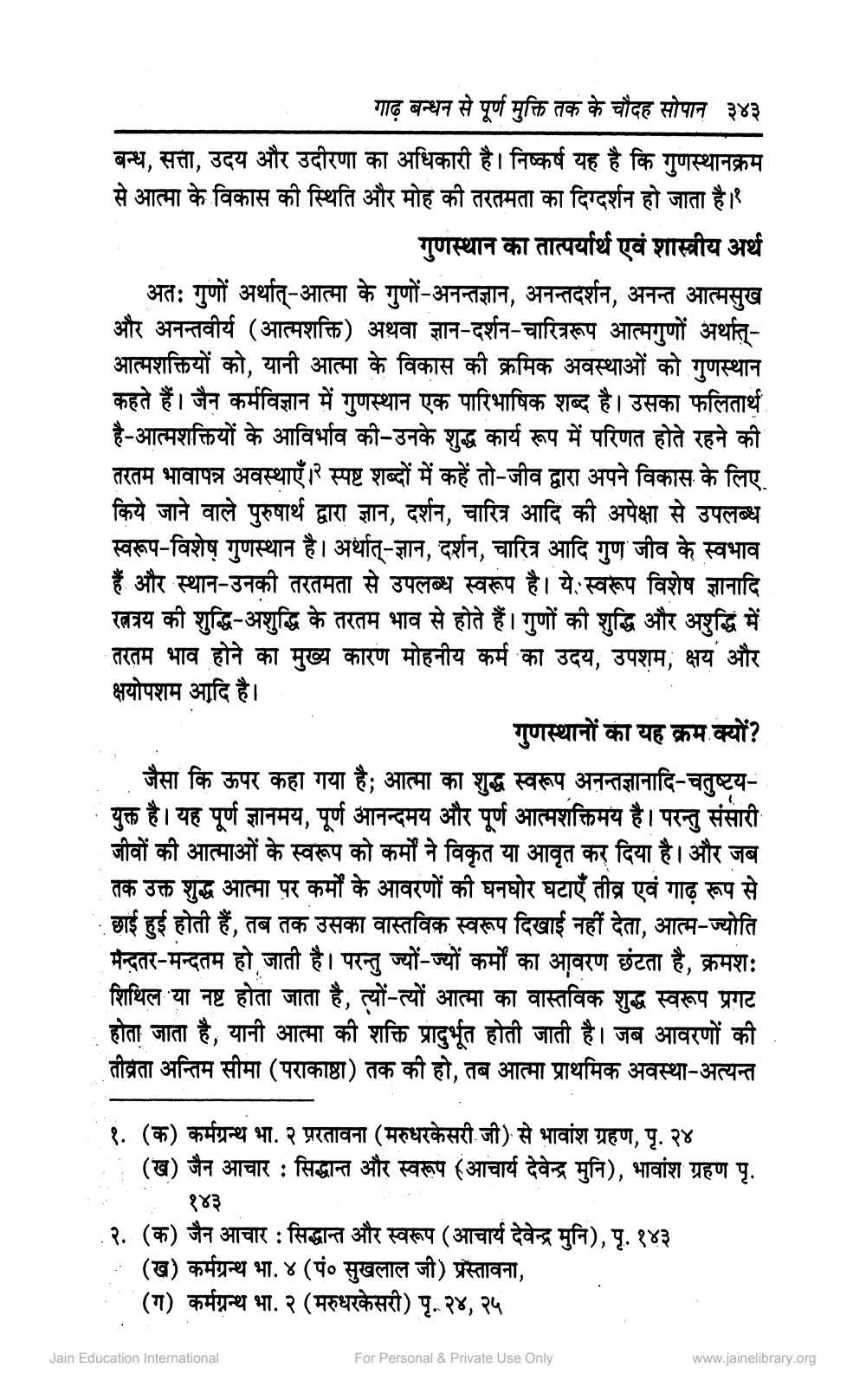________________
गाढ़ बन्धन से पूर्ण मुक्ति तक के चौदह सोपान ३४३ बन्ध, सत्ता, उदय और उदीरणा का अधिकारी है। निष्कर्ष यह है कि गुणस्थानक्रम से आत्मा के विकास की स्थिति और मोह की तरतमता का दिग्दर्शन हो जाता है । १
गुणस्थान का तात्पर्यार्थ एवं शास्त्रीय अर्थ
अतः गुणों अर्थात्-आत्मा के गुणों- अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त आत्मसुख और अनन्तवीर्य (आत्मशक्ति) अथवा ज्ञान दर्शन - चारित्ररूप आत्मगुणों अर्थात्आत्मशक्तियों को, यानी आत्मा के विकास की क्रमिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं । जैन कर्मविज्ञान में गुणस्थान एक पारिभाषिक शब्द है । उसका फलितार्थ है - आत्मशक्तियों के आविर्भाव की उनके शुद्ध कार्य रूप में परिणत होते रहने की तरतम भावापन्न अवस्थाएँ। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जीव द्वारा अपने विकास के लिएकिये जाने वाले पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की अपेक्षा से उपलब्ध स्वरूप- - विशेष गुणस्थान है। अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुण जीव के स्वभाव हैं और स्थान उनकी तरतमता से उपलब्ध स्वरूप है। ये स्वरूप विशेष ज्ञानादि रत्नत्रय की शुद्धि - अशुद्धि के तरतम भाव से होते हैं। गुणों की शुद्धि और अशुद्धि में तरतम भाव होने का मुख्य कारण मोहनीय कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम आदि है।
गुणस्थानों का यह क्रम क्यों?
जैसा कि ऊपर कहा गया है; आत्मा का शुद्ध स्वरूप अनन्तज्ञानादि- चतुष्टययुक्त है। यह पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण आनन्दमय और पूर्ण आत्मशक्तिमय है । परन्तु संसारी जीवों की आत्माओं के स्वरूप को कर्मों ने विकृत या आवृत कर दिया है। और जब तक उक्त शुद्ध आत्मा पर कर्मों के आवरणों की घनघोर घटाएँ तीव्र एवं गाढ़ रूप से . छाई हुई होती हैं, तब तक उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता, आत्म-ज्योति मैन्दतर- मन्दतम हो जाती है । परन्तु ज्यों-ज्यों कर्मों का आवरण छंटता है, क्रमशः शिथिल या नष्ट होता जाता है, त्यों-त्यों आत्मा का वास्तविक शुद्ध स्वरूप प्रगट होता जाता है, यानी आत्मा की शक्ति प्रादुर्भूत होती जाती है। जब आवरणों की तीव्रता अन्तिम सीमा (पराकाष्ठा) तक की हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्था - अत्यन्त
१. (क) कर्मग्रन्थ भा. २ प्रस्तावना (मरुधरकेसरी जी) से भावांश ग्रहण, पृ. २४ (ख) जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप ( आचार्य देवेन्द्र मुनि), भावांश ग्रहण पृ.
१४३
.२. (क) जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप ( आचार्य देवेन्द्र मुनि), पृ. १४३
(ख) कर्मग्रन्थ भा. ४ ( पं० सुखलाल जी) प्रस्तावना, (ग) कर्मग्रन्थ भा. २ ( मरुधरकेसरी) पृ. २४, २५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org