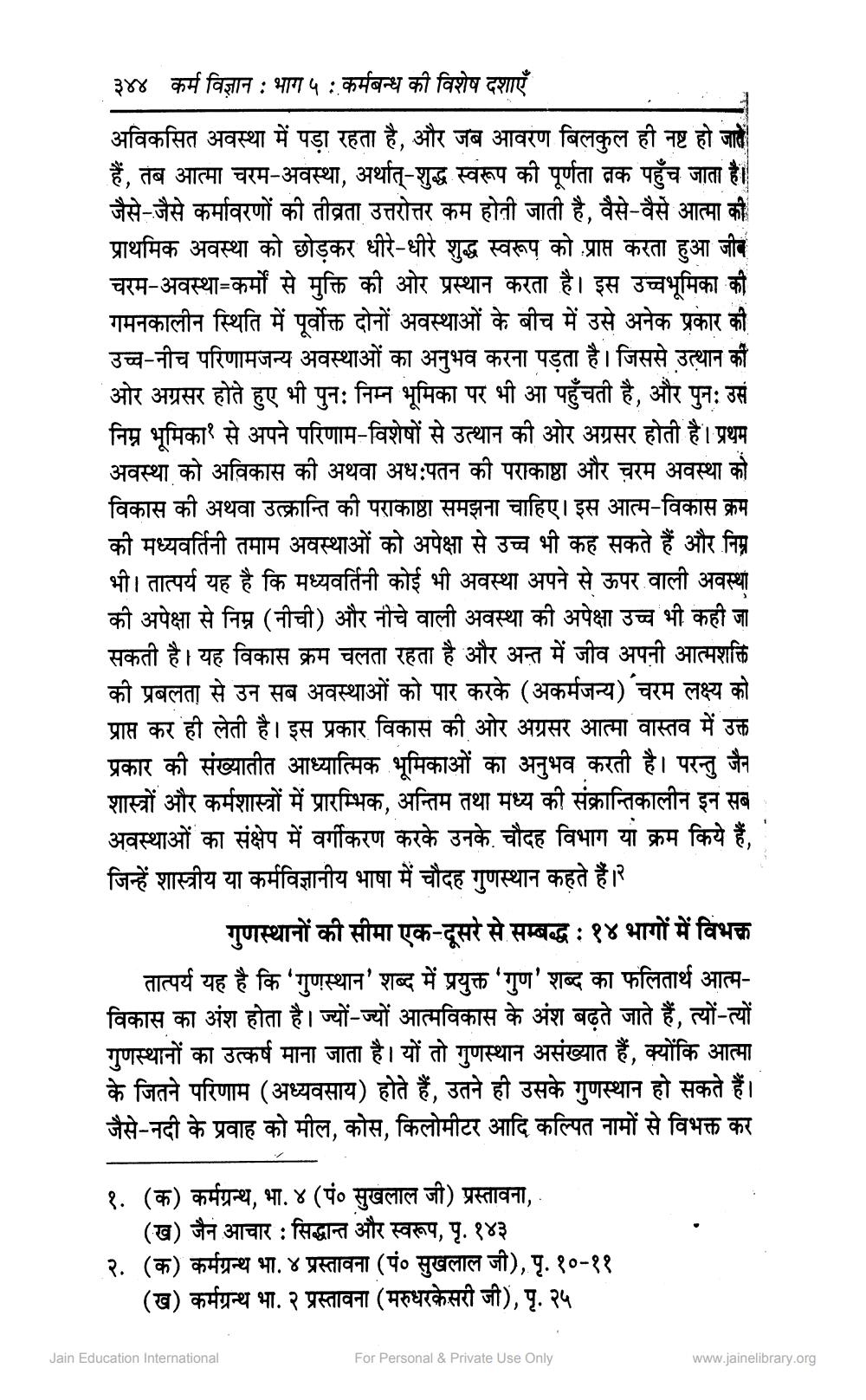________________
३४४ कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ अविकसित अवस्था में पड़ा रहता है, और जब आवरण बिलकुल ही नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा चरम-अवस्था, अर्थात्-शुद्ध स्वरूप की पूर्णता तक पहुँच जाता है। जैसे-जैसे कर्मावरणों की तीव्रता उत्तरोत्तर कम होती जाती है, वैसे-वैसे आत्मा की प्राथमिक अवस्था को छोड़कर धीरे-धीरे शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता हुआ जीब चरम-अवस्था कर्मों से मुक्ति की ओर प्रस्थान करता है। इस उच्चभूमिका की गमनकालीन स्थिति में पूर्वोक्त दोनों अवस्थाओं के बीच में उसे अनेक प्रकार की उच्च-नीच परिणामजन्य अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ता है। जिससे उत्थान की
ओर अग्रसर होते हुए भी पुनः निम्न भूमिका पर भी आ पहुँचती है, और पुनः उसं निम्न भूमिकासे अपने परिणाम-विशेषों से उत्थान की ओर अग्रसर होती है। प्रथम अवस्था को अविकास की अथवा अध:पतन की पराकाष्ठा और चरम अवस्था को विकास की अथवा उत्क्रान्ति की पराकाष्ठा समझना चाहिए। इस आत्म-विकास क्रम की मध्यवर्तिनी तमाम अवस्थाओं को अपेक्षा से उच्च भी कह सकते हैं और निम्र भी। तात्पर्य यह है कि मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपने से ऊपर वाली अवस्था की अपेक्षा से निम्न (नीची) और नीचे वाली अवस्था की अपेक्षा उच्च भी कही जा सकती है। यह विकास क्रम चलता रहता है और अन्त में जीव अपनी आत्मशक्ति की प्रबलता से उन सब अवस्थाओं को पार करके (अकर्मजन्य) चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेती है। इस प्रकार विकास की ओर अग्रसर आत्मा वास्तव में उक्त प्रकार की संख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओं का अनुभव करती है। परन्तु जैन शास्त्रों और कर्मशास्त्रों में प्रारम्भिक, अन्तिम तथा मध्य की संक्रान्तिकालीन इन सब अवस्थाओं का संक्षेप में वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग या क्रम किये हैं, जिन्हें शास्त्रीय या कर्मविज्ञानीय भाषा में चौदह गुणस्थान कहते हैं।२
गुणस्थानों की सीमा एक-दूसरे से सम्बद्ध : १४ भागों में विभक्त तात्पर्य यह है कि 'गुणस्थान' शब्द में प्रयुक्त 'गुण' शब्द का फलितार्थ आत्मविकास का अंश होता है। ज्यों-ज्यों आत्मविकास के अंश बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों गुणस्थानों का उत्कर्ष माना जाता है। यों तो गुणस्थान असंख्यात हैं, क्योंकि आत्मा के जितने परिणाम (अध्यवसाय) होते हैं, उतने ही उसके गुणस्थान हो सकते हैं। जैसे-नदी के प्रवाह को मील, कोस, किलोमीटर आदि कल्पित नामों से विभक्त कर
१. (क) कर्मग्रन्थ, भा. ४ (पं० सुखलाल जी) प्रस्तावना, .
(ख) जैन आचार : सिद्धान्त और स्वरूप, पृ. १४३ २. (क) कर्मग्रन्थ भा. ४ प्रस्तावना (पं० सुखलाल जी), पृ. १०-११
(ख) कर्मग्रन्थ भा. २ प्रस्तावना (मरुधरकेसरी जी), पृ. २५
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org