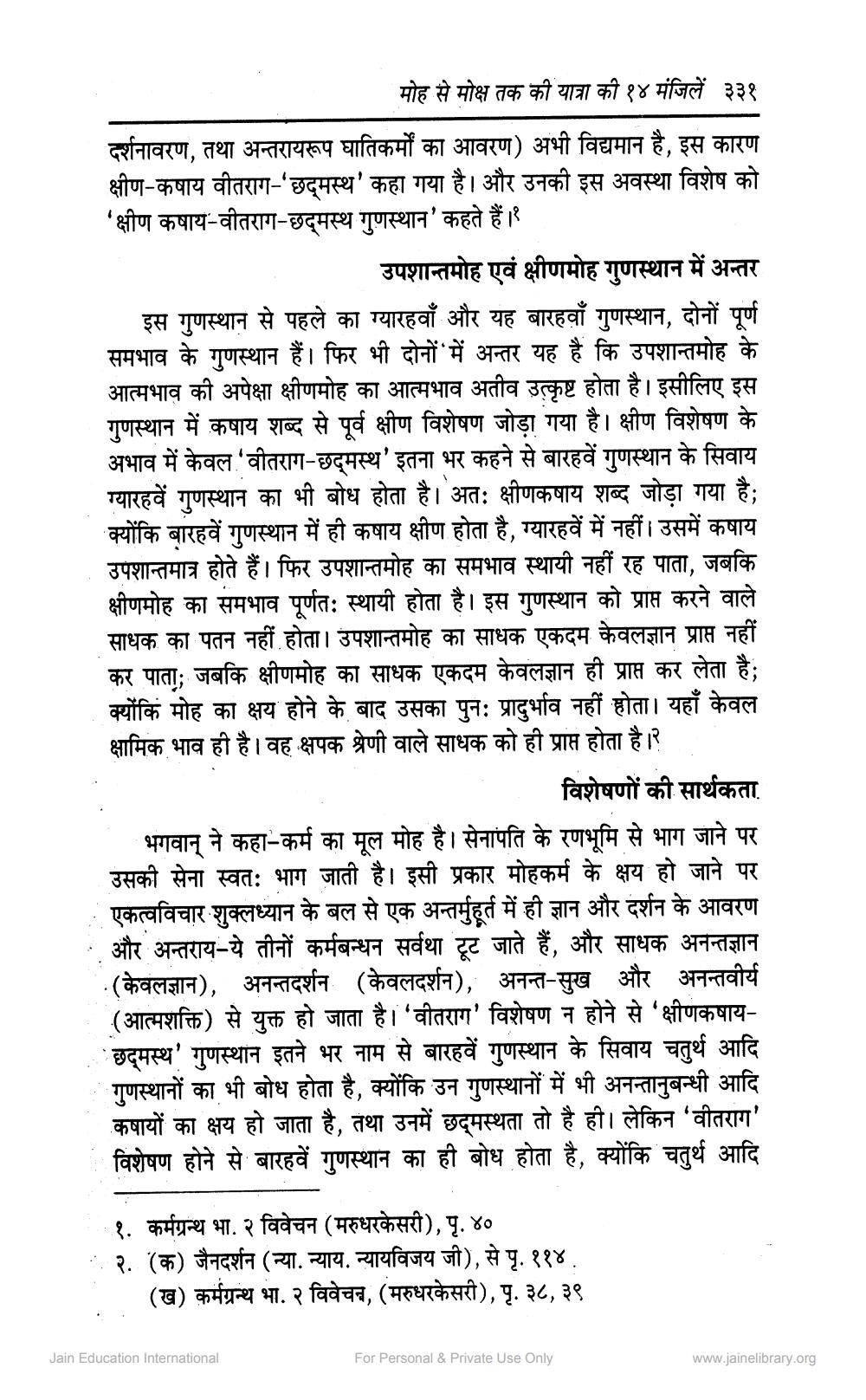________________
मोह से मोक्ष तक की यात्रा की १४ मंजिलें ३३१
दर्शनावरण, तथा अन्तरायरूप घातिकर्मों का आवरण) अभी विद्यमान है, इस कारण क्षीण- कषाय वीतराग-'छद्मस्थ' कहा गया है। और उनकी इस अवस्था विशेष को ' क्षीण कषाय- वीतराग - छद्मस्थ गुणस्थान' कहते हैं । १
उपशान्तमोह एवं क्षीणमोह गुणस्थान में अन्तर
इस गुणस्थान से पहले का ग्यारहवाँ और यह बारहवाँ गुणस्थान, दोनों पूर्ण समभाव के गुणस्थान हैं। फिर भी दोनों में अन्तर यह है कि उपशान्तमोह के आत्मभाव की अपेक्षा क्षीणमोह का आत्मभाव अतीव उत्कृष्ट होता है । इसीलिए इस गुणस्थान में कषाय शब्द से पूर्व क्षीण विशेषण जोड़ा गया है। क्षीण विशेषण के अभाव में केवल 'वीतराग - छद्मस्थ' इतना भर कहने से बारहवें गुणस्थान के सिवाय ग्यारहवें गुणस्थान का भी बोध होता है। अतः क्षीणकषाय शब्द जोड़ा गया है; क्योंकि बारहवें गुणस्थान में ही कषाय क्षीण होता है, ग्यारहवें में नहीं। उसमें कषाय उपशान्तमात्र होते हैं । फिर उपशान्तमोह का समभाव स्थायी नहीं रह पाता, जबकि क्षीणमोह का समभाव पूर्णतः स्थायी होता है। इस गुणस्थान को प्राप्त करने वाले साधक का पतन नहीं होता । उपशान्तमोह का साधक एकदम केवलज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता; जबकि क्षीणमोह का साधक एकदम केवलज्ञान ही प्राप्त कर लेता है; क्योंकि मोह का क्षय होने के बाद उसका पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता। यहाँ केवल क्षामिक भाव ही है । वह क्षपक श्रेणी वाले साधक को ही प्राप्त होता है । २
विशेषणों की सार्थकता.
भगवान् ने कहा- कर्म का मूल मोह है । सेनापति के रणभूमि से भाग जाने पर उसकी सेना स्वतः भाग जाती है। इसी प्रकार मोहकर्म के क्षय हो जाने पर एकत्वविचार शुक्लध्यान के बल से एक अन्तर्मुहूर्त में ही ज्ञान और दर्शन के आवरण और अन्तराय- ये तीनों कर्मबन्धन सर्वथा टूट जाते हैं, और साधक अनन्तज्ञान . (केवलज्ञान), अनन्तदर्शन (केवलदर्शन), अनन्त सुख और अनन्तवीर्य (आत्मशक्ति) से युक्त हो जाता है। 'वीतराग' विशेषण न होने से ' क्षीणकषायछद्मस्थ' गुणस्थान इतने भर नाम से बारहवें गुणस्थान के सिवाय चतुर्थ आदि गुणस्थानों का भी बोध होता है, क्योंकि उन गुणस्थानों में भी अनन्तानुबन्धी आदि कषायों का क्षय हो जाता है, तथा उनमें छद्मस्थता तो है ही। लेकिन 'वीतराग' विशेषण होने से बारहवें गुणस्थान का ही बोध होता है, क्योंकि चतुर्थ आदि
१. कर्मग्रन्थ भा. २ विवेचन ( मरुधरकेसरी), पृ. ४०
२. (क) जैनदर्शन (न्या. न्याय. न्यायविजय जी), से पृ. ११४. (ख) कर्मग्रन्थ भा. २ विवेचन, ( मरुधरकेसरी), पृ. ३८, ३९
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org