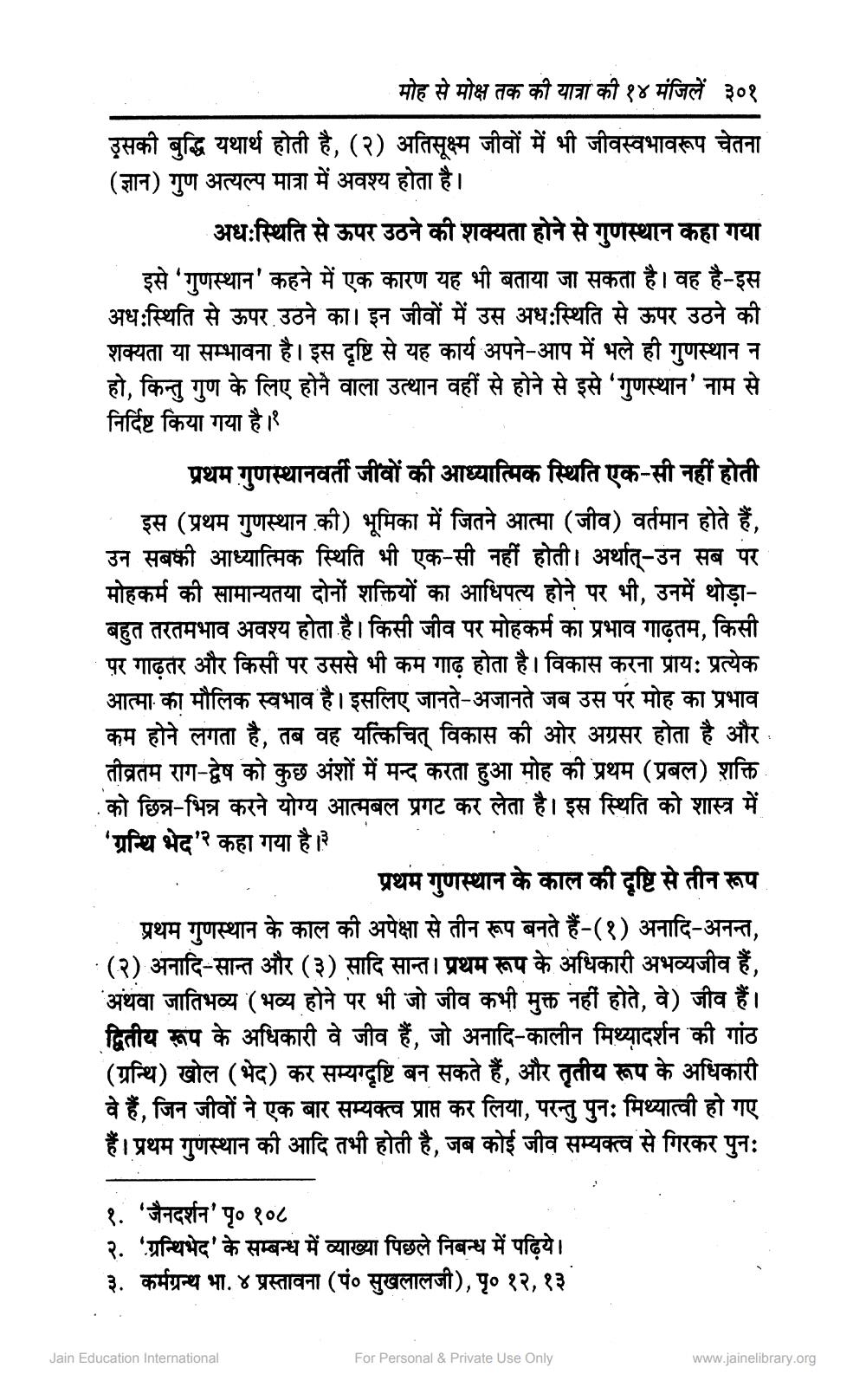________________
मोह से मोक्ष तक की यात्रा की १४ मंजिलें ३०१
उसकी बुद्धि यथार्थ होती है, (२) अतिसूक्ष्म जीवों में भी जीवस्वभावरूप चेतना (ज्ञान) गुण अत्यल्प मात्रा में अवश्य होता है।
अधःस्थिति से ऊपर उठने की शक्यता होने से गुणस्थान कहा गया
इसे 'गुणस्थान' कहने में एक कारण यह भी बताया जा सकता है। वह है-इस अधः स्थिति से ऊपर उठने का। इन जीवों में उस अधःस्थिति से ऊपर उठने की शक्यता या सम्भावना है। इस दृष्टि से यह कार्य अपने-आप में भले ही गुणस्थान न हो, किन्तु गुण के लिए होने वाला उत्थान वहीं से होने से इसे 'गुणस्थान' नाम से निर्दिष्ट किया गया है।
प्रथम गुणस्थानवर्ती जीवों की आध्यात्मिक स्थिति एक सी नहीं होती
इस (प्रथम गुणस्थान की) भूमिका में जितने आत्मा (जीव) वर्तमान होते हैं, उन सबकी आध्यात्मिक स्थिति भी एक सी नहीं होती । अर्थात् - उन सब पर मोहकर्म की सामान्यतया दोनों शक्तियों का आधिपत्य होने पर भी, उनमें थोड़ाबहुत तरतमभाव अवश्य होता है। किसी जीव पर मोहकर्म का प्रभाव गाढ़तम, किसी पर गाढ़तर और किसी पर उससे भी कम गाढ़ होता है। विकास करना प्रायः प्रत्येक आत्मा का मौलिक स्वभाव है। इसलिए जानते - अजानते जब उस पर मोह का प्रभाव कम होने लगता है, तब वह यत्किचित् विकास की ओर अग्रसर होता है और तीव्रतम राग-द्वेष को कुछ अंशों में मन्द करता हुआ मोह की प्रथम (प्रबल) शक्ति . को छिन्न-भिन्न करने योग्य आत्मबल प्रगट कर लेता है। इस स्थिति को शास्त्र में 'ग्रन्थि भेद' २ कहा गया है । ३
प्रथम गुणस्थान के काल की दृष्टि से तीन रूप
प्रथम गुणस्थान के काल की अपेक्षा से तीन रूप बनते हैं - ( १ ) अनादि - अनन्त, (२) अनादि- सान्त और (३) सादि सान्त । प्रथम रूप के अधिकारी अभव्यजीव हैं, अथवा जातिभव्य (भव्य होने पर भी जो जीव कभी मुक्त नहीं होते, वे) जीव हैं । द्वितीय रूप के अधिकारी वे जीव हैं, जो अनादि कालीन मिथ्यादर्शन की गांठ (ग्रन्थि) खोल (भेद) कर सम्यग्दृष्टि बन सकते हैं, और तृतीय रूप के अधिकारी वे हैं, जिन जीवों ने एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया, परन्तु पुनः मिथ्यात्वी हो गए हैं। प्रथम गुणस्थान की आदि तभी होती है, जब कोई जीव सम्यक्त्व से गिरकर पुनः
१. 'जैनदर्शन' पृ० १०८
२. ' ग्रन्थिभेद' के सम्बन्ध में व्याख्या पिछले निबन्ध में पढ़िये ।
३.
कर्मग्रन्थ भा. ४ प्रस्तावना (पं० सुखलालजी), पृ० १२, १३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org