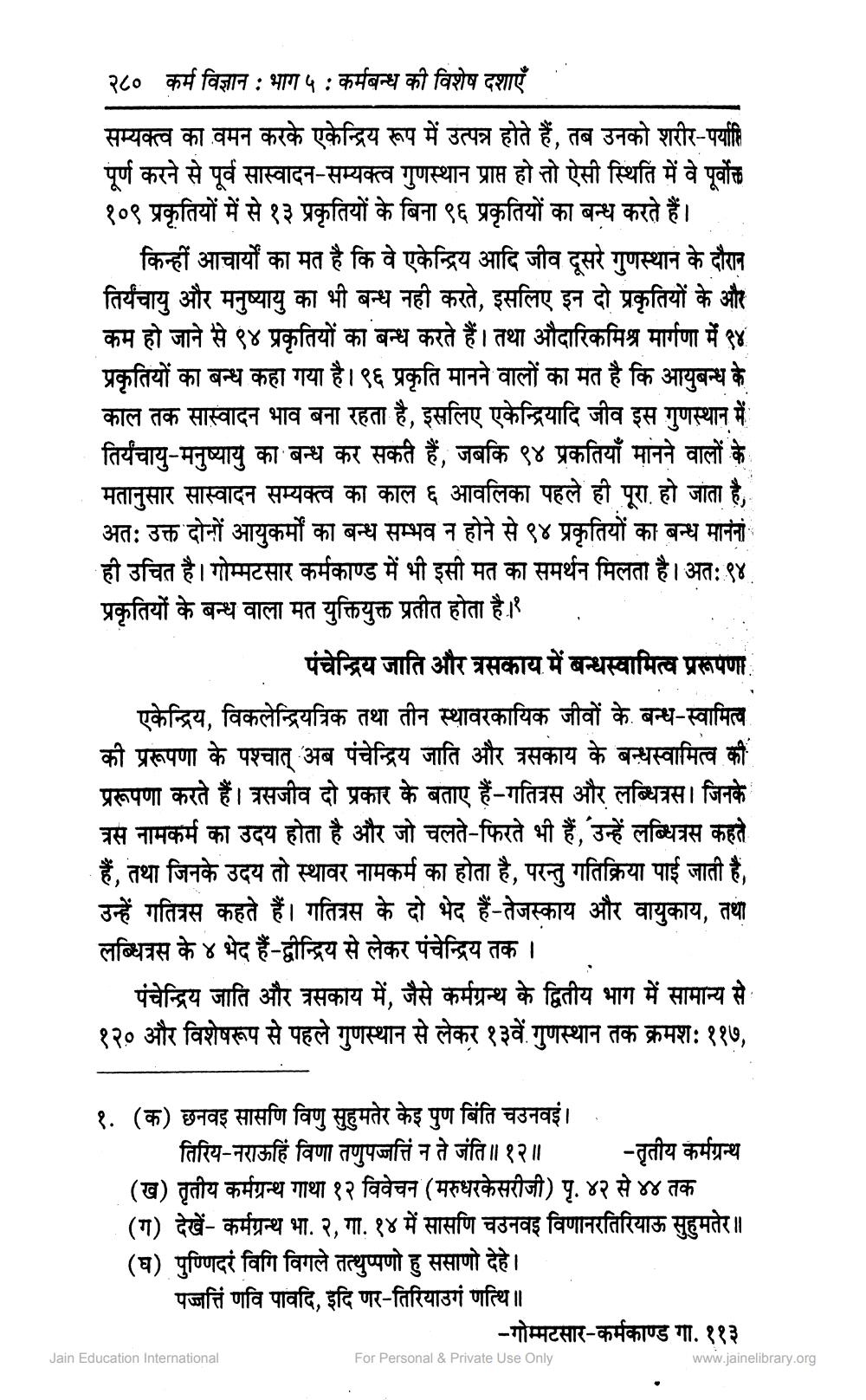________________
२८० कर्म विज्ञान : भाग ५ : कर्मबन्ध की विशेष दशाएँ । सम्यक्त्व का वमन करके एकेन्द्रिय रूप में उत्पन्न होते हैं, तब उनको शरीर-पति पूर्ण करने से पूर्व सास्वादन-सम्यक्त्व गुणस्थान प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में वे पूर्वोक्त १०९ प्रकृतियों में से १३ प्रकृतियों के बिना ९६ प्रकृतियों का बन्ध करते हैं।
किन्हीं आचार्यों का मत है कि वे एकेन्द्रिय आदि जीव दूसरे गुणस्थान के दौरान तिर्यंचायु और मनुष्यायु का भी बन्ध नही करते, इसलिए इन दो प्रकृतियों के और कम हो जाने से ९४ प्रकृतियों का बन्ध करते हैं। तथा औदारिकमिश्र मार्गणा में ९४ प्रकृतियों का बन्ध कहा गया है। ९६ प्रकृति मानने वालों का मत है कि आयुबन्ध के काल तक सास्वादन भाव बना रहता है, इसलिए एकेन्द्रियादि जीव इस गुणस्थान में तिर्यंचायु-मनुष्यायु का बन्ध कर सकते हैं, जबकि ९४ प्रकतियाँ मानने वालों के मतानुसार सास्वादन सम्यक्त्व का काल ६ आवलिका पहले ही पूरा हो जाता है, अतः उक्त दोनों आयुकर्मों का बन्ध सम्भव न होने से ९४ प्रकृतियों का बन्ध मानना ही उचित है। गोम्मटसार कर्मकाण्ड में भी इसी मत का समर्थन मिलता है। अतः ९४ प्रकृतियों के बन्ध वाला मत युक्तियुक्त प्रतीत होता है। .
पंचेन्द्रिय जाति और त्रसकाय में बन्धस्वामित्व प्ररूपणा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रियत्रिक तथा तीन स्थावरकायिक जीवों के बन्ध-स्वामित्व की प्ररूपणा के पश्चात् अब पंचेन्द्रिय जाति और त्रसकाय के बन्धस्वामित्व की प्ररूपणा करते हैं। त्रसजीव दो प्रकार के बताए हैं-गतित्रस और लब्धित्रस। जिनके त्रस नामकर्म का उदय होता है और जो चलते-फिरते भी हैं, उन्हें लब्धित्रस कहते हैं, तथा जिनके उदय तो स्थावर नामकर्म का होता है, परन्तु गतिक्रिया पाई जाती हैं, उन्हें गतित्रस कहते हैं। गतित्रस के दो भेद हैं-तेजस्काय और वायुकाय, तथा लब्धिवस के ४ भेद हैं-द्वीन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक ।
पंचेन्द्रिय जाति और सकाय में, जैसे कर्मग्रन्थ के द्वितीय भाग में सामान्य से १२० और विशेषरूप से पहले गुणस्थान से लेकर १३वें. गुणस्थान तक क्रमशः ११७,
१. (क) छनवइ सासणि विणु सुहुमतेर केइ पुण बिंति चउनवइं।
तिरिय-नराऊहिं विणा तणुपज्जत्तिं न ते जंति ॥ १२॥ -तृतीय कर्मग्रन्थ (ख) तृतीय कर्मग्रन्थ गाथा १२ विवेचन (मरुधरकेसरीजी) पृ. ४२ से ४४ तक (ग) देखें- कर्मग्रन्थ भा. २, गा. १४ में सासणि चउनवइ विणानरतिरियाऊ सहमतेर॥ (घ) पुण्णिदरं विगि विगले तत्थुप्पणो हु ससाणो देहे। पजत्तिं णवि पावदि, इदि णर-तिरियाउगं णत्थि॥
-गोम्मटसार-कर्मकाण्ड गा. ११३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org