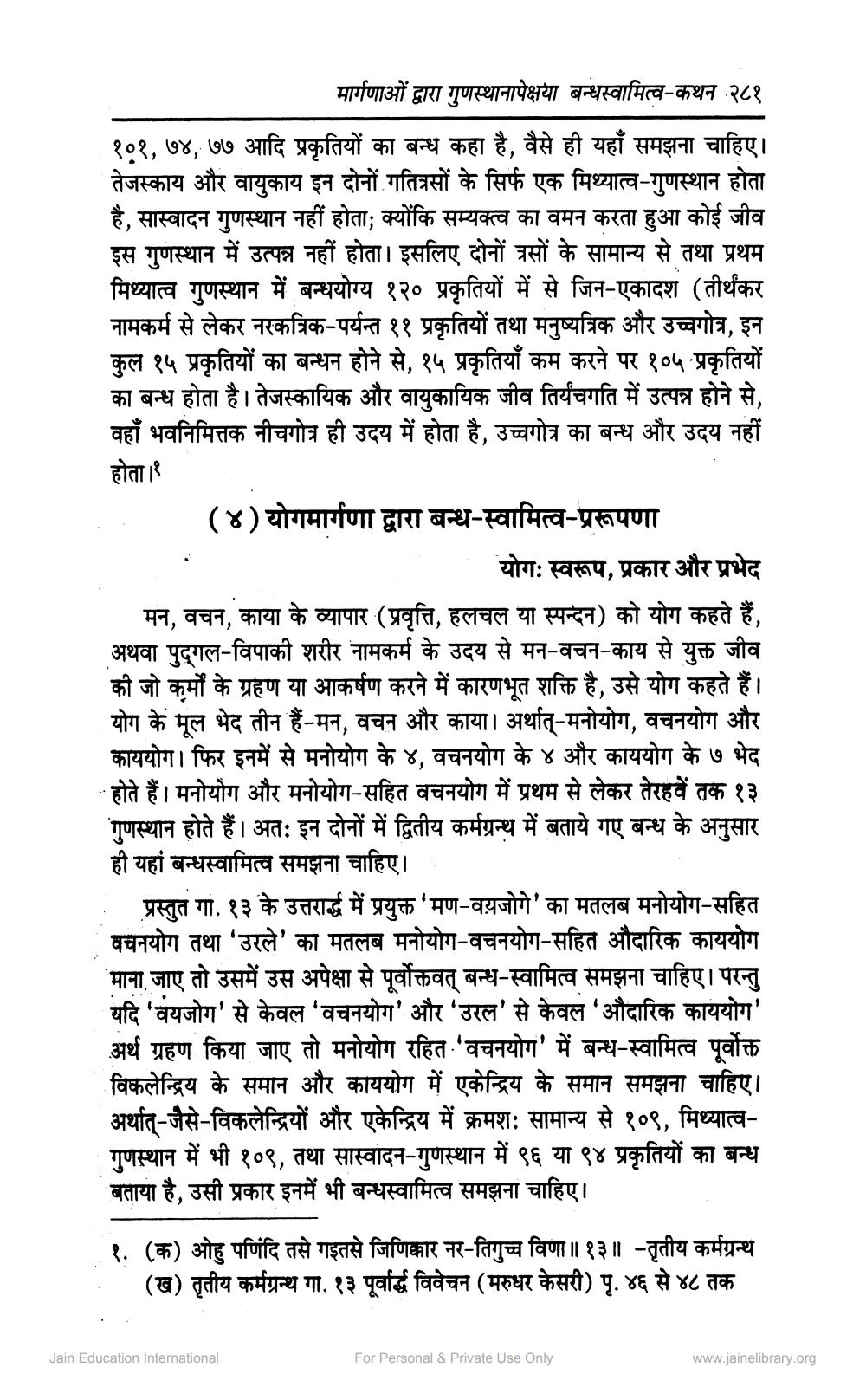________________
मार्गणाओं द्वारा गुणस्थानापेक्षया बन्धस्वामित्व-कथन २८१ १०१, ७४, ७७ आदि प्रकृतियों का बन्ध कहा है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए। तेजस्काय और वायुकाय इन दोनों गतित्रसों के सिर्फ एक मिथ्यात्व-गुणस्थान होता है, सास्वादन गुणस्थान नहीं होता; क्योंकि सम्यक्त्व का वमन करता हुआ कोई जीव इस गुणस्थान में उत्पन्न नहीं होता। इसलिए दोनों बसों के सामान्य से तथा प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में बन्धयोग्य १२० प्रकृतियों में से जिन-एकादश (तीर्थंकर नामकर्म से लेकर नरकत्रिक-पर्यन्त ११ प्रकृतियों तथा मनुष्यत्रिक और उच्चगोत्र, इन कुल १५ प्रकृतियों का बन्धन होने से, १५ प्रकृतियाँ कम करने पर १०५ प्रकृतियों का बन्ध होता है। तेजस्कायिक और वायुकायिक जीव तिर्यंचगति में उत्पन्न होने से, वहाँ भवनिमित्तक नीचगोत्र ही उदय में होता है, उच्चगोत्र का बन्ध और उदय नहीं होता। (४) योगमार्गणा द्वारा बन्ध-स्वामित्व-प्ररूपणा
योगः स्वरूप, प्रकार और प्रभेद मन, वचन, काया के व्यापार (प्रवृत्ति, हलचल या स्पन्दन) को योग कहते हैं, अथवा पुद्गल-विपाकी शरीर नामकर्म के उदय से मन-वचन-काय से युक्त जीव की जो कर्मों के ग्रहण या आकर्षण करने में कारणभूत शक्ति है, उसे योग कहते हैं। योग के मूल भेद तीन हैं-मन, वचन और काया। अर्थात्-मनोयोग, वचनयोग और काययोग। फिर इनमें से मनोयोग के ४, वचनयोग के ४ और काययोग के ७ भेद होते हैं। मनोयोग और मनोयोग-सहित वचनयोग में प्रथम से लेकर तेरहवें तक १३ गुणस्थान होते हैं। अतः इन दोनों में द्वितीय कर्मग्रन्थ में बताये गए बन्ध के अनुसार ही यहां बन्धस्वामित्व समझना चाहिए।
प्रस्तुत गा. १३ के उत्तरार्द्ध में प्रयुक्त 'मण-वयजोगे' का मतलब मनोयोग-सहित वचनयोग तथा 'उरले' का मतलब मनोयोग-वचनयोग-सहित औदारिक काययोग माना जाए तो उसमें उस अपेक्षा से पूर्वोक्तवत् बन्ध-स्वामित्व समझना चाहिए। परन्तु यदि 'वयजोग' से केवल 'वचनयोग' और 'उरल' से केवल 'औदारिक काययोग' अर्थ ग्रहण किया जाए तो मनोयोग रहित 'वचनयोग' में बन्ध-स्वामित्व पूर्वोक्त विकलेन्द्रिय के समान और काययोग में एकेन्द्रिय के समान समझना चाहिए। अर्थात्-जैसे-विकलेन्द्रियों और एकेन्द्रिय में क्रमशः सामान्य से १०९, मिथ्यात्वगुणस्थान में भी १०९, तथा सास्वादन-गुणस्थान में ९६ या ९४ प्रकृतियों का बन्ध बताया है, उसी प्रकार इनमें भी बन्धस्वामित्व समझना चाहिए।
. १. (क) ओहु पणिंदि तसे गइतसे जिणिक्कार नर-तिगुच्च विणा ॥ १३॥ -तृतीय कर्मग्रन्थ ___ (ख) तृतीय कर्मग्रन्थ गा. १३ पूर्वार्द्ध विवेचन (मरुधर केसरी) पृ. ४६ से ४८ तक
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org