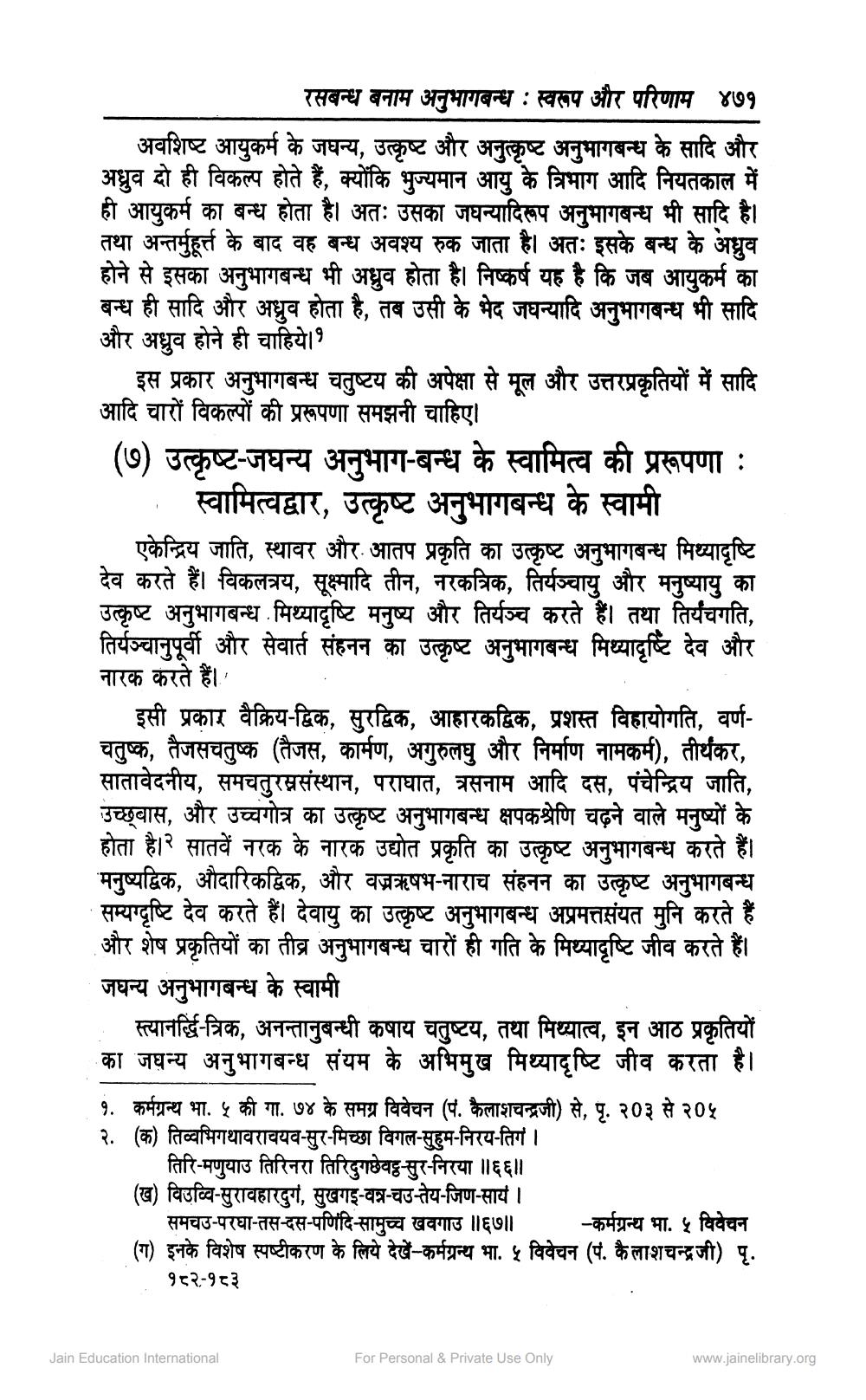________________
रसबन्ध बनाम अनुभागबन्ध : स्वरूप और परिणाम ४७१ अवशिष्ट आयुकर्म के जघन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध के सादि और अध्रुव दो ही विकल्प होते हैं, क्योंकि भुज्यमान आयु के त्रिभाग आदि नियतकाल में ही आयुकर्म का बन्ध होता है। अतः उसका जघन्यादिरूप अनुभागबन्ध भी सादि है। तथा अन्तर्मुहूर्त के बाद वह बन्ध अवश्य रुक जाता है। अतः इसके बन्ध के अध्रुव होने से इसका अनुभागबन्ध भी अध्रुव होता है। निष्कर्ष यह है कि जब आयुकर्म का बन्ध ही सादि और अध्रुव होता है, तब उसी के भेद जघन्यादि अनुभागबन्ध भी सादि और अध्रुव होने ही चाहिये।
इस प्रकार अनुभागबन्ध चतुष्टय की अपेक्षा से मूल और उत्तरप्रकृतियों में सादि आदि चारों विकल्पों की प्ररूपणा समझनी चाहिए। (७) उत्कृष्ट-जघन्य अनुभाग-बन्ध के स्वामित्व की प्ररूपणा :
स्वामित्वद्वार, उत्कृष्ट अनुभागबन्ध के स्वामी एकेन्द्रिय जाति, स्थावर और. आतप प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि देव करते हैं। विकलत्रय, सूक्ष्मादि तीन, नरकत्रिक, तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि मनुष्य और तिर्यञ्च करते हैं। तथा तिर्यंचगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी और सेवार्त संहनन का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्यादृष्टि देव और नारक करते हैं। __इसी प्रकार वैक्रिय-द्विक, सुरद्विक, आहारकद्विक, प्रशस्त विहायोगति, वर्णचतुष्क, तैजसचतुष्क (तैजस, कार्मण, अगुरुलघु और निर्माण नामकम), तीर्थंकर, सातावेदनीय, समचतुरनसंस्थान, पराघात, त्रसनाम आदि दस, पंचेन्द्रिय जाति, उच्छ्वास, और उच्चगोत्र का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपक श्रेणि चढ़ने वाले मनुष्यों के होता है। सातवें नरक के नारक उद्योत प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं। मनुष्यद्विक, औदारिकद्विक, और वज्रऋषभ-नाराच संहनन का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि देव करते हैं। देवायु का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत मुनि करते हैं
और शेष प्रकृतियों का तीव्र अनुभागबन्ध चारों ही गति के मिथ्यादृष्टि जीव करते हैं। जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी
स्त्यानर्द्धि-त्रिक, अनन्तानुबन्धी कषाय चतुष्टय, तथा मिथ्यात्व, इन आठ प्रकृतियों का जघन्य अनुभागबन्ध संयम के अभिमुख मिथ्यादृष्टि जीव करता है। १. कर्मग्रन्थ भा. ५ की गा. ७४ के समग्र विवेचन (प. कैलाशचन्द्रजी) से, पृ. २०३ से २०५ २. (क) तिव्वभिगथावरावयव-सुर-मिच्छा विगल-सुहुम-निरय-तिगं ।
तिरि-मणुयाउ तिरिनरा तिरिदुगछेवट्ठ-सुर-निरया ॥६६॥ (ख) विउव्वि-सुरावहारदुर्ग, सुखगइ-वन्न-चउ-तेय-जिण-सायं ।
समचउ-परघा-तस-दस-पणिदि-सामुच्च खवगाउ ॥६७॥ -कर्मग्रन्थ भा. ५ विवेचन (ग) इनके विशेष स्पष्टीकरण के लिये देखें-कर्मग्रन्थ भा. ५ विवेचन (पं. कैलाशचन्द्रजी) पृ.
१८२-१८३
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org