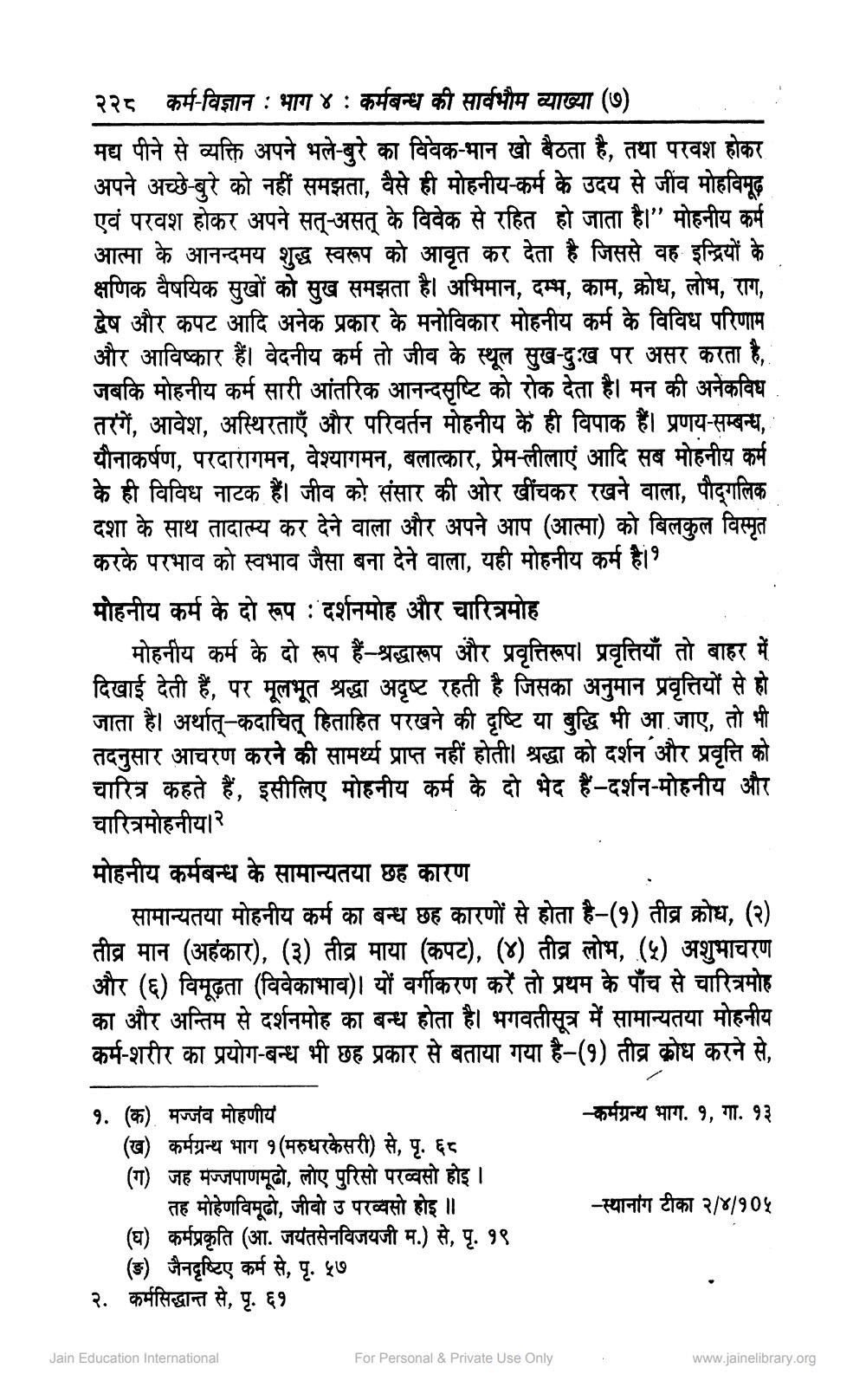________________
२२८ कर्म - विज्ञान : भाग ४ : कर्मबन्ध की सार्वभौम व्याख्या (७)
मद्य पीने से व्यक्ति अपने भले-बुरे का विवेक-भान खो बैठता है, तथा परवश होकर अपने अच्छे-बुरे को नहीं समझता, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से जींव मोहविमूढ़ एवं परवश होकर अपने सत्-असत् के विवेक से रहित हो जाता है।" मोहनीय कर्म आत्मा के आनन्दमय शुद्ध स्वरूप को आवृत कर देता है जिससे वह इन्द्रियों के क्षणिक वैषयिक सुखों को सुख समझता है। अभिमान, दम्भ, काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष और कपट आदि अनेक प्रकार के मनोविकार मोहनीय कर्म के विविध परिणाम और आविष्कार हैं। वेदनीय कर्म तो जीव के स्थूल सुख-दुःख पर असर करता है,. जबकि मोहनीय कर्म सारी आंतरिक आनन्दसृष्टि को रोक देता है। मन की अनेकविध तरंगें, आवेश, अस्थिरताएँ और परिवर्तन मोहनीय के ही विपाक हैं। प्रणय-सम्बन्ध, यौनाकर्षण, परदारगमन, वेश्यागमन, बलात्कार, प्रेम-लीलाएं आदि सब मोहनीय कर्म के ही विविध नाटक हैं। जीव को संसार की ओर खींचकर रखने वाला, पौद्गलिक दशा के साथ तादात्म्य कर देने वाला और अपने आप (आत्मा) को बिलकुल विस्मृत करके परभाव को स्वभाव जैसा बना देने वाला, यही मोहनीय कर्म है। १
मोहनीय कर्म के दो रूप दर्शनमोह और चारित्रमोह
मोहनीय कर्म के दो रूप हैं - श्रद्धारूप और प्रवृत्तिरूप । प्रवृत्तियाँ तो बाहर में दिखाई देती हैं, पर मूलभूत श्रद्धा अदृष्ट रहती है जिसका अनुमान प्रवृत्तियों से हो जाता है। अर्थात् कदाचित् हिताहित परखने की दृष्टि या बुद्धि भी आ जाए, तो भी तदनुसार आचरण करने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती। श्रद्धा को दर्शन और प्रवृत्ति को चारित्र कहते हैं, इसीलिए मोहनीय कर्म के दो भेद हैं- दर्शन - मोहनीय और चारित्रमोहनीय । २
मोहनीय कर्मबन्ध के सामान्यतया छह कारण
सामान्यतया मोहनीय कर्म का बन्ध छह कारणों से होता है - ( १ ) तीव्र क्रोध, (२) तीव्र मान (अहंकार), (३) तीव्र माया ( कपट), (४) तीव्र लोभ, (५) अशुभाचरण और (६) विमूढ़ता (विवेकाभाव ) । यों वर्गीकरण करें तो प्रथम के पाँच से चारित्रमोह का और अन्तिम से दर्शनमोह का बन्ध होता है। भगवतीसूत्र में सामान्यतया मोहनीय कर्म-शरीर का प्रयोग-बन्ध भी छह प्रकार से बताया गया है - ( 9 ) तीव्र क्रोध करने से,
- कर्मग्रन्थ भाग १, गा. १३
१. (क) मज्जेव मोहणीय
(ख) कर्मग्रन्थ भाग १ ( मरुधरकेसरी) से, पृ. ६८ (ग) जह मज्जपाणमूढो, लोए पुरिसो परव्वसो होइ । तह मोहेणविमूढो, जीवो उपरव्यसो होइ ॥ (घ) कर्मप्रकृति ( आ. जयंतसेनविजयजी म.) से, पृ. १९ (ङ) जैनदृष्टिए कर्म से, पृ. ५७
२. कर्मसिद्धान्त से, पृ. ६१
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
-स्थानांग टीका २/४/१०५
www.jainelibrary.org