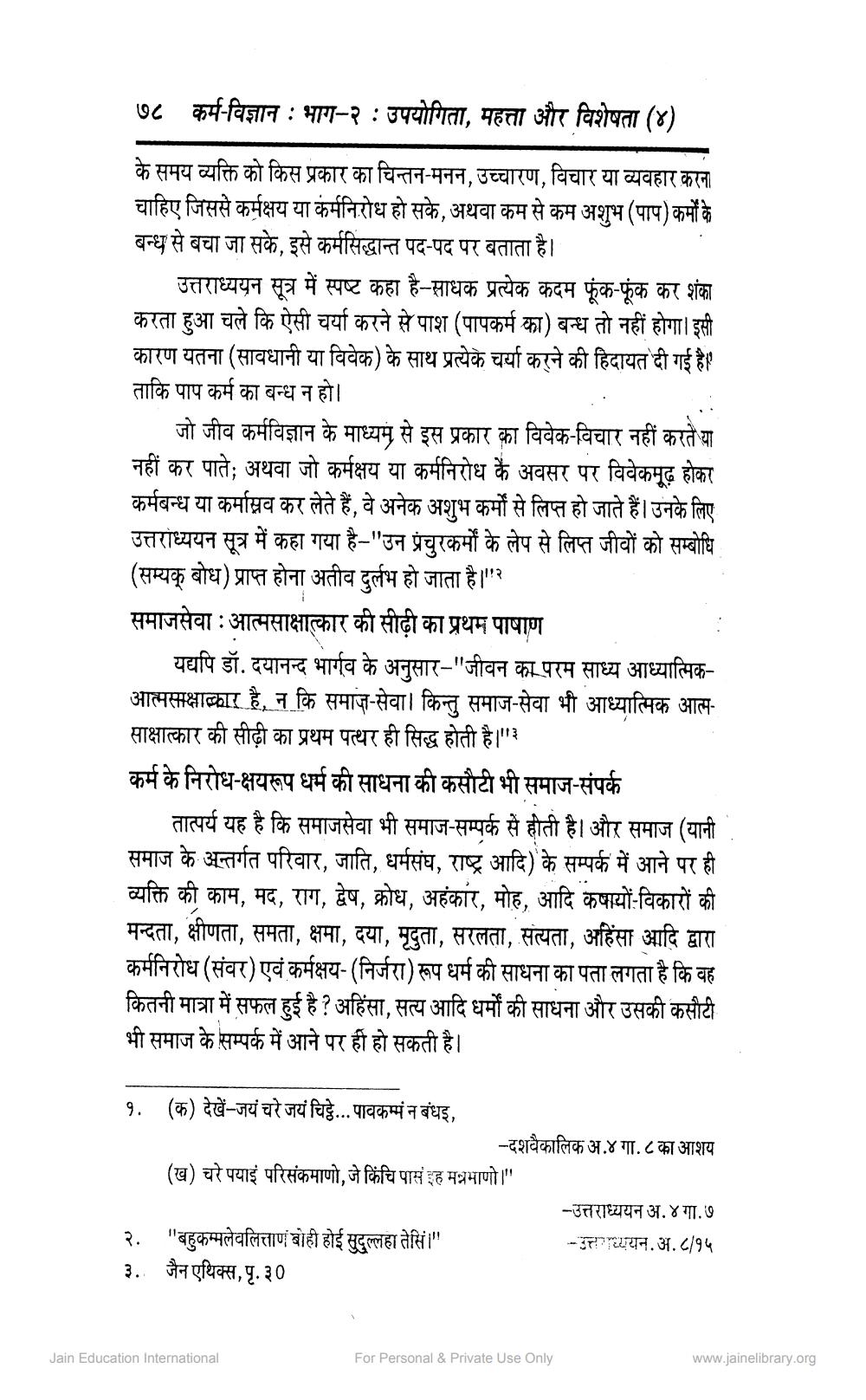________________
७८ कर्म-विज्ञान : भाग-२ : उपयोगिता, महत्ता और विशेषता (४) के समय व्यक्ति को किस प्रकार का चिन्तन-मनन, उच्चारण, विचार या व्यवहार करना चाहिए जिससे कर्मक्षय या कर्मनिरोध हो सके, अथवा कम से कम अशुभ (पाप) कर्मों के बन्ध से बचा जा सके, इसे कर्मसिद्धान्त पद-पद पर बताता है।
उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट कहा है-साधक प्रत्येक कदम फूंक-फूंक कर शंका करता हुआ चले कि ऐसी चर्या करने से पाश (पापकर्म का) बन्ध तो नहीं होगा। इसी कारण यतना (सावधानी या विवेक) के साथ प्रत्येक चर्या करने की हिदायत दी गई है।" ताकि पाप कर्म का बन्ध न हो।
जो जीव कर्मविज्ञान के माध्यम से इस प्रकार का विवेक-विचार नहीं करते या नहीं कर पाते; अथवा जो कर्मक्षय या कर्मनिरोध के अवसर पर विवेकमूढ़ होकर कर्मबन्ध या कर्मानव कर लेते हैं, वे अनेक अशुभ कर्मों से लिप्त हो जाते हैं। उनके लिए उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है-"उन पंचुरकर्मों के लेप से लिप्त जीवों को सम्बोधि (सम्यक् बोध) प्राप्त होना अतीव दुर्लभ हो जाता है।'२ समाजसेवा : आत्मसाक्षात्कार की सीढ़ी का प्रथम पाषाण
यद्यपि डॉ. दयानन्द भार्गव के अनुसार-"जीवन का परम साध्य आध्यात्मिकआत्मसाक्षात्कार है, न कि समाज-सेवा। किन्तु समाज-सेवा भी आध्यात्मिक आत्मसाक्षात्कार की सीढ़ी का प्रथम पत्थर ही सिद्ध होती है।"३ । कर्म के निरोध-क्षयरूप धर्म की साधना की कसौटी भी समाज-संपर्क
तात्पर्य यह है कि समाजसेवा भी समाज-सम्पर्क से होती है। और समाज (यानी समाज के अन्तर्गत परिवार, जाति, धर्मसंघ, राष्ट्र आदि) के सम्पर्क में आने पर ही व्यक्ति की काम, मद, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार, मोह, आदि कषायों-विकारों की मन्दता, क्षीणता, समता, क्षमा, दया, मृदुता, सरलता, सत्यता, अहिंसा आदि द्वारा कर्मनिरोध (संवर) एवं कर्मक्षय- (निर्जरा) रूप धर्म की साधना का पता लगता है कि वह कितनी मात्रा में सफल हुई है ? अहिंसा, सत्य आदि धर्मों की साधना और उसकी कसौटी भी समाज के सम्पर्क में आने पर ही हो सकती है।
१. (क) देखें-जयं चरे जयं चिढ़े... पावकम्मं न बंधइ,
-दशवकालिक अ.४ गा.८का आशय (ख) चरे पयाई परिसंकमाणो, जे किंचि पास इह मन्नभाणो।"
-उत्तराध्ययन अ.४ गा.७ २. "बहुकम्मलेवलित्ताणं बोही होई सुदुल्लहा तेसिं।"
- उत्ताध्ययन.अ.८/१५ ३.. जैन एथिक्स, पृ.३०
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org