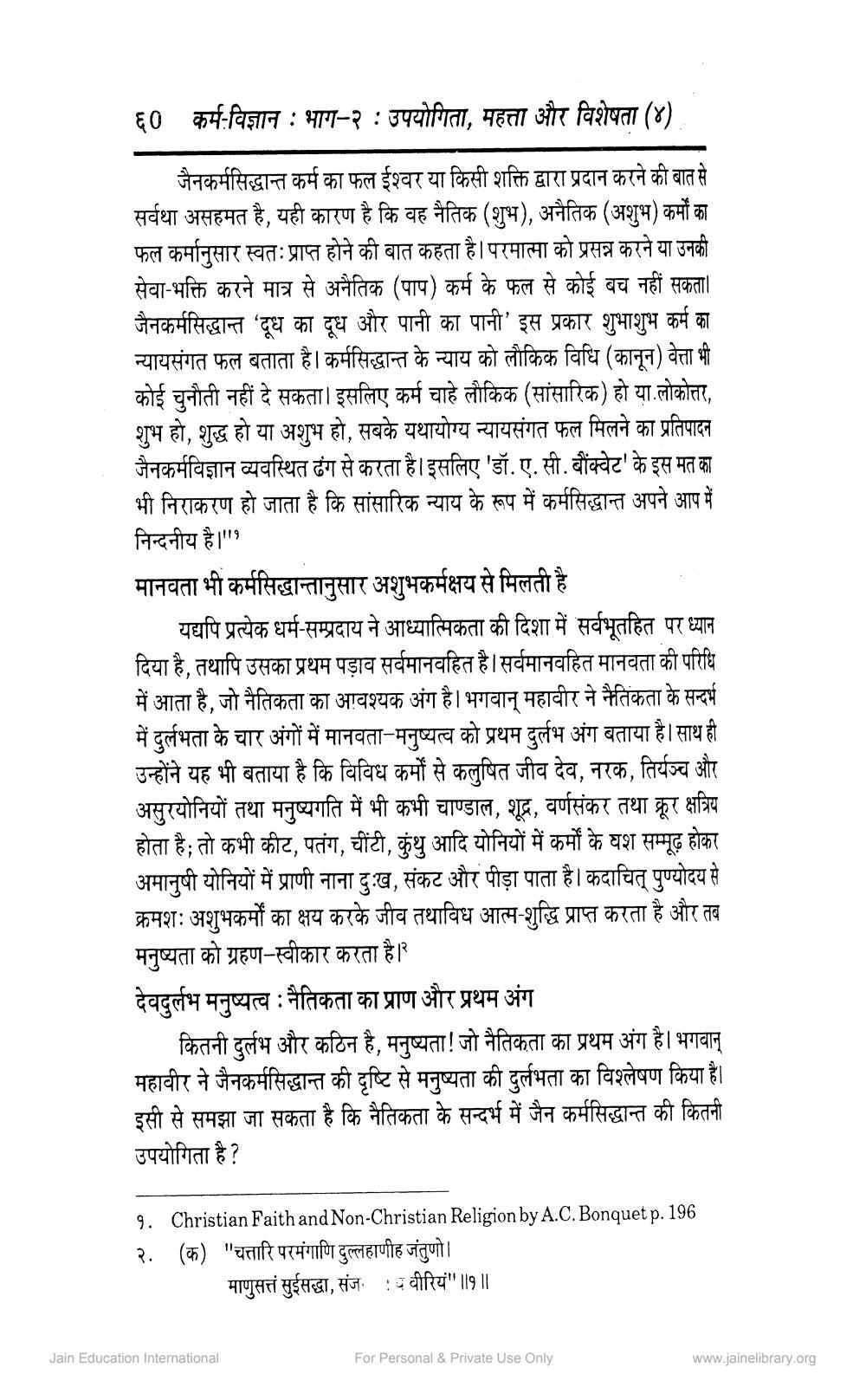________________
६० कर्म-विज्ञान : भाग-२ : उपयोगिता, महत्ता और विशेषता (४)
जैनकर्मसिद्धान्त कर्म का फल ईश्वर या किसी शक्ति द्वारा प्रदान करने की बात से सर्वथा असहमत है, यही कारण है कि वह नैतिक (शुभ), अनैतिक (अशुभ) कर्मों का फल कर्मानुसार स्वतः प्राप्त होने की बात कहता है। परमात्मा को प्रसन्न करने या उनकी सेवा-भक्ति करने मात्र से अनैतिक (पाप) कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। जैनकर्मसिद्धान्त 'दूध का दूध और पानी का पानी' इस प्रकार शुभाशुभ कर्म का न्यायसंगत फल बताता है। कर्मसिद्धान्त के न्याय को लौकिक विधि (कानून) वेत्ता भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए कर्म चाहे लौकिक (सांसारिक) हो या.लोकोत्तर, शुभ हो, शुद्ध हो या अशुभ हो, सबके यथायोग्य न्यायसंगत फल मिलने का प्रतिपादन जैनकर्मविज्ञान व्यवस्थित ढंग से करता है। इसलिए 'डॉ. ए. सी. बौंक्वेट' के इस मत का भी निराकरण हो जाता है कि सांसारिक न्याय के रूप में कर्मसिद्धान्त अपने आप में निन्दनीय है। मानवता भी कर्मसिद्धान्तानुसार अशुभकर्मक्षय से मिलती है
यद्यपि प्रत्येक धर्म-सम्प्रदाय ने आध्यात्मिकता की दिशा में सर्वभूतहित पर ध्यान दिया है, तथापि उसका प्रथम पड़ाव सर्वमानवहित है। सर्वमानवहित मानवता की परिधि में आता है, जो नैतिकता का आवश्यक अंग है। भगवान् महावीर ने नैतिकता के सन्दर्भ में दुर्लभता के चार अंगों में मानवता-मनुष्यत्व को प्रथम दुर्लभ अंग बताया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि विविध कर्मों से कलुषित जीव देव, नरक, तिर्यञ्च और असुरयोनियों तथा मनुष्यगति में भी कभी चाण्डाल, शूद्र, वर्णसंकर तथा क्रूर क्षत्रिय होता है; तो कभी कीट, पतंग, चींटी, कुंथु आदि योनियों में कर्मों के घश सम्मूढ़ होकर
अमानुषी योनियों में प्राणी नाना दुःख, संकट और पीड़ा पाता है। कदाचित् पुण्योदय से क्रमशः अशुभकर्मों का क्षय करके जीव तथाविध आत्म-शुद्धि प्राप्त करता है और तब मनुष्यता को ग्रहण-स्वीकार करता है। देवदुर्लभ मनुष्यत्व : नैतिकता का प्राण और प्रथम अंग __कितनी दुर्लभ और कठिन है, मनुष्यता! जो नैतिकता का प्रथम अंग है। भगवान् महावीर ने जैनकर्मसिद्धान्त की दृष्टि से मनुष्यता की दुर्लभता का विश्लेषण किया है। इसी से समझा जा सकता है कि नैतिकता के सन्दर्भ में जैन कर्मसिद्धान्त की कितनी उपयोगिता है?
9. Christian Faith and Non-Christian Religion by A.C. Bonquet p. 196 २. (क) "चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो।
माणुसत्तं सुईसद्धा, संज. चवीरियं" ॥१॥
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org