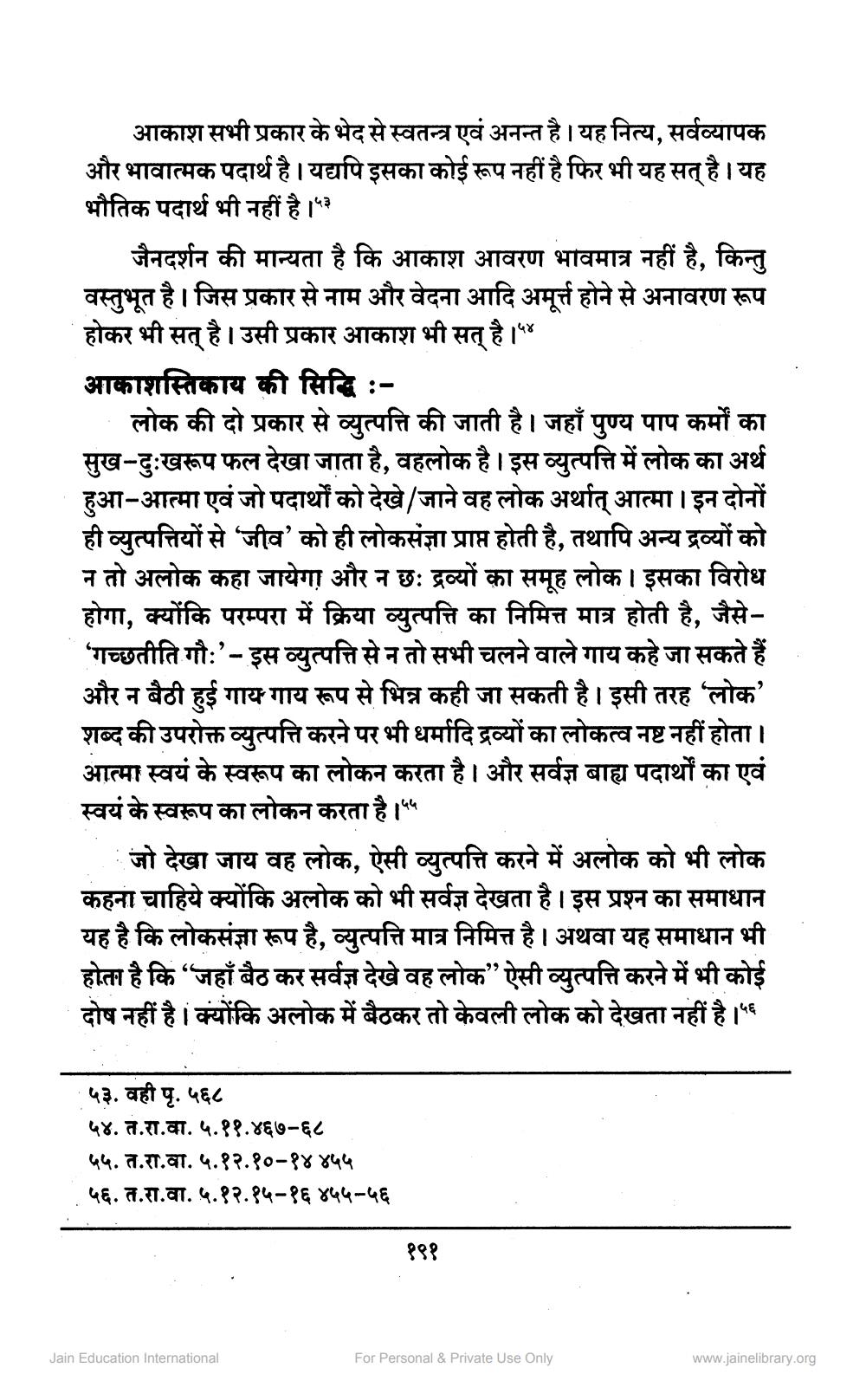________________
आकाश सभी प्रकार के भेद से स्वतन्त्र एवं अनन्त है । यह नित्य, सर्वव्यापक और भावात्मक पदार्थ है । यद्यपि इसका कोई रूप नहीं है फिर भी यह सत् है । यह भौतिक पदार्थ भी नहीं है । ५३
जैनदर्शन की मान्यता है कि आकाश आवरण भावमात्र नहीं है, किन्तु वस्तुभूत है । जिस प्रकार से नाम और वेदना आदि अमूर्त होने से अनावरण रूप होकर भी सत् है । उसी प्रकार आकाश भी सत् है । ५४
आकाशस्तिकाय की सिद्धि
लोक की दो प्रकार से व्युत्पत्ति की जाती है । जहाँ पुण्य पाप कर्मों का सुख-दुःखरूप फल देखा जाता है, वहलोक है। इस व्युत्पत्ति में लोक का अर्थ हुआ-आत्मा एवं जो पदार्थों को देखे / जाने वह लोक अर्थात् आत्मा । इन दोनों ही व्युत्पत्तियों से 'जीव' को ही लोकसंज्ञा प्राप्त होती है, तथापि अन्य द्रव्यों को न तो अलोक कहा जायेगा और न छः द्रव्यों का समूह लोक । इसका विरोध होगा, क्योंकि परम्परा में क्रिया व्युत्पत्ति का निमित्त मात्र होती है, जैसे'गच्छतीति गौः ' - इस व्युत्पत्ति से न तो सभी चलने वाले गाय कहे जा सकते हैं और न बैठी हुई गाय गाय रूप से भिन्न कही जा सकती है । इसी तरह 'लोक' शब्द की उपरोक्त व्युत्पत्ति करने पर भी धर्मादि द्रव्यों का लोकत्व नष्ट नहीं होता । आत्मा स्वयं के स्वरूप का लोकन करता है । और सर्वज्ञ बाह्य पदार्थों का एवं स्वयं के स्वरूप का लोकन करता है । ५५
· -
जो देखा जाय वह लोक, ऐसी व्युत्पत्ति करने में अलोक को भी लोक कहना चाहिये क्योंकि अलोक को भी सर्वज्ञ देखता है। इस प्रश्न का समाधान यह है कि लोकसंज्ञा रूप है, व्युत्पत्ति मात्र निमित्त है । अथवा यह समाधान भी होता है कि “जहाँ बैठ कर सर्वज्ञ देखे वह लोक" ऐसी व्युत्पत्ति करने में भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि अलोक में बैठकर तो केवली लोक को देखता नहीं है । ५६
1
५३. वही पृ. ५६८
५४. त. रा. वा. ५.११.४६७-६८
५५. त. रा. वा. ५.१२.१०-१४४५५
५६. त. रा. वा. ५.१२.१५-१६४५५-५६
Jain Education International
१९१
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org