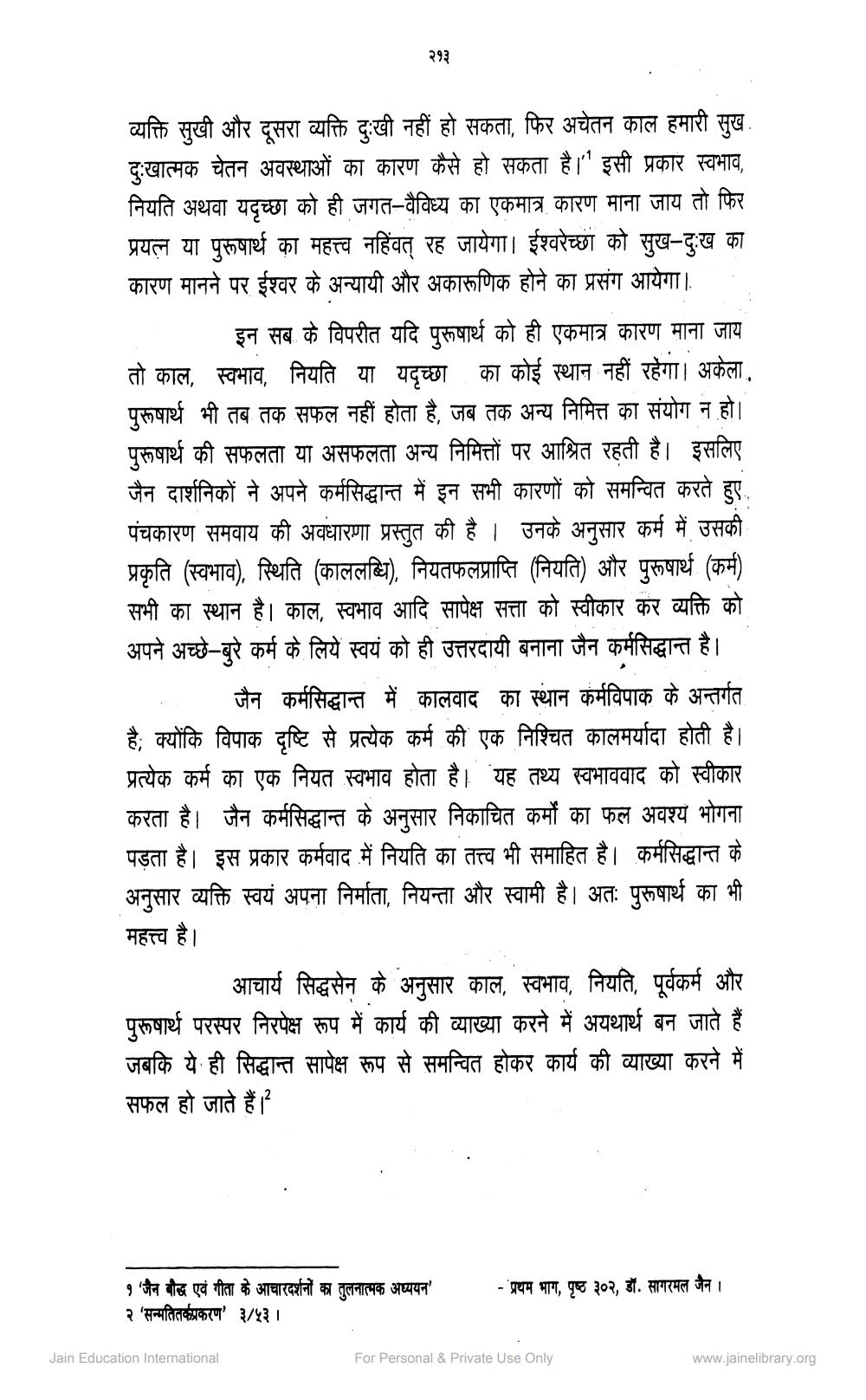________________
२१३
व्यक्ति सुखी और दूसरा व्यक्ति दुःखी नहीं हो सकता, फिर अचेतन काल हमारी सुख. दुःखात्मक चेतन अवस्थाओं का कारण कैसे हो सकता है।" इसी प्रकार स्वभाव, नियति अथवा यदृच्छा को ही जगत-वैविध्य का एकमात्र कारण माना जाय तो फिर प्रयत्न या पुरूषार्थ का महत्त्व नहिंवत् रह जायेगा। ईश्वरेच्छा को सुख-दुःख का कारण मानने पर ईश्वर के अन्यायी और अकारूणिक होने का प्रसंग आयेगा।
इन सब के विपरीत यदि पुरूषार्थ को ही एकमात्र कारण माना जाय तो काल, स्वभाव, नियति या यदृच्छा का कोई स्थान नहीं रहेगा। अकेला . पुरूषार्थ भी तब तक सफल नहीं होता है, जब तक अन्य निमित्त का संयोग न हो। पुरूषार्थ की सफलता या असफलता अन्य निमित्तों पर आश्रित रहती है। इसलिए जैन दार्शनिकों ने अपने कर्मसिद्धान्त में इन सभी कारणों को समन्वित करते हुए. पंचकारण समवाय की अवधारणा प्रस्तुत की है । उनके अनुसार कर्म में उसकी प्रकृति (स्वभाव), स्थिति (काललब्धि), नियतफलप्राप्ति (नियति) और पुरूषार्थ (कर्म) सभी का स्थान है। काल, स्वभाव आदि सापेक्ष सत्ता को स्वीकार कर व्यक्ति को अपने अच्छे-बुरे कर्म के लिये स्वयं को ही उत्तरदायी बनाना जैन कर्मसिद्धान्त है।
. जैन कर्मसिद्धान्त में कालवाद का स्थान कर्मविपाक के अन्तर्गत है; क्योंकि विपाक दृष्टि से प्रत्येक कर्म की एक निश्चित कालमर्यादा होती है। प्रत्येक कर्म का एक नियत स्वभाव होता है। यह तथ्य स्वभाववाद को स्वीकार करता है। जैन कर्मसिद्धान्त के अनुसार निकाचित कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस प्रकार कर्मवाद में नियति का तत्त्व भी समाहित है। कर्मसिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपना निर्माता, नियन्ता और स्वामी है। अतः पुरूषार्थ का भी महत्त्व है।
आचार्य सिद्धसेन के अनुसार काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकर्म और पुरूषार्थ परस्पर निरपेक्ष रूप में कार्य की व्याख्या करने में अयथार्थ बन जाते हैं जबकि ये ही सिद्धान्त सापेक्ष रूप से समन्वित होकर कार्य की व्याख्या करने में सफल हो जाते हैं।
१'जैन बौद्ध एवं गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन' २ 'सन्मतितकाकरण' ३/५३ ।।
- प्रथम भाग, पृष्ठ ३०२, डॉ. सागरमल जैन ।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org