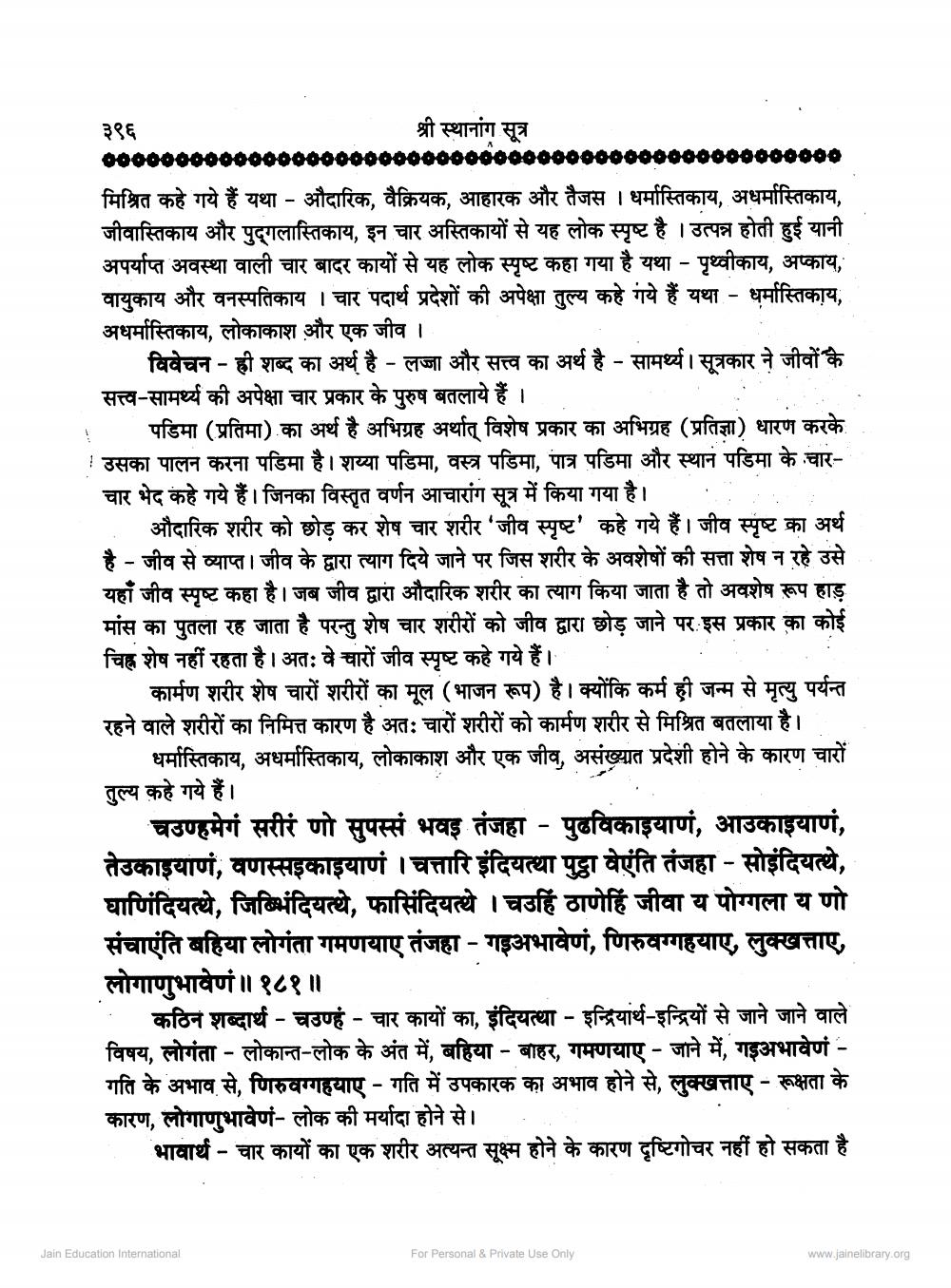________________
३९६
श्री स्थानांग सूत्र 000000000000000000000000000000000000000000000000000 मिश्रित कहे गये हैं यथा - औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तैजस । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, इन चार अस्तिकायों से यह लोक स्पृष्ट है । उत्पन्न होती हुई यानी अपर्याप्त अवस्था वाली चार बादर कायों से यह लोक स्पृष्ट कहा गया है यथा - पृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय । चार पदार्थ प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य कहे गये हैं यथा - धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव ।
विवेचन - ही शब्द का अर्थ है - लज्जा और सत्त्व का अर्थ है - सामर्थ्य । सूत्रकार ने जीवों के सत्त्व-सामर्थ्य की अपेक्षा चार प्रकार के पुरुष बतलाये हैं। । पडिमा (प्रतिमा) का अर्थ है अभिग्रह अर्थात् विशेष प्रकार का अभिग्रह (प्रतिज्ञा) धारण करके । उसका पालन करना पडिमा है। शय्या पडिमा, वस्त्र पडिमा, पात्र पडिमा और स्थान पडिमा के चार
चार भेद कहे गये हैं। जिनका विस्तृत वर्णन आचारांग सूत्र में किया गया है। ..... . औदारिक शरीर को छोड़ कर शेष चार शरीर 'जीव स्पृष्ट' कहे गये हैं। जीव स्पृष्ट का अर्थ है - जीव से व्याप्त। जीव के द्वारा त्याग दिये जाने पर जिस शरीर के अवशेषों की सत्ता शेष न रहे उसे यहाँ जीव स्पृष्ट कहा है। जब जीव द्वारा औदारिक शरीर का त्याग किया जाता है तो अवशेष रूप हाड़ मांस का पुतला रह जाता है परन्तु शेष चार शरीरों को जीव द्वारा छोड़ जाने पर इस प्रकार का कोई चिह्न शेष नहीं रहता है। अतः वे चारों जीव स्पृष्ट कहे गये हैं। ____ कार्मण शरीर शेष चारों शरीरों का मूल (भाजन रूप) है। क्योंकि कर्म ही जन्म से मृत्यु पर्यन्त रहने वाले शरीरों का निमित्त कारण है अतः चारों शरीरों को कार्मण शरीर से मिश्रित बतलाया है।
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, असंख्यात प्रदेशी होने के कारण चारों तुल्य कहे गये हैं।
चउण्हमेगं सरीरं णो सुपस्सं भवइ तंजहा - पुढविकाइयाणं, आउकाइयाणं, तेउकाइयाणं, वणस्सइकाइयाणं । चत्तारि इंदियत्था पुट्ठा वेएंति तंजहा - सोइंदियत्थे, पाणिंदियत्थे, जिब्भिंदियत्थे, फासिंदियत्थे । चउहिं ठाणेहिं जीवा य पोग्गला य णो संचाएंति बहिया लोगंता गमणयाए तंजहा - गइअभावेणं, णिरुवग्गहयाए, लुक्खत्ताए, लोगाणुभावेणं॥१८१॥ - कठिन शब्दार्थ - चउण्हं - चार कायों का, इंदियत्था - इन्द्रियार्थ-इन्द्रियों से जाने जाने वाले विषय, लोगंता - लोकान्त-लोक के अंत में, बहिया - बाहर, गमणयाए - जाने में, गइअभावेणं - गति के अभाव से, णिरुवग्गहयाए - गति में उपकारक का अभाव होने से, लुक्खत्ताए - रूक्षता के कारण, लोगाणुभावेणं- लोक की मर्यादा होने से।
भावार्थ - चार कायों का एक शरीर अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org