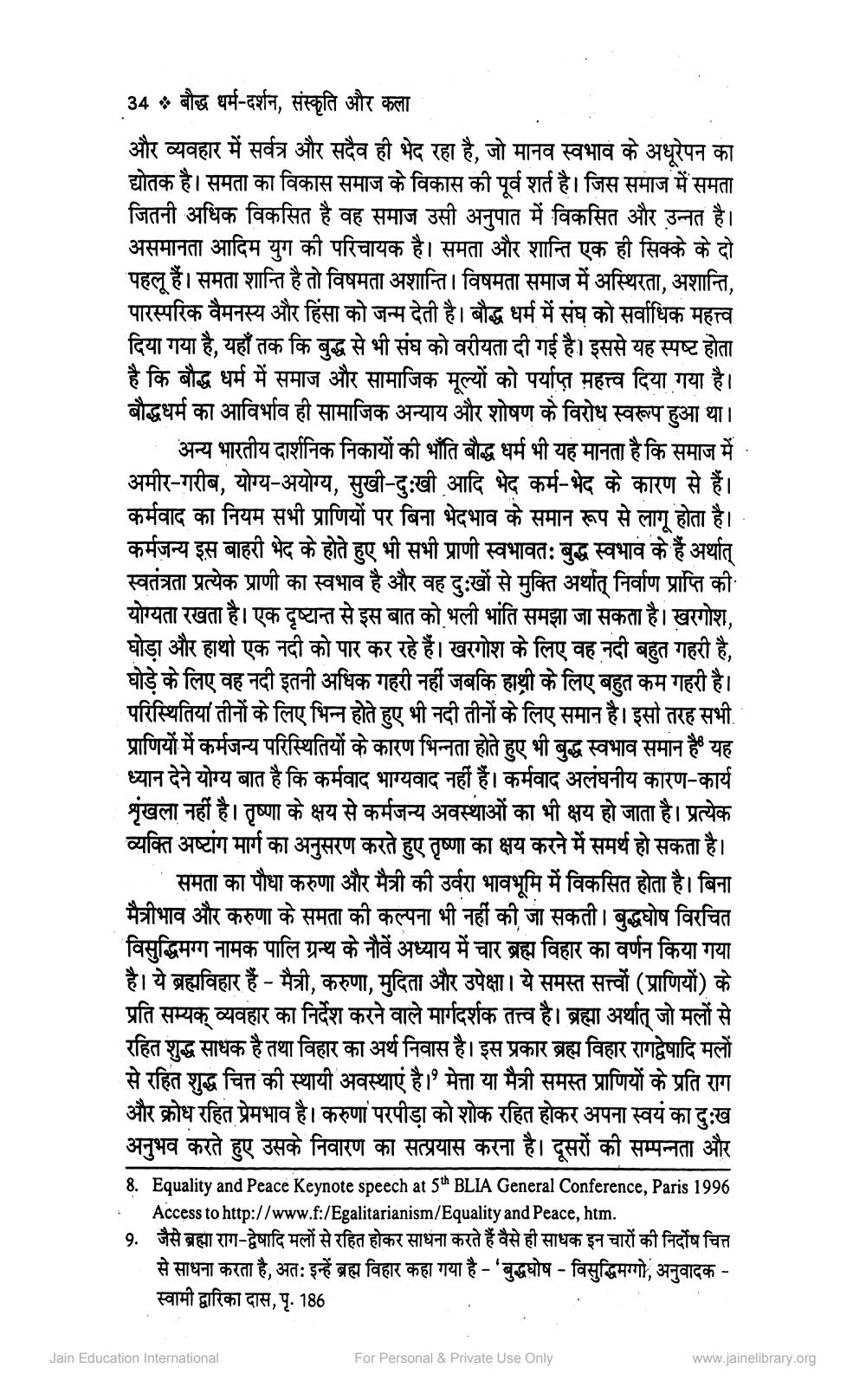________________
34 * बौद्ध धर्म-दर्शन, संस्कृति और कला
और व्यवहार में सर्वत्र और सदैव ही भेद रहा है, जो मानव स्वभाव के अधूरेपन का द्योतक है। समता का विकास समाज के विकास की पूर्व शर्त है। जिस समाज में समता जितनी अधिक विकसित है वह समाज उसी अनुपात में विकसित और उन्नत है। असमानता आदिम युग की परिचायक है। समता और शान्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समता शान्ति है तो विषमता अशान्ति। विषमता समाज में अस्थिरता, अशान्ति, पारस्परिक वैमनस्य और हिंसा को जन्म देती है। बौद्ध धर्म में संघ को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि बुद्ध से भी संघ को वरीयता दी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में समाज और सामाजिक मूल्यों को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। बौद्धधर्म का आविर्भाव ही सामाजिक अन्याय और शोषण के विरोध स्वरूप हुआ था। __अन्य भारतीय दार्शनिक निकायों की भाँति बौद्ध धर्म भी यह मानता है कि समाज में : अमीर-गरीब, योग्य-अयोग्य, सुखी-दुःखी आदि भेद कर्म-भेद के कारण से हैं। कर्मवाद का नियम सभी प्राणियों पर बिना भेदभाव के समान रूप से लागू होता है। कर्मजन्य इस बाहरी भेद के होते हुए भी सभी प्राणी स्वभावतः बुद्ध स्वभाव के हैं अर्थात् स्वतंत्रता प्रत्येक प्राणी का स्वभाव है और वह दुःखों से मुक्ति अर्थात् निर्वाण प्राप्ति की योग्यता रखता है। एक दृष्टान्त से इस बात को भली भांति समझा जा सकता है। खरगोश, घोड़ा और हाथो एक नदी को पार कर रहे हैं। खरगोश के लिए वह नदी बहुत गहरी है, घोड़े के लिए वह नदी इतनी अधिक गहरी नहीं जबकि हाथी के लिए बहुत कम गहरी है। परिस्थितियां तीनों के लिए भिन्न होते हुए भी नदी तीनों के लिए समान है। इसी तरह सभी. प्राणियों में कर्मजन्य परिस्थितियों के कारण भिन्नता होते हुए भी बुद्ध स्वभाव समान है यह ध्यान देने योग्य बात है कि कर्मवाद भाग्यवाद नहीं हैं। कर्मवाद अलंघनीय कारण-कार्य श्रृंखला नहीं है। तृष्णा के क्षय से कर्मजन्य अवस्थाओं का भी क्षय हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अष्टांग मार्ग का अनुसरण करते हुए तृष्णा का क्षय करने में समर्थ हो सकता है।
समता का पौधा करुणा और मैत्री की उर्वरा भावभूमि में विकसित होता है। बिना मैत्रीभाव और करुणा के समता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुद्धघोष विरचित विसुद्धिमग्ग नामक पालि ग्रन्थ के नौवें अध्याय में चार ब्रह्म विहार का वर्णन किया गया है। ये ब्रह्मविहार हैं - मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये समस्त सत्त्वों (प्राणियों) के प्रति सम्यक् व्यवहार का निर्देश करने वाले मार्गदर्शक तत्त्व है। ब्रह्मा अर्थात् जो मलों से रहित शुद्ध साधक है तथा विहार का अर्थ निवास है। इस प्रकार ब्रह्म विहार रागद्वेषादि मलों से रहित शुद्ध चित्त की स्थायी अवस्थाएं है।' मेत्ता या मैत्री समस्त प्राणियों के प्रति राग और क्रोध रहित प्रेमभाव है। करुणा परपीड़ा को शोक रहित होकर अपना स्वयं का दुःख अनुभव करते हुए उसके निवारण का सत्प्रयास करना है। दूसरों की सम्पन्नता और 8. Equality and Peace Keynote speech at 5th BLIA General Conference, Paris 1996 + Access to http://www.f:/Egalitarianism/Equality and Peace, htm. 9. जैसे ब्रह्मा राग-द्वेषादि मलों से रहित होकर साधना करते हैं वैसे ही साधक इन चारों की निर्दोष चित्त
से साधना करता है, अतः इन्हें ब्रह्म विहार कहा गया है - 'बुद्धघोष - विसुद्धिमग्गो, अनुवादक - स्वामी द्वारिका दास, पृ. 186
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org