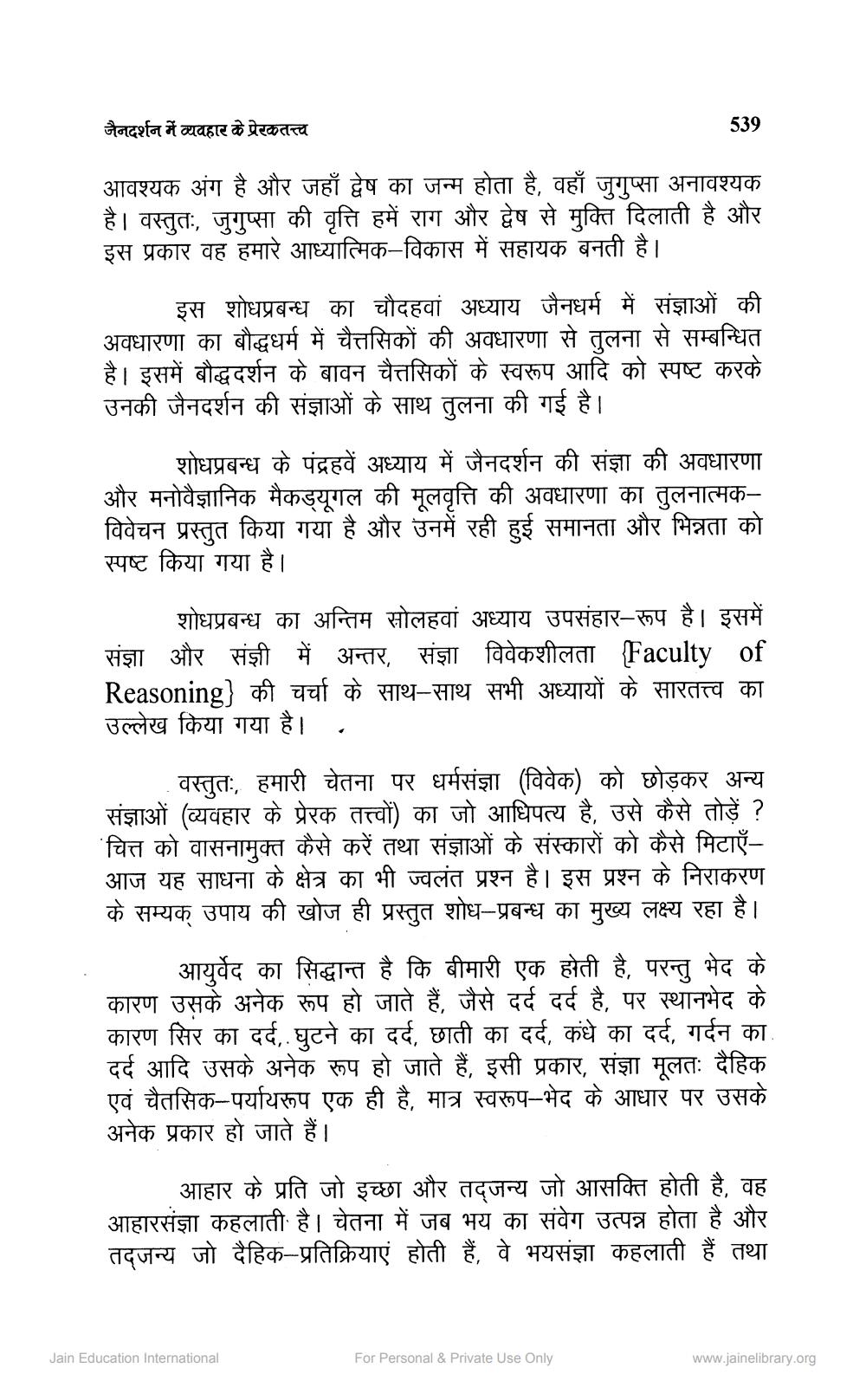________________
जैनदर्शन में व्यवहार के प्रेरकतत्त्व
539
आवश्यक अंग है और जहाँ द्वेष का जन्म होता है, वहाँ जुगुप्सा अनावश्यक है। वस्तुतः, जुगुप्सा की वृत्ति हमें राग और द्वेष से मुक्ति दिलाती है और इस प्रकार वह हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक बनती है।
इस शोधप्रबन्ध का चौदहवां अध्याय जैनधर्म में संज्ञाओं की अवधारणा का बौद्धधर्म में चैत्तसिकों की अवधारणा से तुलना से सम्बन्धित है। इसमें बौद्धदर्शन के बावन चैत्तसिकों के स्वरूप आदि को स्पष्ट करके उनकी जैनदर्शन की संज्ञाओं के साथ तुलना की गई है।
शोधप्रबन्ध के पंद्रहवें अध्याय में जैनदर्शन की संज्ञा की अवधारणा और मनोवैज्ञानिक मैकड्यूगल की मूलवृत्ति की अवधारणा का तुलनात्मकविवेचन प्रस्तुत किया गया है और उनमें रही हुई समानता और भिन्नता को स्पष्ट किया गया है।
शोधप्रबन्ध का अन्तिम सोलहवां अध्याय उपसंहार-रूप है। इसमें संज्ञा और संज्ञी में अन्तर, संज्ञा विवेकशीलता {Faculty of Reasoning} की चर्चा के साथ-साथ सभी अध्यायों के सारतत्त्व का उल्लेख किया गया है। .
. वस्तुतः, हमारी चेतना पर धर्मसंज्ञा (विवेक) को छोड़कर अन्य संज्ञाओं (व्यवहार के प्रेरक तत्त्वों) का जो आधिपत्य है, उसे कैसे तोड़ें ? चित्त को वासनामुक्त कैसे करें तथा संज्ञाओं के संस्कारों को कैसे मिटाएँआज यह साधना के क्षेत्र का भी ज्वलंत प्रश्न है। इस प्रश्न के निराकरण के सम्यक् उपाय की खोज ही प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का मुख्य लक्ष्य रहा है।
आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि बीमारी एक होती है, परन्तु भेद के कारण उसके अनेक रूप हो जाते हैं, जैसे दर्द दर्द है, पर स्थानभेद के कारण सिर का दर्द, घुटने का दर्द, छाती का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द आदि उसके अनेक रूप हो जाते हैं, इसी प्रकार, संज्ञा मूलतः दैहिक एवं चैतसिक-पर्यायरूप एक ही है, मात्र स्वरूप-भेद के आधार पर उसके अनेक प्रकार हो जाते हैं।
आहार के प्रति जो इच्छा और तद्जन्य जो आसक्ति होती है, वह आहारसंज्ञा कहलाती है। चेतना में जब भय का संवेग उत्पन्न होता है और तद्जन्य जो दैहिक-प्रतिक्रियाएं होती हैं, वे भयसंज्ञा कहलाती हैं तथा
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org