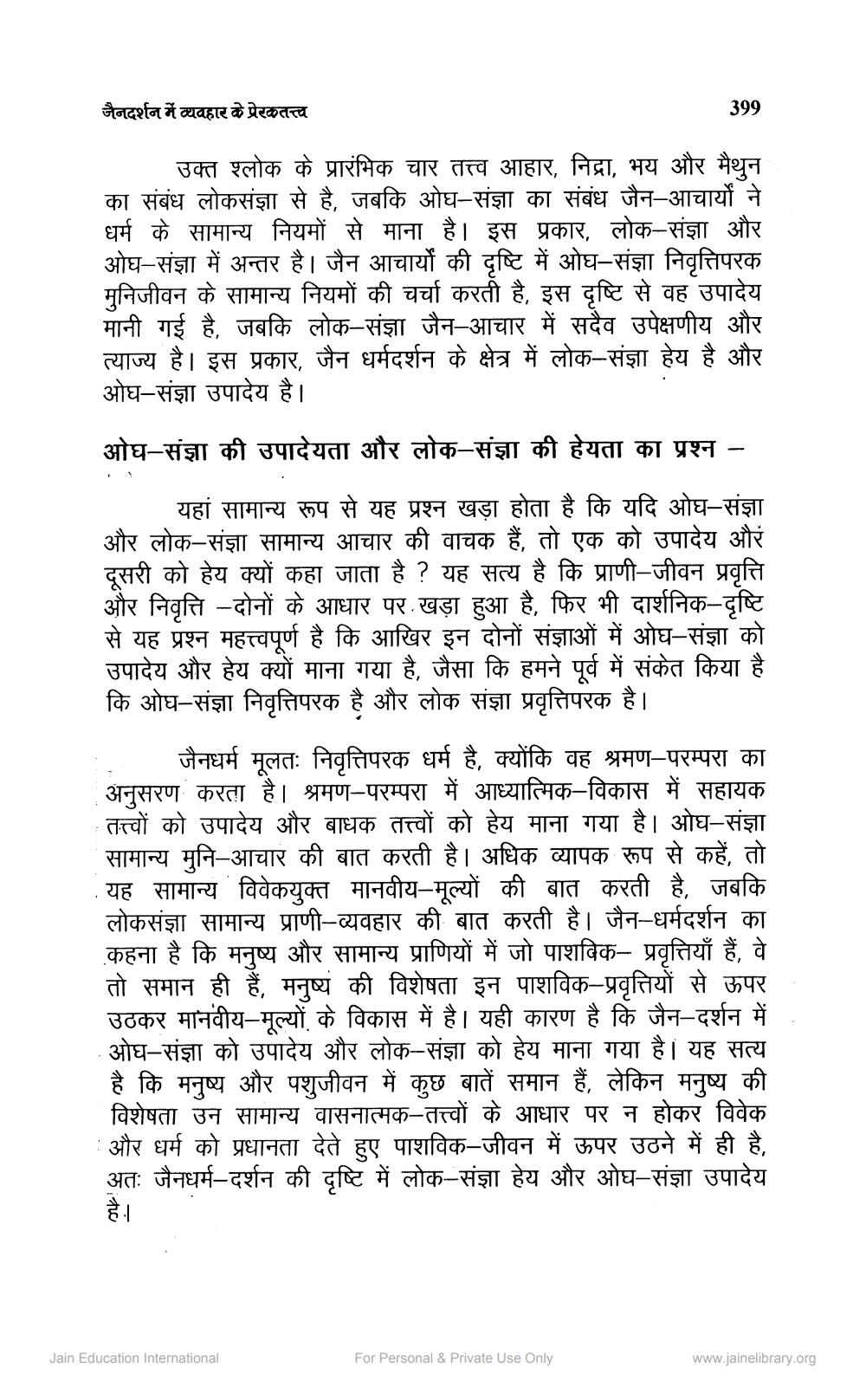________________
जैनदर्शन में व्यवहार के प्रेरकतत्त्व
399
उक्त श्लोक के प्रारंभिक चार तत्त्व आहार, निद्रा, भय और मैथुन का संबंध लोकसंज्ञा से है, जबकि ओघ-संज्ञा का संबंध जैन-आचार्यों ने धर्म के सामान्य नियमों से माना है। इस प्रकार, लोक-संज्ञा और ओघ-संज्ञा में अन्तर है। जैन आचार्यों की दृष्टि में ओघ-संज्ञा निवृत्तिपरक मुनिजीवन के सामान्य नियमों की चर्चा करती है, इस दृष्टि से वह उपादेय मानी गई है, जबकि लोक-संज्ञा जैन-आचार में सदैव उपेक्षणीय और त्याज्य है। इस प्रकार, जैन धर्मदर्शन के क्षेत्र में लोक-संज्ञा हेय है और ओघ-संज्ञा उपादेय है।
ओघ-संज्ञा की उपादेयता और लोक-संज्ञा की हेयता का प्रश्न -
यहां सामान्य रूप से यह प्रश्न खड़ा होता है कि यदि ओघ-संज्ञा और लोक-संज्ञा सामान्य आचार की वाचक हैं, तो एक को उपादेय और दूसरी को हेय क्यों कहा जाता है ? यह सत्य है कि प्राणी-जीवन प्रवृत्ति और निवृत्ति -दोनों के आधार पर खड़ा हुआ है, फिर भी दार्शनिक-दृष्टि से यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि आखिर इन दोनों संज्ञाओं में ओघ-संज्ञा को उपादेय और हेय क्यों माना गया है, जैसा कि हमने पूर्व में संकेत किया है कि ओघ-संज्ञा निवृत्तिपरक है और लोक संज्ञा प्रवृत्तिपरक है।
___ जैनधर्म मूलतः निवृत्तिपरक धर्म है, क्योंकि वह श्रमण-परम्परा का अनुसरण करता है। श्रमण-परम्परा में आध्यात्मिक विकास में सहायक तत्त्वों को उपादेय और बाधक तत्त्वों को हेय माना गया है। ओघ-संज्ञा सामान्य मुनि-आचार की बात करती है। अधिक व्यापक रूप से कहें, तो यह सामान्य विवेकयुक्त मानवीय मूल्यों की बात करती है, जबकि लोकसंज्ञा सामान्य प्राणी-व्यवहार की बात करती है। जैन धर्मदर्शन का कहना है कि मनुष्य और सामान्य प्राणियों में जो पाशविक- प्रवृत्तियाँ हैं, वे तो समान ही हैं, मनुष्य की विशेषता इन पाशविक-प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों के विकास में है। यही कारण है कि जैन-दर्शन में ओघ-संज्ञा को उपादेय और लोक-संज्ञा को हेय माना गया है। यह सत्य है कि मनुष्य और पशुजीवन में कुछ बातें समान हैं, लेकिन मनुष्य की विशेषता उन सामान्य वासनात्मक-तत्त्वों के आधार पर न होकर विवेक और धर्म को प्रधानता देते हुए पाशविक-जीवन में ऊपर उठने में ही है, अतः जैनधर्म-दर्शन की दृष्टि में लोक-संज्ञा हेय और ओघ–संज्ञा उपादेय
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org