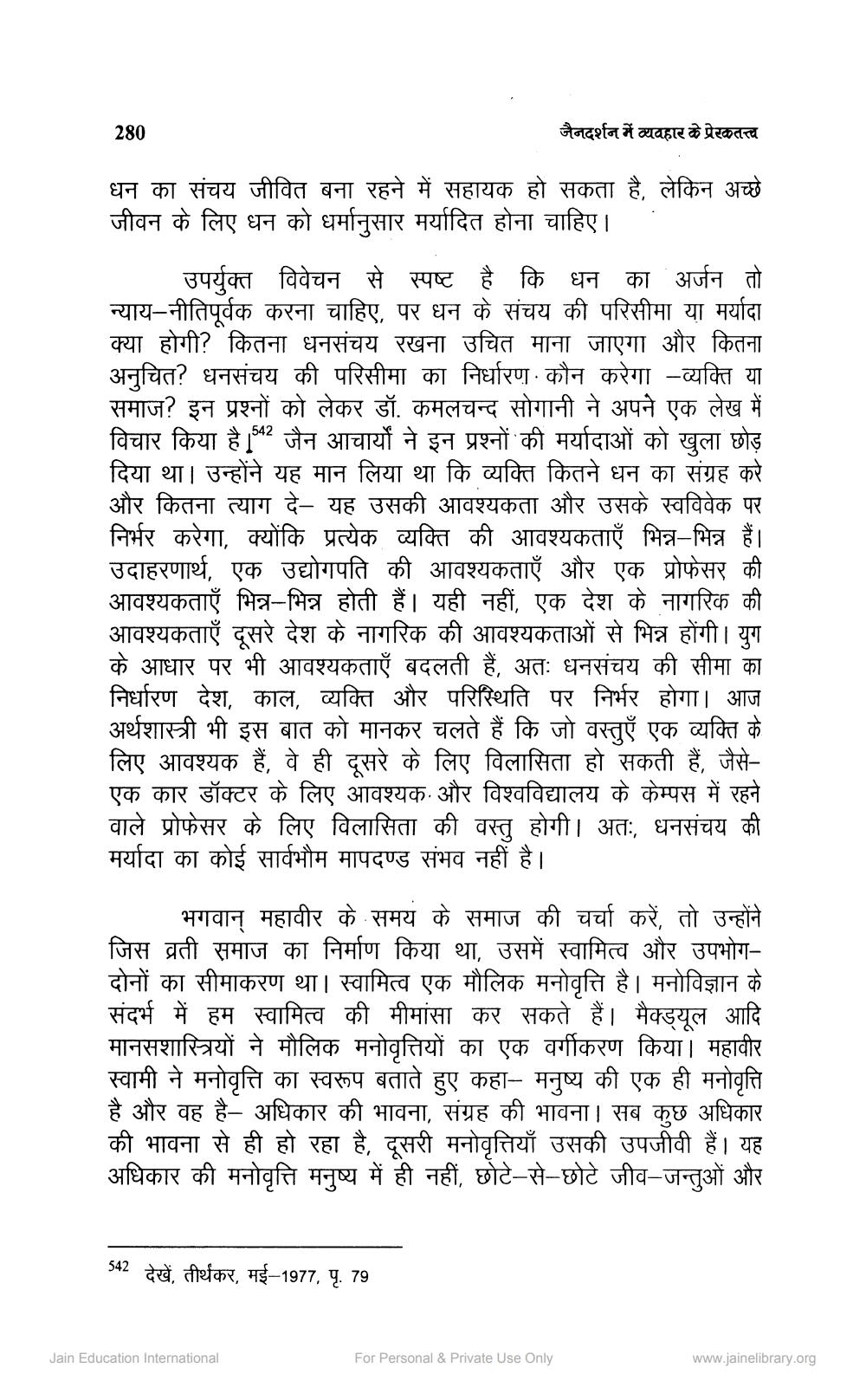________________
280
जैनदर्शन में व्यवहार के प्रेरकतत्त्व
धन का संचय जीवित बना रहने में सहायक हो सकता है, लेकिन अच्छे जीवन के लिए धन को धर्मानुसार मर्यादित होना चाहिए।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि धन का अर्जन तो न्याय-नीतिपूर्वक करना चाहिए, पर धन के संचय की परिसीमा या मर्यादा क्या होगी? कितना धनसंचय रखना उचित माना जाएगा और कितना अनुचित? धनसंचय की परिसीमा का निर्धारण कौन करेगा -व्यक्ति या समाज? इन प्रश्नों को लेकर डॉ. कमलचन्द सोगानी ने अपने एक लेख में विचार किया है।42 जैन आचार्यों ने इन प्रश्नों की मर्यादाओं को खुला छोड़ दिया था। उन्होंने यह मान लिया था कि व्यक्ति कितने धन का संग्रह करे
और कितना त्याग दे- यह उसकी आवश्यकता और उसके स्वविवेक पर निर्भर करेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, एक उद्योगपति की आवश्यकताएँ और एक प्रोफेसर की आवश्यकताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। यही नहीं, एक देश के नागरिक की आवश्यकताएँ दूसरे देश के नागरिक की आवश्यकताओं से भिन्न होंगी। युग के आधार पर भी आवश्यकताएँ बदलती हैं, अतः धनसंचय की सीमा का निर्धारण देश, काल, व्यक्ति और परिस्थिति पर निर्भर होगा। आज अर्थशास्त्री भी इस बात को मानकर चलते हैं कि जो वस्तुएँ एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, वे ही दूसरे के लिए विलासिता हो सकती हैं, जैसेएक कार डॉक्टर के लिए आवश्यक और विश्वविद्यालय के केम्पस में रहने वाले प्रोफेसर के लिए विलासिता की वस्तु होगी। अतः, धनसंचय की मर्यादा का कोई सार्वभौम मापदण्ड संभव नहीं है।
___ भगवान महावीर के समय के समाज की चर्चा करें, तो उन्होंने जिस व्रती समाज का निर्माण किया था, उसमें स्वामित्व और उपभोगदोनों का सीमाकरण था। स्वामित्व एक मौलिक मनोवृत्ति है। मनोविज्ञान के संदर्भ में हम स्वामित्व की मीमांसा कर सकते हैं। मैक्ड्यूल आदि मानसशास्त्रियों ने मौलिक मनोवृत्तियों का एक वर्गीकरण किया। महावीर स्वामी ने मनोवृत्ति का स्वरूप बताते हुए कहा- मनुष्य की एक ही मनोवृत्ति है और वह है- अधिकार की भावना, संग्रह की भावना। सब कुछ अधिकार की भावना से ही हो रहा है, दूसरी मनोवृत्तियाँ उसकी उपजीवी हैं। यह अधिकार की मनोवृत्ति मनुष्य में ही नहीं, छोटे-से-छोटे जीव-जन्तुओं और
542 देखें, तीर्थकर, मई-1977, पृ. 79
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org