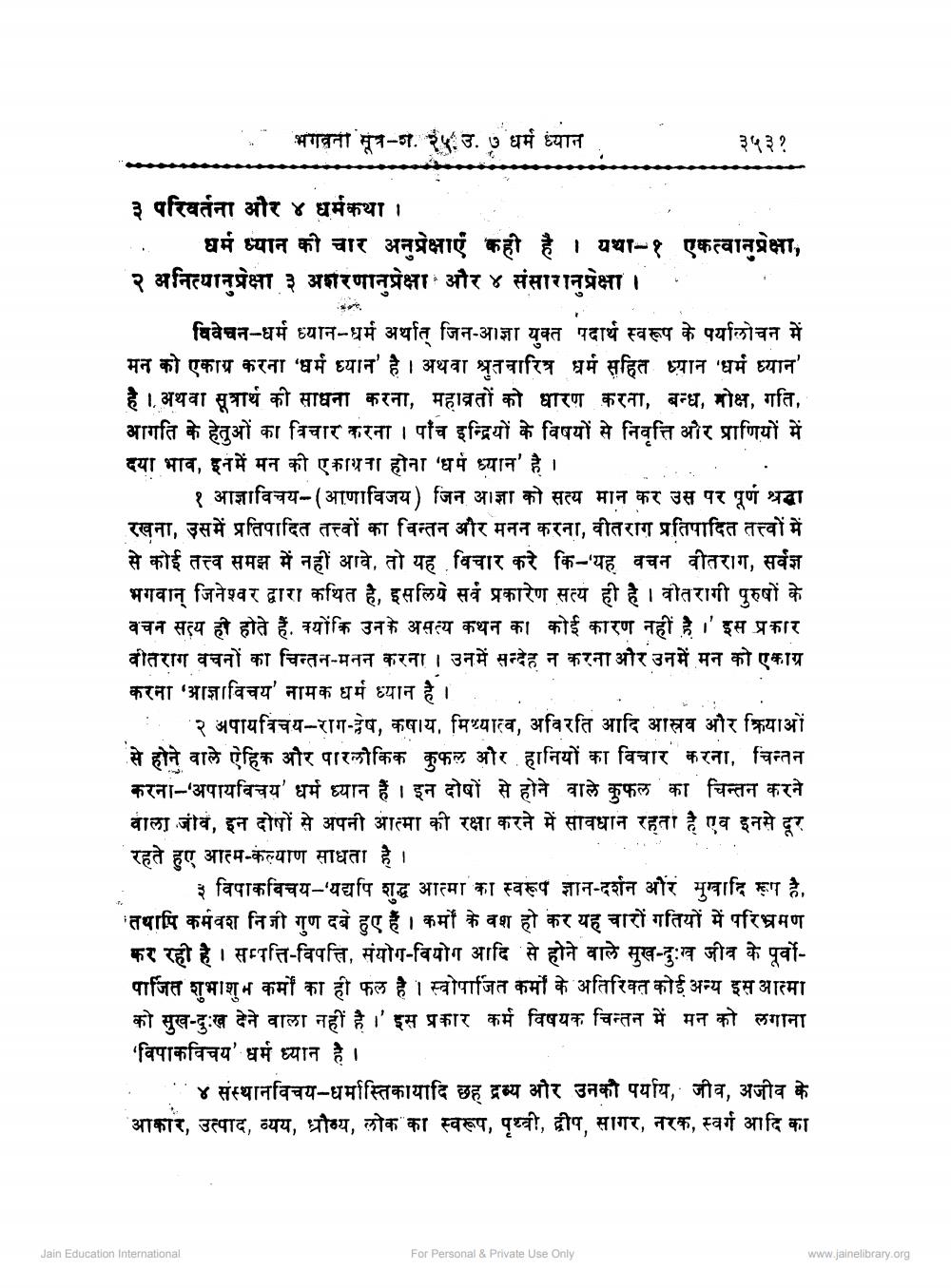________________
भगवता मूत्र-ग. २५. उ. ७ धर्म ध्यान
३५३?
३ परिवर्तना और ४ धर्मकथा ।
धर्म ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं कही है । यथा-१ एकत्वानप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा ३ अशरणानुप्रेक्षा और ४ संसारानुप्रेक्षा। .
विवेचन-धर्म ध्यान-धर्म अर्थात् जिन-आज्ञा युक्त पदार्थ स्वरूप के पर्यालोचन में मन को एकाग्र करना 'धर्म ध्यान' है । अथवा श्रुतचारित्र धर्म सहित ध्यान 'धर्म ध्यान' है । अथवा सूत्रार्थ की साधना करना, महाव्रतों को धारण करना, बन्ध, मोक्ष, गति, आगति के हेतुओं का विचार करना । पाँच इन्द्रियों के विषयों से निवृत्ति और प्राणियों में दया भाव, इनमें मन की एकाग्रता होना 'धर्म ध्यान' है। ......
१ आज्ञाविचय-(आणाविजय) जिन आज्ञा को सत्य मान कर उस पर पूर्ण श्रद्धा रखना, उसमें प्रतिपादित तत्त्वों का चिन्तन और मनन करना, वीतराग प्रतिपादित तत्त्वों में से कोई तत्त्व समझ में नहीं आवे, तो यह विचार करे कि-'यह वचन वीतराग, सर्वज्ञ भगवान् जिनेश्वर द्वारा कथित है, इसलिये सर्व प्रकारेण सत्य ही है । वीतरागी पुरुषों के वचन सत्य ही होते हैं. क्योंकि उनके असत्य कथन का कोई कारण नहीं है।' इस प्रकार वीतराग वचनों का चिन्तन-मनन करना । उनमें सन्देह न करना और उनमें मन को एकाग्र करना आज्ञाविचय' नामक धर्म ध्यान है।
२ अपायविचय-राग-द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति आदि आस्रव और क्रियाओं से होने वाले ऐहिक और पारलौकिक कुफल और हानियों का विचार करना, चिन्तन करना-'अपायविचय' धर्म ध्यान हैं । इन दोषों से होने वाले कुफल का चिन्तन करने वाला जीव, इन दोषों से अपनी आत्मा की रक्षा करने में सावधान रहता है एव इनसे दूर रहते हुए आत्म-कल्याण साधता है।
३ विपाकविचय-'यद्यपि शुद्ध आत्मा का स्वरूप ज्ञान-दर्शन और मुग्वादि रूप है, तथापि कर्मवश निजी गुण दबे हुए हैं । कर्मों के वश हो कर यह चारों गतियों में परिभ्रमण कर रही है । सम्पत्ति-विपत्ति, संयोग-वियोग आदि से होने वाले सुख-दुःख जीव के पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्मों का ही फल है । स्वोपार्जित कर्मों के अतिरिक्त कोई अन्य इस आत्मा को सुख-दुःख देने वाला नहीं है।' इस प्रकार कर्म विषयक चिन्तन में मन को लगाना 'विपाकविचय' धर्म ध्यान है।
४ संस्थानविचय-धर्मास्तिकायादि छह द्रव्य और उनको पर्याय, जीव, अजीव के आकार, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, लोक का स्वरूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, स्वर्ग आदि का
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org