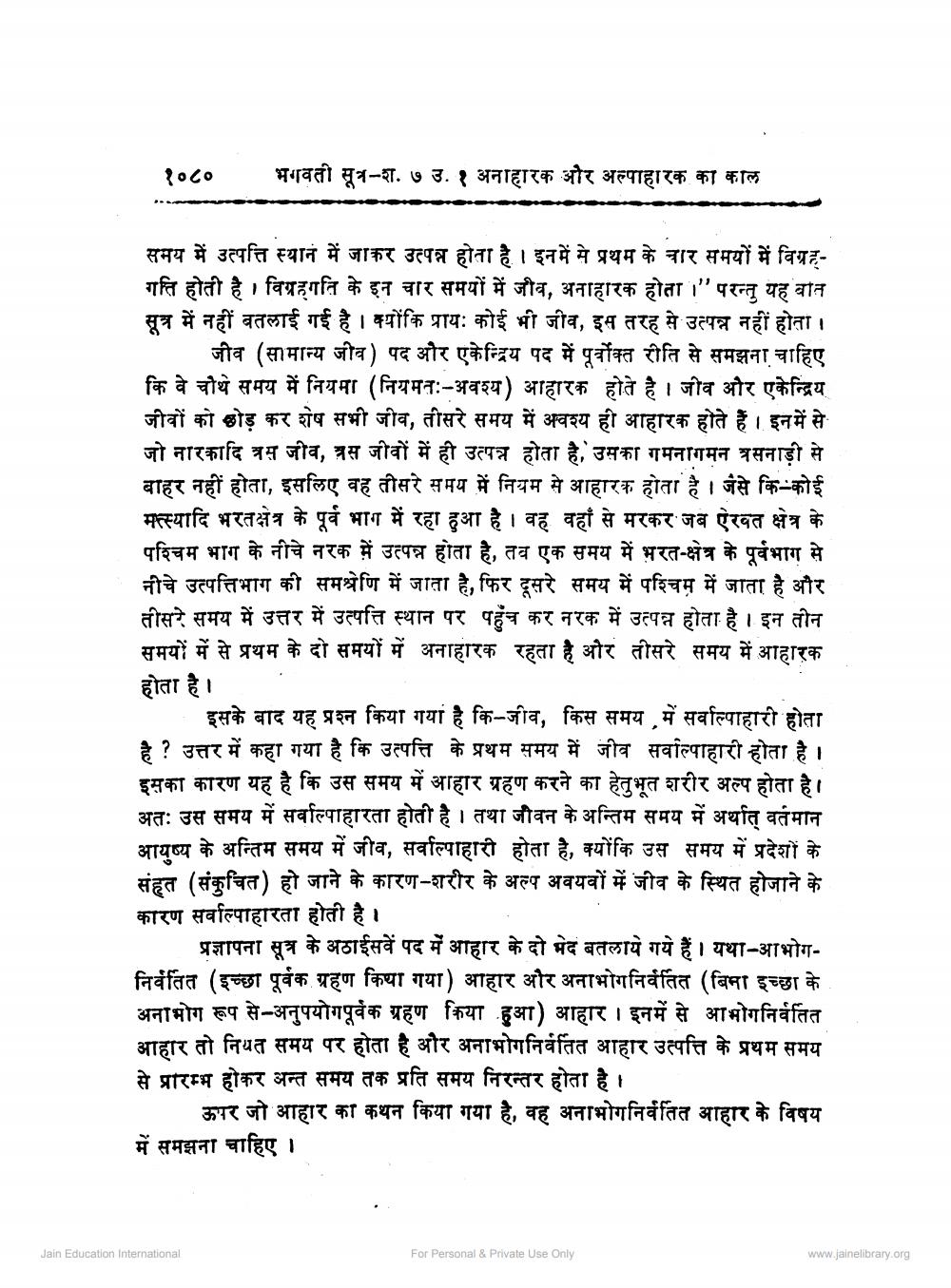________________
१०८०
भगवती सत्र-श. ७उ.. अनाहारक और अल्पाहारक का काल
समय में उत्पत्ति स्थान में जाकर उत्पन्न होता है । इनमें से प्रथम के चार समयों में विग्रहगति होती है । विग्रहगति के इन चार समयों में जीव, अनाहारक होता।" परन्तु यह बात सूत्र में नहीं बतलाई गई है । क्योंकि प्रायः कोई भी जीव, इस तरह से उत्पन्न नहीं होता।
जीव (सामान्य जीव) पद और एकेन्द्रिय पद में पूर्वोक्त रीति से समझना चाहिए कि वे चौथे समय में नियमा (नियमत:-अवश्य) आहारक होते है । जीव और एकेन्द्रिय जीवों को छोड़ कर शेष सभी जीव, तीसरे समय में अवश्य ही आहारक होते हैं। इनमें से जो नारकादि त्रस जीव, बस जीवों में ही उत्पन्न होता है, उसका गमनागमन सनाड़ी से बाहर नहीं होता, इसलिए वह तीसरे समय में नियम से आहारक होता है । जैसे कि कोई मत्स्यादि भरतक्षेत्र के पूर्व भाग में रहा हुआ है । वह वहाँ से मरकर जब ऐरक्त क्षेत्र के पश्चिम भाग के नीचे नरक में उत्पन्न होता है, तव एक समय में भरत-क्षेत्र के पूर्वभाग से नीचे उत्पत्तिभाग की समश्रेणि में जाता है, फिर दूसरे समय में पश्चिम में जाता है और तीसरे समय में उत्तर में उत्पत्ति स्थान पर पहुंच कर नरक में उत्पन्न होता है । इन तीन समयों में से प्रथम के दो समयों में अनाहारक रहता है और तीसरे समय में आहारक
होता है।
इसके बाद यह प्रश्न किया गया है कि-जीव, किस समय में सर्वाल्पाहारी होता है ? उत्तर में कहा गया है कि उत्पत्ति के प्रथम समय में जीव सर्वाल्पाहारी होता है। इसका कारण यह है कि उस समय में आहार ग्रहण करने का हेतुभूत शरीर अल्प होता है। अतः उस समय में सर्वाल्पाहारता होती है । तथा जीवन के अन्तिम समय में अर्थात् वर्तमान आयष्य के अन्तिम समय में जीव, सल्पिाहारी होता है, क्योंकि उस समय में प्रदेशों के संहृत (संकुचित) हो जाने के कारण-शरीर के अल्प अवयवों में जीव के स्थित होजाने के कारण सर्वाल्पाहारता होती है।
प्रज्ञापना सूत्र के अठाईसवें पद में आहार के दो भेद बतलाये गये हैं। यथा-आभोगनिर्वतित (इच्छा पूर्वक ग्रहण किया गया) आहार और अनाभोगनिर्वतित (बिमा इच्छा के अनाभोग रूप से अनुपयोगपूर्वक ग्रहण किया हुआ) आहार । इनमें से आभोगनिर्वतित आहार तो नियत समय पर होता है और अनाभोगनिर्वतित आहार उत्पत्ति के प्रथम समय से प्रारम्भ होकर अन्त समय तक प्रति समय निरन्तर होता है।
ऊपर जो आहार का कथन किया गया है, वह अनाभोगनिर्वतित आहार के विषय में समझना चाहिए।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org