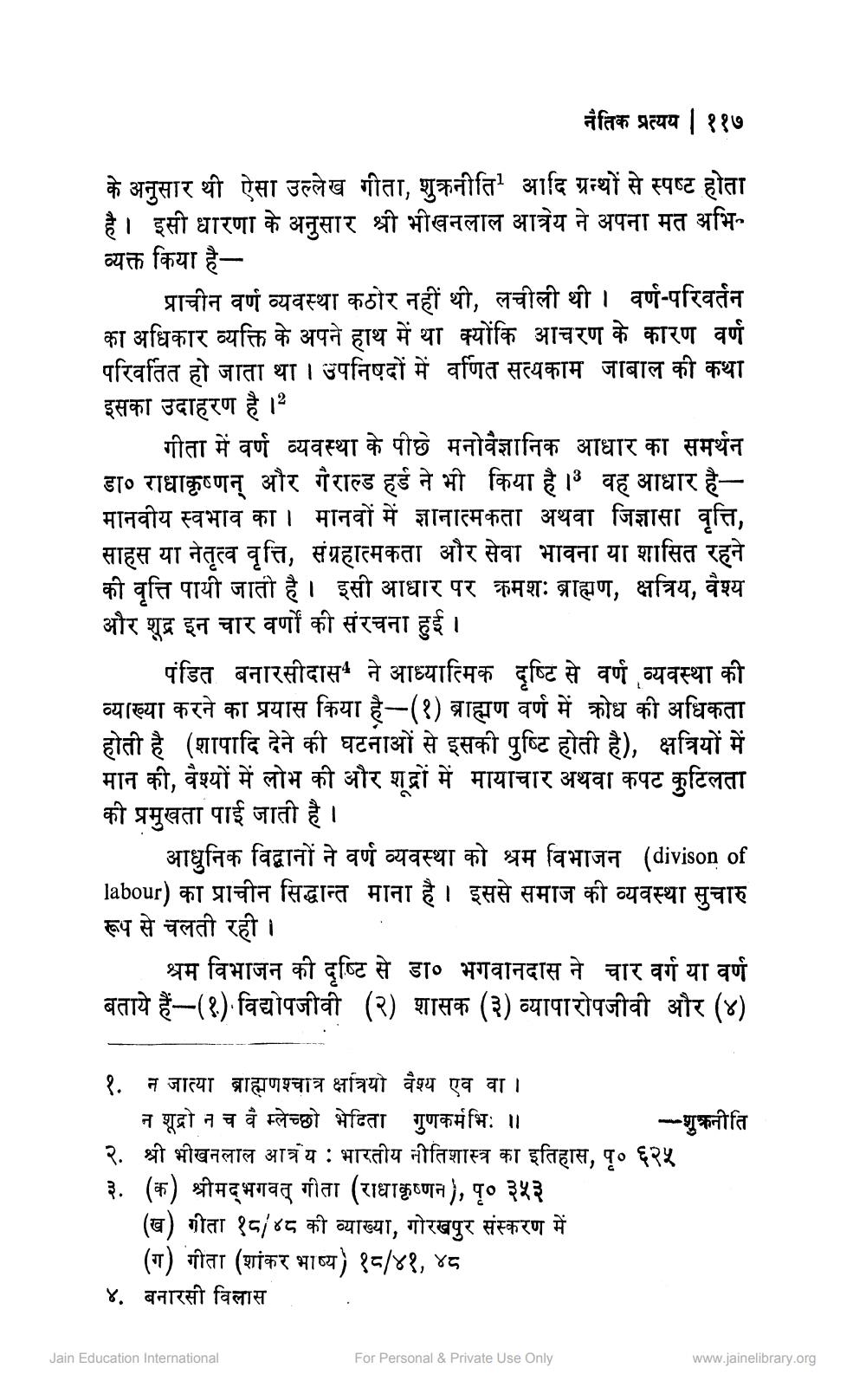________________
नैतिक प्रत्यय | ११७
के
अनुसार थी ऐसा उल्लेख गीता, शुक्रनीति' आदि ग्रन्थों से स्पष्ट होता है । इसी धारणा के अनुसार श्री भीखनलाल आत्रेय ने अपना मत अभि व्यक्त किया है
प्राचीन वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी, लचीली थी । वर्ण- परिवर्तन का अधिकार व्यक्ति के अपने हाथ में था क्योंकि आचरण के कारण वर्ण परिवर्तित हो जाता था । उपनिषदों में वर्णित सत्यकाम जाबाल की कथा इसका उदाहरण है । 2
गीता में वर्ण व्यवस्था के पीछे मनोवैज्ञानिक आधार का समर्थन डा० राधाकृष्णन् और गैराल्ड हर्ड ने भी किया है । वह आधार है— मानवीय स्वभाव का । मानवों में ज्ञानात्मकता अथवा जिज्ञासा वृत्ति, साहस या नेतृत्व वृत्ति, संग्रहात्मकता और सेवा भावना या शासित रहने की वृत्ति पायी जाती है । इसी आधार पर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इन चार वर्णों की संरचना हुई ।
पंडित बनारसीदास ने आध्यात्मिक दृष्टि से वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने का प्रयास किया है - (१) ब्राह्मण वर्ण में क्रोध की अधिकता होती है ( शापादि देने की घटनाओं से इसकी पुष्टि होती है), क्षत्रियों में मान की, वैश्यों में लोभ की और शूद्रों में मायाचार अथवा कपट कुटिलता की प्रमुखता पाई जाती है ।
आधुनिक विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन (divison of labour) का प्राचीन सिद्धान्त माना है । इससे समाज की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही ।
श्रम विभाजन की दृष्टि से डा० भगवानदास ने चार वर्ग या वर्ण बताये हैं - ( १ ) विद्योपजीवी ( २ ) शासक ( ३ ) व्यापारोपजीवी और ( ४ )
१. न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव वा ।
न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेटिता गुणकर्मभिः ॥
२. श्री भीखनलाल आत्रेय : भारतीय नीतिशास्त्र का इतिहास, पृ० ६२५
३. ( क ) श्रीमद्भगवत् गीता (राधाकृष्णन ), पृ० ३५३
(ख) गीता १८ / ४८ की व्याख्या, गोरखपुर संस्करण में
(ग) गीता ( शांकर भाष्य ) १८ / ४१, ४८
४. बनारसी विलास
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
शुक्रनीति
www.jainelibrary.org