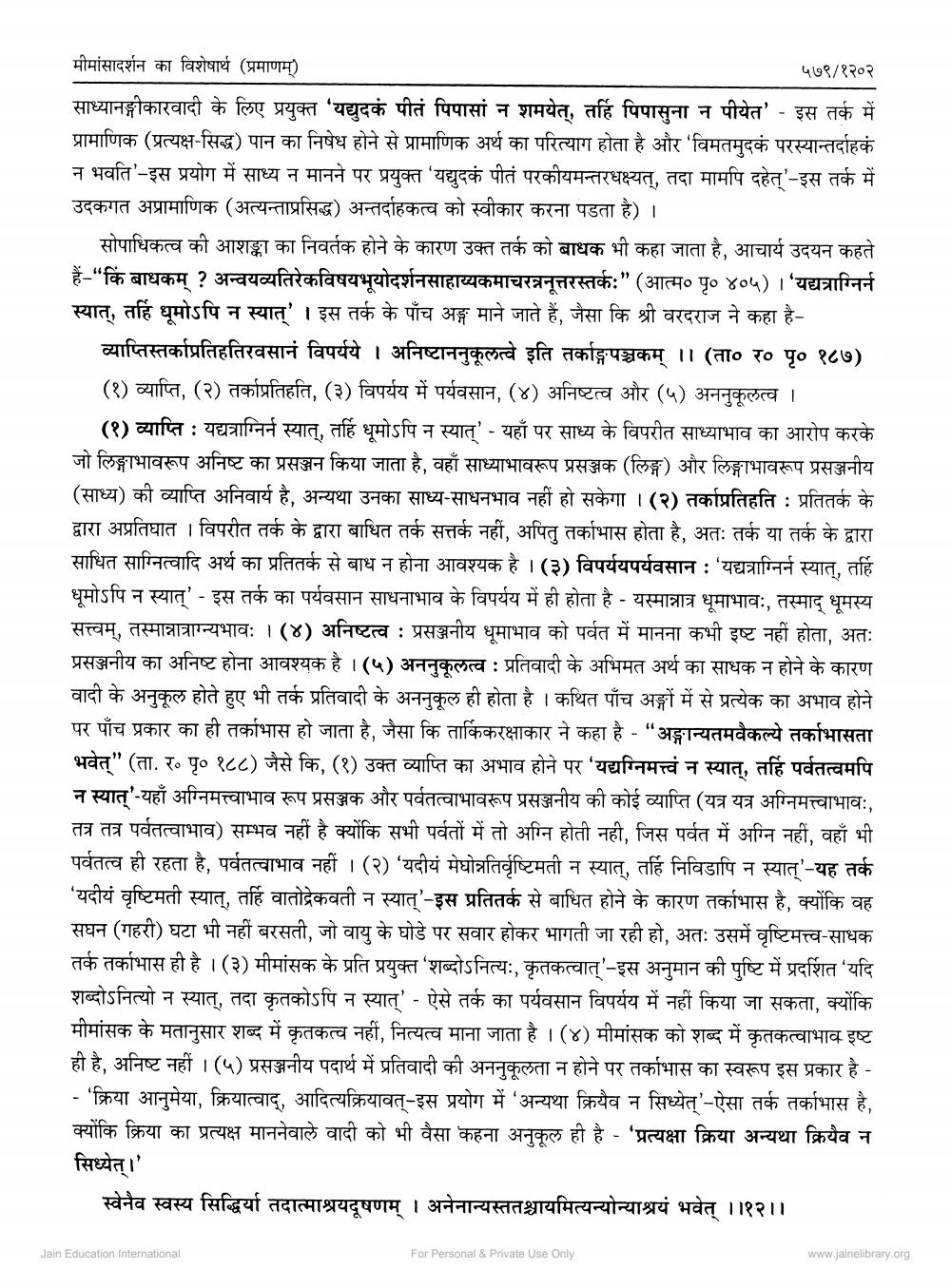________________
मीमांसादर्शन का विशेषार्थ (प्रमाणम्)
५७९/१२०२ साध्यानङ्गीकारवादी के लिए प्रयुक्त 'यधुदकं पीतं पिपासां न शमयेत्, तर्हि पिपासुना न पीयेत' - इस तर्क में प्रामाणिक (प्रत्यक्ष-सिद्ध) पान का निषेध होने से प्रामाणिक अर्थ का परित्याग होता है और 'विमतमुदकं परस्यान्तर्दाहकं न भवति'-इस प्रयोग में साध्य न मानने पर प्रयुक्त 'यधुदकं पीतं परकीयमन्तरधक्ष्यत, तदा मामपि दहेत्'-इस तर्क में उदकगत अप्रामाणिक (अत्यन्ताप्रसिद्ध) अन्तर्दाहकत्व को स्वीकार करना पडता है) ।
सोपाधिकत्व की आशङ्का का निवर्तक होने के कारण उक्त तर्क को बाधक भी कहा जाता है, आचार्य उदयन कहते हैं-"किं बाधकम् ? अन्वयव्यतिरेकविषयभूयोदर्शनसाहाय्यकमाचरन्ननूत्तरस्तर्कः" (आत्म० पृ० ४०५) । 'यद्यत्राग्निर्न स्यात्, तर्हि धूमोऽपि न स्यात्' । इस तर्क के पाँच अङ्ग माने जाते हैं, जैसा कि श्री वरदराज ने कहा है
व्याप्तिस्तर्काप्रतिहतिरवसानं विपर्यये । अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्काङ्गपञ्चकम् ।। (ता० र० पृ० १८७) (१) व्याप्ति, (२) तर्काप्रतिहति, (३) विपर्यय में पर्यवसान, (४) अनिष्टत्व और (५) अननुकूलत्व ।
(१) व्याप्ति : यद्यत्राग्निर्न स्यात्, तर्हि धूमोऽपि न स्यात्' - यहाँ पर साध्य के विपरीत साध्याभाव का आरोप करके जो लिङ्गाभावरूप अनिष्ट का प्रसञ्जन किया जाता है, वहाँ साध्याभावरूप प्रसञ्जक (लिङ्ग) और लिङ्गाभावरूप प्रसञ्जनीय (साध्य) की व्याप्ति अनिवार्य है, अन्यथा उनका साध्य-साधनभाव नहीं हो सकेगा । (२) तर्काप्रतिहति : प्रतितर्क के द्वारा अप्रतिघात । विपरीत तर्क के द्वारा बाधित तर्क सत्तर्क नहीं, अपितु तर्काभास होता है, अतः तर्क या तर्क के द्वारा साधित साग्नित्वादि अर्थ का प्रतितर्क से बाध न होना आवश्यक है । (३) विपर्ययपर्यवसान : 'यद्यत्राग्निर्न स्यात्, तर्हि धूमोऽपि न स्यात्' - इस तर्क का पर्यवसान साधनाभाव के विपर्यय में ही होता है - यस्मान्नात्र धूमाभावः, तस्माद् धूमस्य सत्त्वम्, तस्मान्नात्राग्न्यभावः । (४) अनिष्टत्व : प्रसञ्जनीय धूमाभाव को पर्वत में मानना कभी इष्ट नहीं होता, अतः प्रसञ्जनीय का अनिष्ट होना आवश्यक है । (५) अननुकूलत्व : प्रतिवादी के अभिमत अर्थ का साधक न होने के कारण वादी के अनुकूल होते हुए भी तर्क प्रतिवादी के अननुकूल ही होता है । कथित पाँच अङ्गों में से प्रत्येक का अभाव होने पर पाँच प्रकार का ही तर्काभास हो जाता है, जैसा कि तार्किकरक्षाकार ने कहा है - "अङ्गान्यतमवैकल्ये तर्काभासता भवेत्" (ता. र० पृ० १८८) जैसे कि, (१) उक्त व्याप्ति का अभाव होने पर 'यद्यग्निमत्त्वं न स्यात्, तर्हि पर्वतत्वमपि न स्यात'-यहाँ अग्निमत्त्वाभाव रूप प्रसञ्जक और पर्वतत्वाभावरूप प्रसञ्जनीय की कोई व्याप्ति (यत्र यत्र अग्निमत्त्वाभावः तत्र तत्र पर्वतत्वाभाव) सम्भव नहीं है क्योंकि सभी पर्वतों में तो अग्नि होती नही, जिस पर्वत में अग्नि नहीं, वहाँ भी पर्वतत्व ही रहता है, पर्वतत्वाभाव नहीं । (२) 'यदीयं मेघोन्नतिवृष्टिमती न स्यात्, तर्हि निविडापि न स्यात्'-यह तर्क 'यदीयं वृष्टिमती स्यात्, तर्हि वातोद्रेकवती न स्यात्'-इस प्रतितर्क से बाधित होने के कारण तर्काभास है, क्योंकि वह सघन (गहरी) घटा भी नहीं बरसती, जो वायु के घोडे पर सवार होकर भागती जा रही हो, अतः उसमें वृष्टिमत्त्व-साधक तर्क तर्काभास ही है । (३) मीमांसक के प्रति प्रयक्त 'शब्दोऽनित्यः कतकत्वात'-इस अनमान की पष्टि में प्रदर्शित 'यदि शब्दोऽनित्यो न स्यात्, तदा कृतकोऽपि न स्यात्' - ऐसे तर्क का पर्यवसान विपर्यय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मीमांसक के मतानुसार शब्द में कृतकत्व नहीं, नित्यत्व माना जाता है । (४) मीमांसक को शब्द में कृतकत्वाभाव इष्ट ही है, अनिष्ट नहीं । (५) प्रसञ्जनीय पदार्थ में प्रतिवादी की अननुकूलता न होने पर तर्काभास का स्वरूप इस प्रकार है - - ‘क्रिया आनुमेया, क्रियात्वाद्, आदित्यक्रियावत्-इस प्रयोग में 'अन्यथा क्रियैव न सिध्येत्'-ऐसा तर्क तर्काभास है, क्योंकि क्रिया का प्रत्यक्ष माननेवाले वादी को भी वैसा कहना अनुकूल ही है - 'प्रत्यक्षा क्रिया अन्यथा क्रियैव न सिध्येत्।'
स्वेनैव स्वस्य सिद्धिर्या तदात्माश्रयदूषणम् । अनेनान्यस्ततश्चायमित्यन्योन्याश्रयं भवेत् ।।१२।।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org