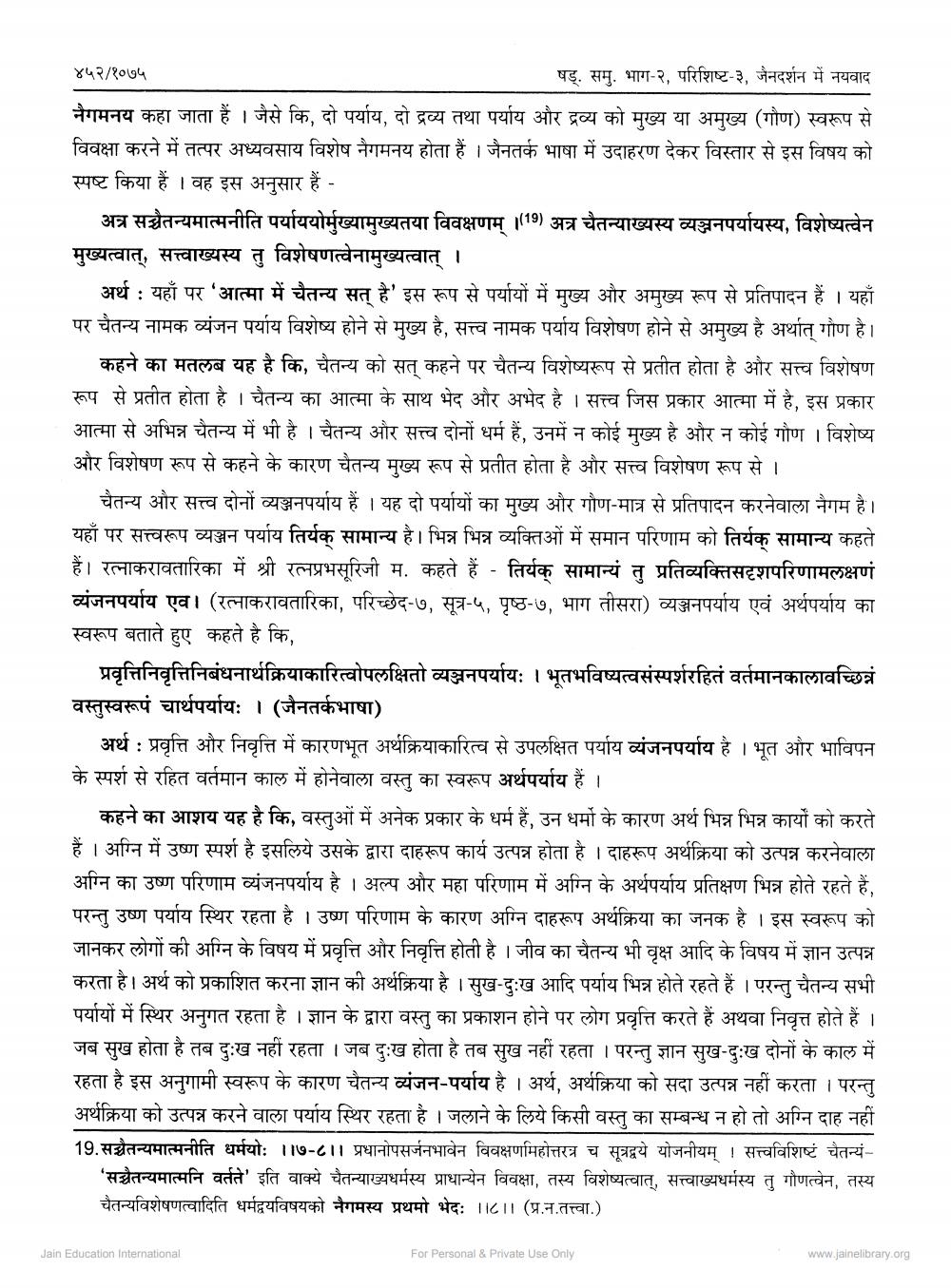________________
४५२/१०७५
षड्. समु. भाग - २, परिशिष्ट-३, जैनदर्शन में नयवाद नैगमनय कहा जाता हैं। जैसे कि, दो पर्याय, दो द्रव्य तथा पर्याय और द्रव्य को मुख्य या अमुख्य (गौण) स्वरूप से विवक्षा करने में तत्पर अध्यवसाय विशेष नैगमनय होता हैं । जैनतर्क भाषा में उदाहरण देकर विस्तार से इस विषय को स्पष्ट किया हैं । वह इस अनुसार हैं -
अत्र सच्चैतन्यमात्मनीति पर्याययोर्मुख्यामुख्यतया विवक्षणम् ।(19) अत्र चैतन्याख्यस्य व्यञ्जनपर्यायस्य, विशेष्यत्वेन मुख्यत्वात्, सत्त्वाख्यस्य तु विशेषणत्वेनामुख्यत्वात् ।
अर्थ : यहाँ पर 'आत्मा में चैतन्य सत् है' इस रूप से पर्यायों में मुख्य और अमुख्य रूप से प्रतिपादन हैं । यहाँ पर चैतन्य नामक व्यंजन पर्याय विशेष्य होने से मुख्य है, सत्त्व नामक पर्याय विशेषण होने से अमुख्य है अर्थात् गौण है।
कहने का मतलब यह है कि, चैतन्य को सत् कहने पर चैतन्य विशेष्यरूप से प्रतीत होता और सत्त्व विशेषण रूप से प्रतीत होता है । चैतन्य का आत्मा के साथ भेद और अभेद है । सत्त्व जिस प्रकार आत्मा में है, इस प्रकार आत्मा से अभिन्न चैतन्य में भी है । चैतन्य और सत्त्व दोनों धर्म हैं, उनमें न कोई मुख्य है और न कोई गौण । विशेष्य और विशेषण रूप से कहने के कारण चैतन्य मुख्य रूप से प्रतीत होता है और सत्त्व विशेषण रूप से ।
चैतन्य और सत्त्व दोनों व्यञ्जनपर्याय हैं । यह दो पर्यायों का मुख्य और गौण - मात्र से प्रतिपादन करनेवाला नैगम है। यहाँ पर सत्त्वरूप व्यञ्जन पर्याय तिर्यक् सामान्य है । भिन्न भिन्न व्यक्तिओं में समान परिणाम को तिर्यक् सामान्य कहते हैं । रत्नाकरावतारिका में श्री रत्नप्रभसूरिजी म. कहते हैं व्यंजनपर्याय एव । (रत्नाकरावतारिका, परिच्छेद-७, सूत्र- ५, स्वरूप बताते हुए कहते है कि.
-
तिर्यक् सामान्यं तु प्रतिव्यक्तिसदृशपरिणामलक्षणं पृष्ठ-७, भाग तीसरा व्यञ्जनपर्याय एवं अर्थपर्याय का
प्रवृत्तिनिवृत्तिनिबंधनार्थक्रियाकारित्वोपलक्षितो व्यञ्जनपर्याय: । भूतभविष्यत्वसंस्पर्शरहितं वर्तमानकालावच्छिन्नं वस्तुस्वरूपं चार्थपर्यायः । ( जैनतर्कभाषा )
अर्थ : प्रवृत्ति और निवृत्ति में कारणभूत अर्थक्रियाकारित्व से उपलक्षित पर्याय व्यंजनपर्याय है । भूत और भाविपन के स्पर्श से रहित वर्तमान काल में होनेवाला वस्तु का स्वरूप अर्थपर्याय हैं ।
कहने का आशय यह है कि, वस्तुओं में अनेक प्रकार के धर्म हैं, उन धर्मो के कारण अर्थ भिन्न भिन्न कार्यों को करते हैं। अग्नि में उष्ण स्पर्श है इसलिये उसके द्वारा दाहरूप कार्य उत्पन्न होता है । दाहरूप अर्थक्रिया को उत्पन्न करनेवाला अग्नि का उष्ण परिणाम व्यंजनपर्याय है । अल्प और महा परिणाम में अग्नि के अर्थपर्याय प्रतिक्षण भिन्न होते रहते हैं, परन्तु उष्ण पर्याय स्थिर रहता है । उष्ण परिणाम के कारण अग्नि दाहरूप अर्थक्रिया का जनक है । इस स्वरूप को जानकर लोगों की अग्नि के विषय में प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है । जीव का चैतन्य भी वृक्ष आदि के विषय में ज्ञान उत्पन्न करता है। अर्थ को प्रकाशित करना ज्ञान की अर्थक्रिया है । सुख-दुःख आदि पर्याय भिन्न होते रहते हैं । परन्तु चैतन्य सभी पर्यायों में स्थिर अनुगत रहता है । ज्ञान के द्वारा वस्तु का प्रकाशन होने पर लोग प्रवृत्ति करते हैं अथवा निवृत्त होते हैं । जब सुख होता है तब दुःख नहीं रहता । जब दुःख होता है तब सुख नहीं रहता । परन्तु ज्ञान सुख - दुःख दोनों के काल में रहता है इस अनुगामी स्वरूप के कारण चैतन्य व्यंजन पर्याय है । अर्थ, अर्थक्रिया को सदा उत्पन्न नहीं करता । परन्तु अर्थक्रिया को उत्पन्न करने वाला पर्याय स्थिर रहता है । जलाने के लिये किसी वस्तु का सम्बन्ध न हो तो अग्नि दाह नहीं 19. सचैतन्यमात्मनीति धर्मयोः ।।७-८ ।। प्रधानोपसर्जनभावेन विवक्षणमिहोत्तरत्र च सूत्रद्वये योजनीयम् । सत्त्वविशिष्टं चैतन्यं'सचैतन्यमात्मनि वर्तते' इति वाक्ये चैतन्याख्यधर्मस्य प्राधान्येन विवक्षा, तस्य विशेष्यत्वात्, सत्त्वाख्यधर्मस्य तु गौणत्वेन, तस्य चैतन्यविशेषणत्वादिति धर्मद्वयविषयको नैगमस्य प्रथमो भेदः ||८|| (प्र.न. तत्त्वा.)
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org