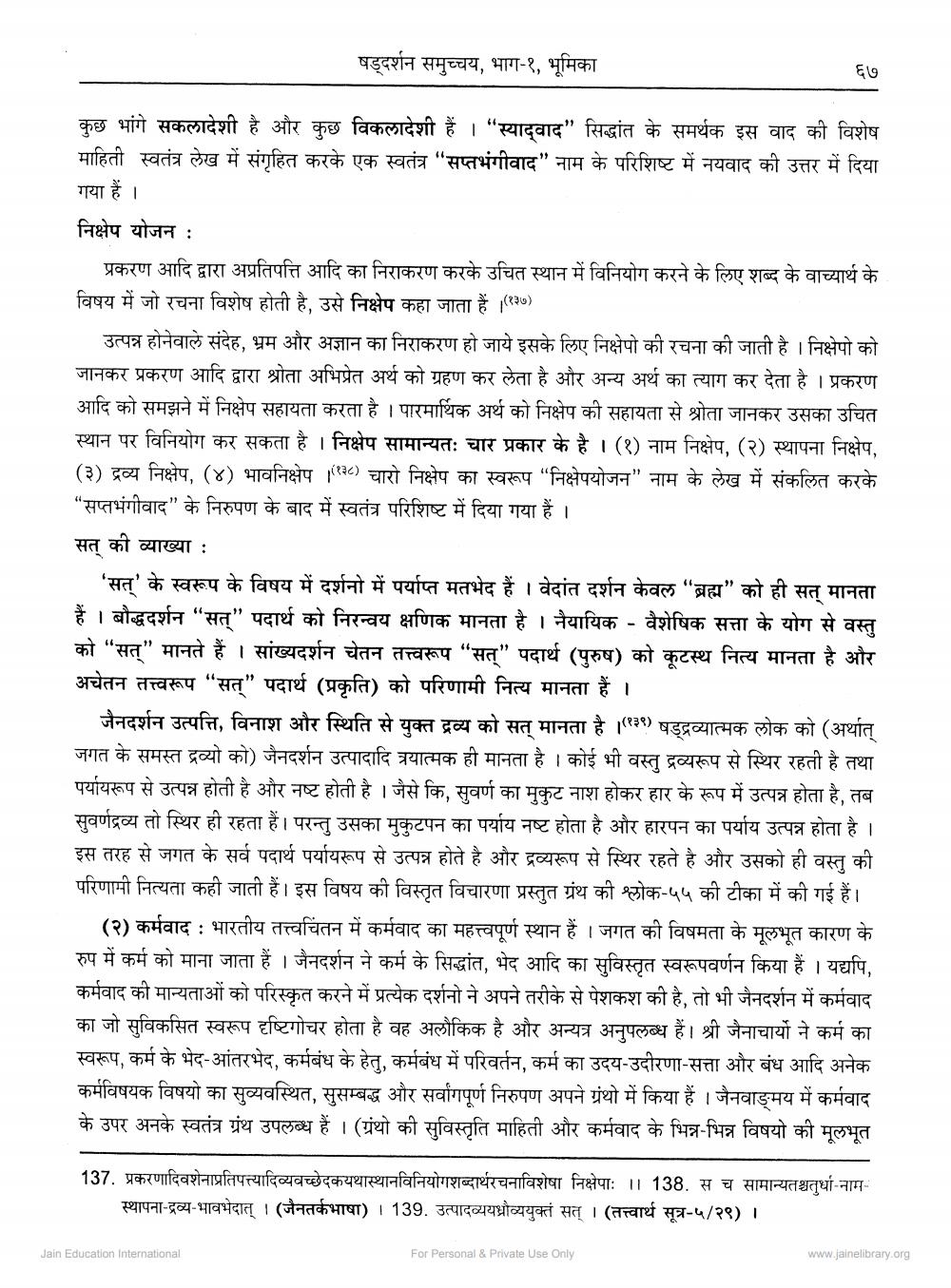________________
षड्दर्शन समुच्चय, भाग-१, भूमिका
कुछ भांगे सकलादेशी है और कुछ विकलादेशी हैं । "स्याद्वाद" सिद्धांत के समर्थक इस वाद की विशेष माहिती स्वतंत्र लेख में संगृहित करके एक स्वतंत्र "सप्तभंगीवाद" नाम के परिशिष्ट में नयवाद की उत्तर में दिया गया है । निक्षेप योजन :
प्रकरण आदि द्वारा अप्रतिपत्ति आदि का निराकरण करके उचित स्थान में विनियोग करने के लिए शब्द के वाच्यार्थ के विषय में जो रचना विशेष होती है, उसे निक्षेप कहा जाता हैं ।(१३७)
उत्पन्न होनेवाले संदेह, भ्रम और अज्ञान का निराकरण हो जाये इसके लिए निक्षेपो की रचना की जाती है । निक्षेपो को जानकर प्रकरण आदि द्वारा श्रोता अभिप्रेत अर्थ को ग्रहण कर लेता है और अन्य अर्थ का त्याग कर देता है । प्रकरण आदि को समझने में निक्षेप सहायता करता है । पारमार्थिक अर्थ को निक्षेप की सहायता से श्रोता जानकर उसका उचित स्थान पर विनियोग कर सकता है । निक्षेप सामान्यत: चार प्रकार के है । (१) नाम निक्षेप, (२) स्थापना निक्षेप, (३) द्रव्य निक्षेप, (४) भावनिक्षेप ।।१३८) चारो निक्षेप का स्वरूप “निक्षेपयोजन" नाम के लेख में संकलित करके “सप्तभंगीवाद" के निरुपण के बाद में स्वतंत्र परिशिष्ट में दिया गया हैं । सत् की व्याख्या :
'सत्' के स्वरूप के विषय में दर्शनी में पर्याप्त मतभेद हैं । वेदांत दर्शन केवल "ब्रह्म" को ही सत् मानता हैं । बौद्धदर्शन “सत्" पदार्थ को निरन्वय क्षणिक मानता है । नैयायिक - वैशेषिक सत्ता के योग से वस्तु को "सत्" मानते हैं । सांख्यदर्शन चेतन तत्त्वरूप "सत्" पदार्थ (पुरुष) को कूटस्थ नित्य मानता है और अचेतन तत्त्वरूप "सत्" पदार्थ (प्रकृति) को परिणामी नित्य मानता हैं ।
जैनदर्शन उत्पत्ति, विनाश और स्थिति से युक्त द्रव्य को सत् मानता है ।(१३९) षड्द्रव्यात्मक लोक को (अर्थात् जगत के समस्त द्रव्यो को) जैनदर्शन उत्पादादि त्रयात्मक ही मानता है । कोई भी वस्तु द्रव्यरूप से स्थिर रहती है तथा पर्यायरूप से उत्पन्न होती है और नष्ट होती है । जैसे कि, सुवर्ण का मुकुट नाश होकर हार के रूप में उत्पन्न होता है, तब सुवर्णद्रव्य तो स्थिर ही रहता हैं। परन्तु उसका मुकुटपन का पर्याय नष्ट होता है और हारपन का पर्याय उत्पन्न होता है । इस तरह से जगत के सर्व पदार्थ पर्यायरूप से उत्पन्न होते है और द्रव्यरूप से स्थिर रहते है और उसको ही वस्तु की परिणामी नित्यता कही जाती हैं। इस विषय की विस्तृत विचारणा प्रस्तुत ग्रंथ की श्लोक-५५ की टीका में की गई हैं।
(२) कर्मवाद : भारतीय तत्त्वचिंतन में कर्मवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । जगत की विषमता के मूलभूत कारण के रुप में कर्म को माना जाता हैं । जैनदर्शन ने कर्म के सिद्धांत, भेद आदि का सविस्तृत स्वरूपवर्णन किया हैं । यद्यपि, कर्मवाद की मान्यताओं को परिस्कृत करने में प्रत्येक दर्शनो ने अपने तरीके से पेशकश की है, तो भी जैनदर्शन में कर्मवाद का जो सुविकसित स्वरूप दृष्टिगोचर होता है वह अलौकिक है और अन्यत्र अनुपलब्ध हैं। श्री जैनाचार्यों ने कर्म का स्वरूप, कर्म के भेद-आंतरभेद, कर्मबंध के हेतु, कर्मबंध में परिवर्तन, कर्म का उदय-उदीरणा-सत्ता और बंध आदि अनेक कर्मविषयक विषयो का सुव्यवस्थित, सुसम्बद्ध और सर्वांगपूर्ण निरुपण अपने ग्रंथो में किया हैं । जैनवाङ्मय में कर्मवाद के उपर अनके स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं । (ग्रंथो की सुविस्तृति माहिती और कर्मवाद के भिन्न-भिन्न विषयो की मूलभूत
137. प्रकरणादिवशेनाप्रतिपत्त्यादिव्यवच्छेदकयथास्थानविनियोगशब्दार्थरचनाविशेषा निक्षेपाः ।। 138. स च सामान्यतश्चतुर्धा-नाम
स्थापना-द्रव्य-भावभेदात् । (जैनतर्कभाषा) । 139. उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् । (तत्त्वार्थ सूत्र-५/२९) ।
For Personal & Private Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org