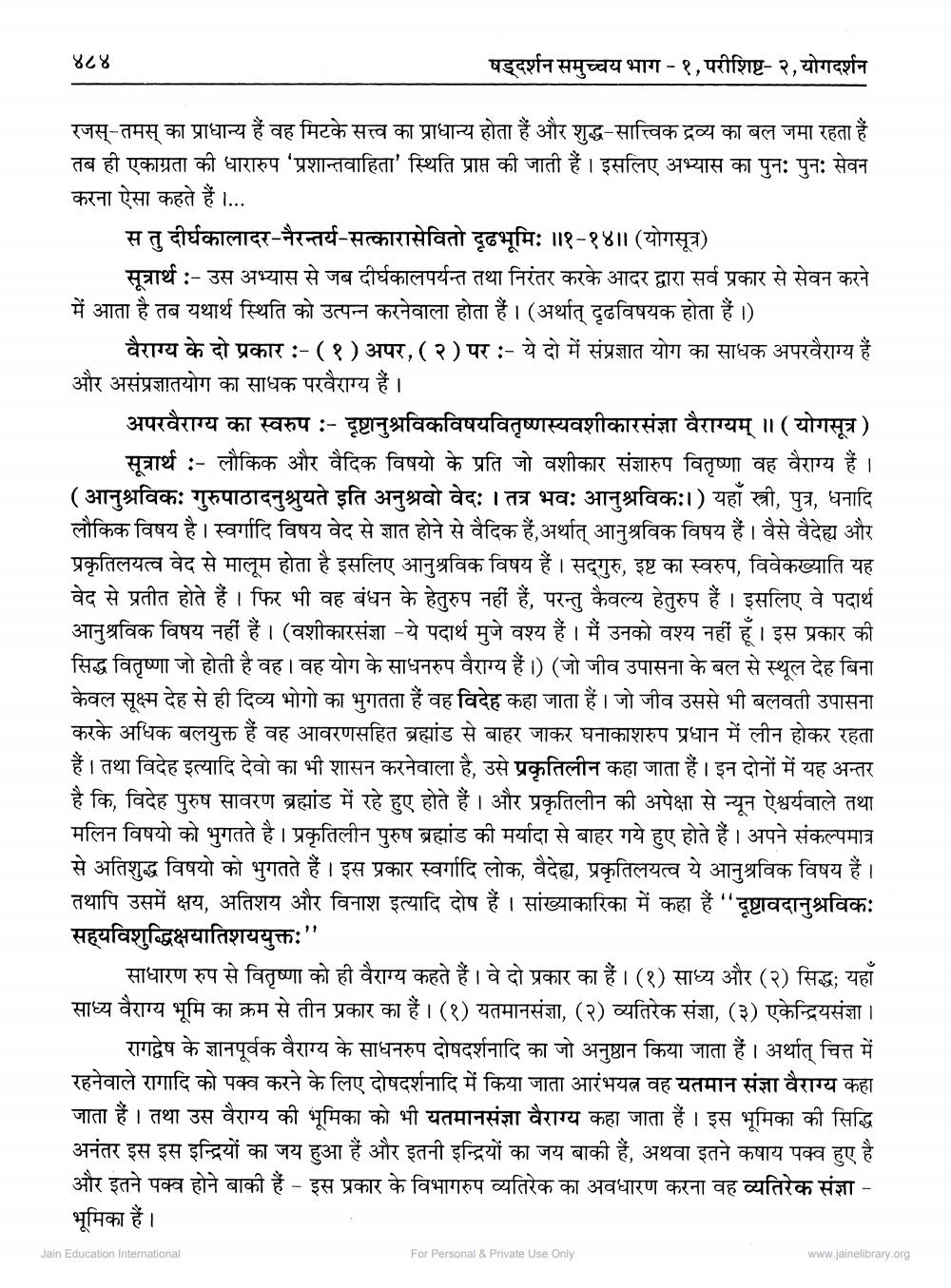________________
४८४
षड्दर्शन समुच्चय भाग - १, परीशिष्ट-२, योगदर्शन
रजस्-तमस् का प्राधान्य हैं वह मिटके सत्त्व का प्राधान्य होता हैं और शुद्ध-सात्त्विक द्रव्य का बल जमा रहता हैं तब ही एकाग्रता की धारारुप 'प्रशान्तवाहिता' स्थिति प्राप्त की जाती हैं। इसलिए अभ्यास का पुनः पुनः सेवन करना ऐसा कहते हैं।...
स तु दीर्घकालादर-नैरन्तर्य-सत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥१-१४॥ (योगसूत्र)
सूत्रार्थ :- उस अभ्यास से जब दीर्घकालपर्यन्त तथा निरंतर करके आदर द्वारा सर्व प्रकार से सेवन करने में आता है तब यथार्थ स्थिति को उत्पन्न करनेवाला होता हैं । (अर्थात् दृढविषयक होता हैं ।)
वैराग्य के दो प्रकार :- (१) अपर, (२) पर :- ये दो में संप्रज्ञात योग का साधक अपरवैराग्य हैं और असंप्रज्ञातयोग का साधक परवैराग्य हैं।
अपरवैराग्य का स्वरुप :- दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्यवशीकारसंज्ञा वैराग्यम् ॥ ( योगसूत्र)
सूत्रार्थ :- लौकिक और वैदिक विषयो के प्रति जो वशीकार संज्ञारुप वितृष्णा वह वैराग्य हैं । (आनुश्रविकः गुरुपाठादनुश्रुयते इति अनुश्रवो वेदः । तत्र भवः आनुश्रविकः।) यहाँ स्त्री, पुत्र, धनादि लौकिक विषय है। स्वर्गादि विषय वेद से ज्ञात होने से वैदिक हैं,अर्थात् आनुश्रविक विषय हैं। वैसे वैदेह्य और प्रकृतिलयत्व वेद से मालूम होता है इसलिए आनुश्रविक विषय हैं । सद्गुरु, इष्ट का स्वरुप, विवेकख्याति यह वेद से प्रतीत होते हैं। फिर भी वह बंधन के हेतुरुप नहीं हैं, परन्तु कैवल्य हेतुरुप हैं । इसलिए वे पदार्थ आनुश्रविक विषय नहीं हैं । (वशीकारसंज्ञा -ये पदार्थ मुजे वश्य हैं । मैं उनको वश्य नहीं हूँ। इस प्रकार की सिद्ध वितृष्णा जो होती है वह। वह योग के साधनरुप वैराग्य हैं।) (जो जीव उपासना के बल से स्थूल देह बिना केवल सूक्ष्म देह से ही दिव्य भोगो का भुगतता हैं वह विदेह कहा जाता हैं । जो जीव उससे भी बलवती उपासना करके अधिक बलयुक्त हैं वह आवरणसहित ब्रह्मांड से बाहर जाकर घनाकाशरुप प्रधान में लीन होकर रहता हैं। तथा विदेह इत्यादि देवो का भी शासन करनेवाला है, उसे प्रकृतिलीन कहा जाता हैं। इन दोनों में यह अन्तर है कि, विदेह पुरुष सावरण ब्रह्मांड में रहे हुए होते हैं। और प्रकृतिलीन की अपेक्षा से न्यून ऐश्वर्यवाले तथा मलिन विषयो को भुगतते है। प्रकृतिलीन पुरुष ब्रह्मांड की मर्यादा से बाहर गये हुए होते हैं। अपने संकल्पमात्र से अतिशुद्ध विषयो को भुगतते हैं। इस प्रकार स्वर्गादि लोक, वैदेह्य, प्रकृतिलयत्व ये आनुश्रविक विषय हैं। तथापि उसमें क्षय, अतिशय और विनाश इत्यादि दोष हैं । सांख्याकारिका में कहा हैं "दृष्टावदानुश्रविकः सह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः"
साधारण रुप से वितृष्णा को ही वैराग्य कहते हैं । वे दो प्रकार का हैं । (१) साध्य और (२) सिद्ध; यहाँ साध्य वैराग्य भूमि का क्रम से तीन प्रकार का हैं । (१) यतमानसंज्ञा, (२) व्यतिरेक संज्ञा, (३) एकेन्द्रियसंज्ञा ।
रागद्वेष के ज्ञानपूर्वक वैराग्य के साधनरुप दोषदर्शनादि का जो अनुष्ठान किया जाता हैं । अर्थात् चित्त में रहनेवाले रागादि को पक्व करने के लिए दोषदर्शनादि में किया जाता आरंभयत्न वह यतमान संज्ञा वैराग्य कहा जाता हैं । तथा उस वैराग्य की भूमिका को भी यतमानसंज्ञा वैराग्य कहा जाता हैं । इस भूमिका की सिद्धि अनंतर इस इस इन्द्रियों का जय हुआ हैं और इतनी इन्द्रियों का जय बाकी हैं, अथवा इतने कषाय पक्व हुए है और इतने पक्व होने बाकी हैं - इस प्रकार के विभागरुप व्यतिरेक का अवधारण करना वह व्यतिरेक संज्ञा - भूमिका हैं।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org