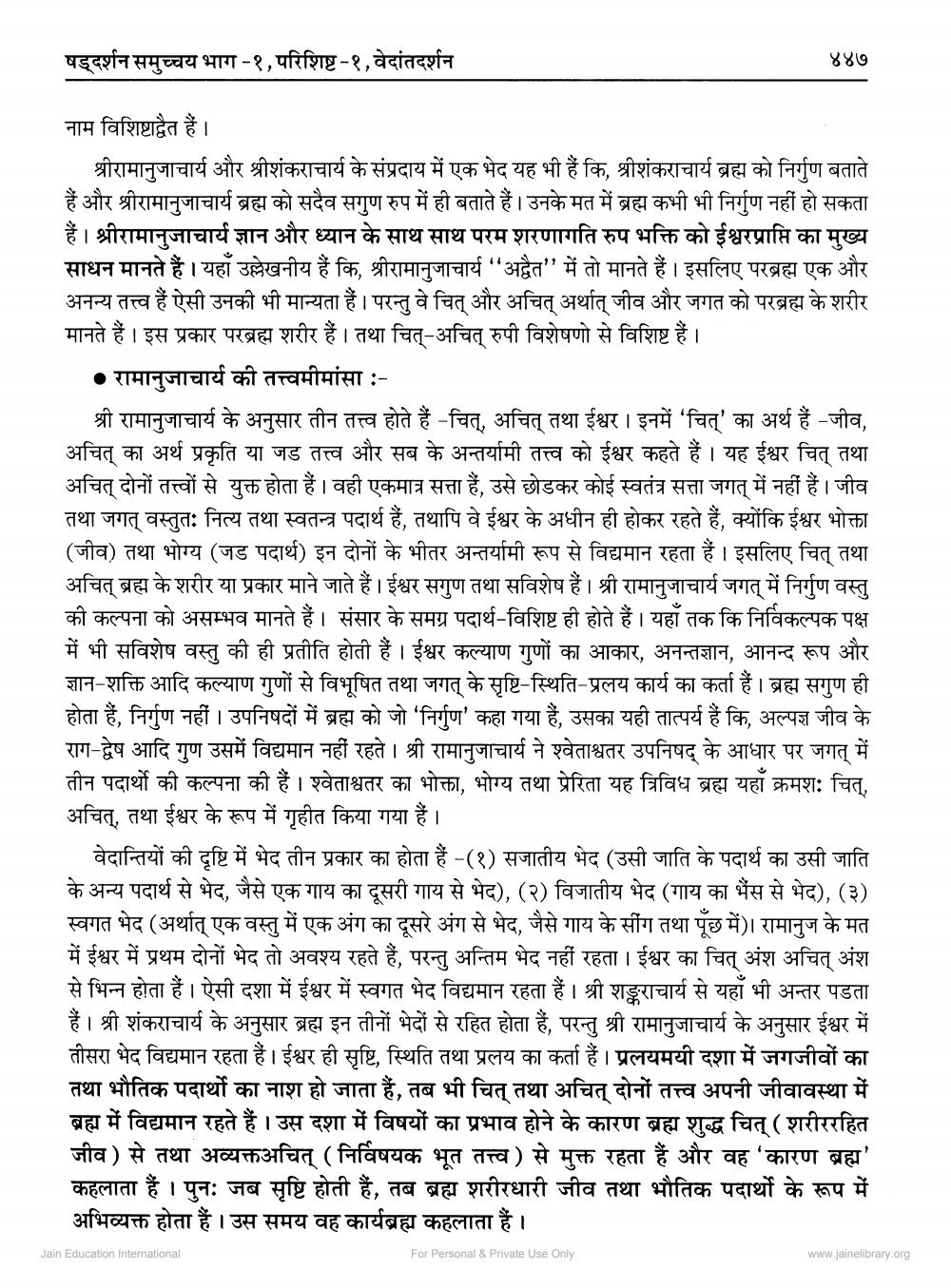________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग -१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
४४७
नाम विशिष्टाद्वैत हैं। ___ श्रीरामानुजाचार्य और श्रीशंकराचार्य के संप्रदाय में एक भेद यह भी हैं कि, श्रीशंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण बताते हैं और श्रीरामानुजाचार्य ब्रह्म को सदैव सगुण रुप में ही बताते हैं। उनके मत में ब्रह्म कभी भी निर्गुण नहीं हो सकता हैं। श्रीरामानुजाचार्य ज्ञान और ध्यान के साथ साथ परम शरणागति रुप भक्ति को ईश्वरप्राप्ति का मुख्य साधन मानते हैं । यहाँ उल्लेखनीय हैं कि, श्रीरामानुजाचार्य "अद्वैत' में तो मानते हैं। इसलिए परब्रह्म एक और अनन्य तत्त्व हैं ऐसी उनकी भी मान्यता हैं। परन्तु वे चित् और अचित् अर्थात् जीव और जगत को परब्रह्म के शरीर मानते हैं । इस प्रकार परब्रह्म शरीर हैं। तथा चित्-अचित् रुपी विशेषणो से विशिष्ट हैं।
• रामानुजाचार्य की तत्त्वमीमांसा :
श्री रामानुजाचार्य के अनुसार तीन तत्त्व होते हैं -चित्, अचित् तथा ईश्वर । इनमें 'चित्' का अर्थ हैं -जीव, अचित् का अर्थ प्रकृति या जड तत्त्व और सब के अन्तर्यामी तत्त्व को ईश्वर कहते हैं । यह ईश्वर चित् तथा अचित् दोनों तत्त्वों से युक्त होता हैं। वही एकमात्र सत्ता हैं, उसे छोडकर कोई स्वतंत्र सत्ता जगत् में नहीं हैं। जीव तथा जगत् वस्तुतः नित्य तथा स्वतन्त्र पदार्थ हैं, तथापि वे ईश्वर के अधीन ही होकर रहते हैं, क्योंकि ईश्वर भोक्ता (जीव) तथा भोग्य (जड पदार्थ) इन दोनों के भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान रहता हैं । इसलिए चित् तथा अचित् ब्रह्म के शरीर या प्रकार माने जाते हैं। ईश्वर सगुण तथा सविशेष हैं। श्री रामानुजाचार्य जगत् में निर्गुण वस्तु की कल्पना को असम्भव मानते हैं। संसार के समग्र पदार्थ-विशिष्ट ही होते हैं। यहाँ तक कि निर्विकल्पक पक्ष में भी सविशेष वस्तु की ही प्रतीति होती हैं । ईश्वर कल्याण गुणों का आकार, अनन्तज्ञान, आनन्द रूप और ज्ञान-शक्ति आदि कल्याण गुणों से विभूषित तथा जगत् के सृष्टि-स्थिति-प्रलय कार्य का कर्ता हैं । ब्रह्म सगुण ही होता हैं, निर्गुण नहीं । उपनिषदों में ब्रह्म को जो 'निर्गुण' कहा गया है, उसका यही तात्पर्य हैं कि, अल्पज्ञ जीव के राग-द्वेष आदि गुण उसमें विद्यमान नहीं रहते। श्री रामानुजाचार्य ने श्वेताश्वतर उपनिषद् के आधार पर जगत् में तीन पदार्थो की कल्पना की हैं। श्वेताश्वतर का भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरिता यह त्रिविध ब्रह्म यहाँ क्रमशः चित्, अचित्, तथा ईश्वर के रूप में गृहीत किया गया हैं।
वेदान्तियों की दृष्टि में भेद तीन प्रकार का होता हैं -(१) सजातीय भेद (उसी जाति के पदार्थ का उसी जाति के अन्य पदार्थ से भेद, जैसे एक गाय का दूसरी गाय से भेद), (२) विजातीय भेद (गाय का भैंस से भेद), (३) स्वगत भेद (अर्थात् एक वस्तु में एक अंग का दूसरे अंग से भेद, जैसे गाय के सींग तथा पूँछ में)। रामानुज के मत में ईश्वर में प्रथम दोनों भेद तो अवश्य रहते हैं, परन्तु अन्तिम भेद नहीं रहता। ईश्वर का चित् अंश अचित् अंश से भिन्न होता हैं । ऐसी दशा में ईश्वर में स्वगत भेद विद्यमान रहता हैं। श्री शङ्कराचार्य से यहाँ भी अन्तर पडता हैं। श्री शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म इन तीनों भेदों से रहित होता हैं, परन्तु श्री रामानुजाचार्य के अनुसार ईश्वर में तीसरा भेद विद्यमान रहता हैं। ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कर्ता हैं। प्रलयमयी दशा में जगजीवों का तथा भौतिक पदार्थो का नाश हो जाता हैं, तब भी चित् तथा अचित् दोनों तत्त्व अपनी जीवावस्था में ब्रह्म में विद्यमान रहते हैं । उस दशा में विषयों का प्रभाव होने के कारण ब्रह्म शुद्ध चित् (शरीररहित जीव) से तथा अव्यक्तअचित् (निर्विषयक भूत तत्त्व) से मुक्त रहता हैं और वह 'कारण ब्रह्म' कहलाता हैं । पुनः जब सृष्टि होती हैं, तब ब्रह्म शरीरधारी जीव तथा भौतिक पदार्थो के रूप में अभिव्यक्त होता हैं । उस समय वह कार्यब्रह्म कहलाता हैं।
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org