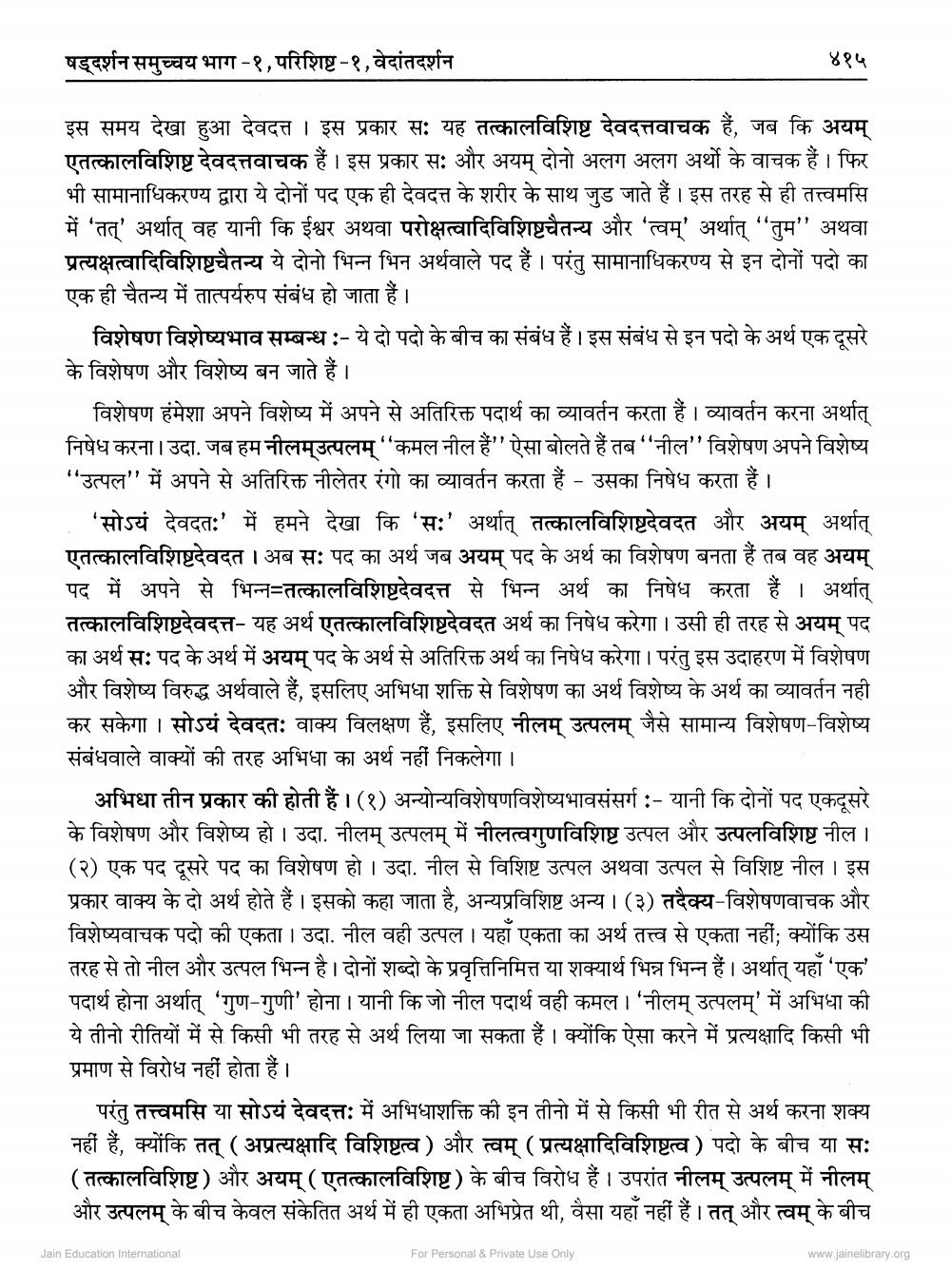________________
षड्दर्शन समुच्चय भाग -१, परिशिष्ट-१, वेदांतदर्शन
४१५
इस समय देखा हुआ देवदत्त । इस प्रकार स: यह तत्कालविशिष्ट देवदत्तवाचक हैं, जब कि अयम् एतत्कालविशिष्ट देवदत्तवाचक हैं । इस प्रकार सः और अयम् दोनो अलग अलग अर्थो के वाचक हैं। फिर भी सामानाधिकरण्य द्वारा ये दोनों पद एक ही देवदत्त के शरीर के साथ जुड जाते हैं। इस तरह से ही तत्त्वमसि में 'तत्' अर्थात् वह यानी कि ईश्वर अथवा परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य और 'त्वम्' अर्थात् "तुम" अथवा प्रत्यक्षत्वादिविशिष्टचैतन्य ये दोनो भिन्न भिन अर्थवाले पद हैं। परंतु सामानाधिकरण्य से इन दोनों पदो का एक ही चैतन्य में तात्पर्यरुप संबंध हो जाता हैं।
विशेषण विशेष्यभाव सम्बन्ध :- ये दो पदो के बीच का संबंध हैं। इस संबंध से इन पदो के अर्थ एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य बन जाते हैं।
विशेषण हमेशा अपने विशेष्य में अपने से अतिरिक्त पदार्थ का व्यावर्तन करता हैं । व्यावर्तन करना अर्थात् निषेध करना। उदा. जब हम नीलम्उत्पलम् “कमल नील हैं" ऐसा बोलते हैं तब "नील'' विशेषण अपने विशेष्य "उत्पल'' में अपने से अतिरिक्त नीलेतर रंगो का व्यावर्तन करता हैं - उसका निषेध करता हैं।
'सोऽयं देवदतः' में हमने देखा कि 'सः' अर्थात् तत्कालविशिष्टदेवदत और अयम् अर्थात् एतत्कालविशिष्टदेवदत । अब सः पद का अर्थ जब अयम् पद के अर्थ का विशेषण बनता हैं तब वह अयम् पद में अपने से भिन्न-तत्कालविशिष्टदेवदत्त से भिन्न अर्थ का निषेध करता हैं । अर्थात् तत्कालविशिष्टदेवदत्त- यह अर्थ एतत्कालविशिष्टदेवदत अर्थ का निषेध करेगा। उसी ही तरह से अयम् पद का अर्थ सः पद के अर्थ में अयम् पद के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ का निषेध करेगा। परंतु इस उदाहरण में विशेषण
और विशेष्य विरुद्ध अर्थवाले हैं, इसलिए अभिधा शक्ति से विशेषण का अर्थ विशेष्य के अर्थ का व्यावर्तन नही कर सकेगा । सोऽयं देवदतः वाक्य विलक्षण हैं, इसलिए नीलम् उत्पलम् जैसे सामान्य विशेषण-विशेष्य संबंधवाले वाक्यों की तरह अभिधा का अर्थ नहीं निकलेगा। ___ अभिधा तीन प्रकार की होती हैं। (१) अन्योन्यविशेषणविशेष्यभावसंसर्ग :- यानी कि दोनों पद एकदूसरे के विशेषण और विशेष्य हो । उदा. नीलम् उत्पलम् में नीलत्वगुणविशिष्ट उत्पल और उत्पलविशिष्ट नील । (२) एक पद दूसरे पद का विशेषण हो । उदा. नील से विशिष्ट उत्पल अथवा उत्पल से विशिष्ट नील । इस प्रकार वाक्य के दो अर्थ होते हैं। इसको कहा जाता है, अन्यप्रविशिष्ट अन्य। (३) तदैक्य-विशेषणवाचक और विशेष्यवाचक पदो की एकता। उदा. नील वही उत्पल । यहाँ एकता का अर्थ तत्त्व से एकता नहीं; क्योंकि उस तरह से तो नील और उत्पल भिन्न है। दोनों शब्दो के प्रवृत्तिनिमित्त या शक्यार्थ भिन्न भिन्न हैं। अर्थात् यहाँ 'एक' पदार्थ होना अर्थात् 'गुण-गुणी' होना। यानी कि जो नील पदार्थ वही कमल । 'नीलम् उत्पलम्' में अभिधा की ये तीनो रीतियों में से किसी भी तरह से अर्थ लिया जा सकता हैं। क्योंकि ऐसा करने में प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं होता हैं।
परंतु तत्त्वमसि या सोऽयं देवदत्तः में अभिधाशक्ति की इन तीनो में से किसी भी रीत से अर्थ करना शक्य नहीं हैं, क्योंकि तत् (अप्रत्यक्षादि विशिष्टत्व) और त्वम् (प्रत्यक्षादिविशिष्टत्व) पदो के बीच या सः (तत्कालविशिष्ट) और अयम् ( एतत्कालविशिष्ट) के बीच विरोध हैं । उपरांत नीलम् उत्पलम् में नीलम् और उत्पलम् के बीच केवल संकेतित अर्थ में ही एकता अभिप्रेत थी, वैसा यहाँ नहीं हैं । तत् और त्वम् के बीच
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org